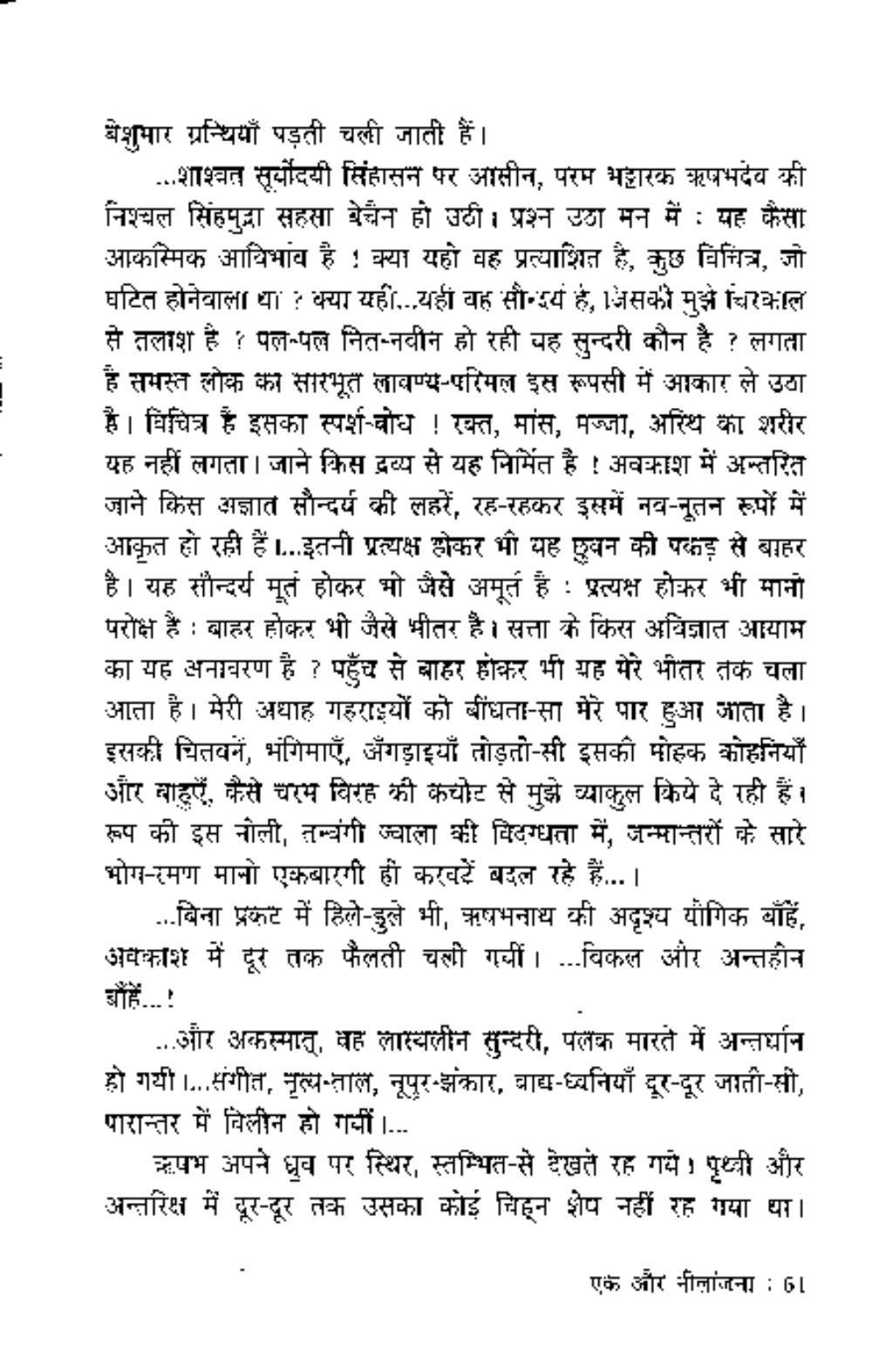________________
बेशुमार ग्रन्थियाँ पड़ती चली जाती हैं। ___...शाश्वत सूर्योदयी सिंहासन पर आसीन, परम भट्टारक ऋषभदेव की निश्चल सिंहमुद्रा सहसा बेचैन हो उठी। प्रश्न उठा मन में : यह कैसा आकस्मिक आविभाव है : क्या यहो वह प्रत्याशित है, कुछ विचित्र, जो घटित होनेवाला था ? क्या यही...यहीं वह सौ इयं है, जिसकी मुझे चिरकाल से तलाश है ? पल-पल नित-नवीन हो रही वह सुन्दरी कौन है ? लगता हैं समस्त लोक का सारभूत लावण्य-परिमल इस रूपसी में आकार ले उठा है। विचित्र हैं इसका स्पर्श-वोध ! रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि का शरीर यह नहीं लगता। जाने किस द्रव्य से यह निर्मित है ! अवकाश में अन्तरित जाने किस अज्ञात सौन्दर्य की लहरें, रह-रहकर इसमें नव-नूतन रूपों में आकृत हो रही हैं।...इतनी प्रत्यक्ष होकर भी यह छुपन की पकड़ से बाहर है। यह सौन्दर्य मतं होकर भी जैसे अमर्त हैं : प्रत्यक्ष होकर भी मानो परोक्ष हैं : बाहर होकर भी जैसे भीतर है। सत्ता के किस अविज्ञात आयाम का यह अनावरण है ? पहुँच से बाहर होकर भी यह मेरे भीतर तक चला आता है। मेरी अथाह गहराइयों को बांधता-सा मेरे पार हुआ जाता है। इसकी चितवन, भंगिमाएँ, अँगड़ाइयाँ तोड़तो-सी इसकी मोहक कोहनियाँ
और बाहुएँ, कैसे चरम विरह की कचोट से मुझे व्याकुल किये दे रही हैं। रूप की इस नौली, तन्वंगी ज्वाला की विदग्धता में, जन्मान्तरों के सारे भोग-रमण मानो एकबारगी ही करवटें बदल रहे हैं...।
....बिना प्रकट में हिले-डुले भी, ऋषभनाथ की अदृश्य यौगिक बाँहें, अवकाश में दूर तक फैलती चली गीं। ...विकल और अन्तहीन बाँहें...!
...और अकस्मात्, वह लास्थलीन सुन्दरी, पलक मारते में अन्तर्धान हो गयी।...संगीत, नृत्य-ताल, नूपुर-झंकार, बाद्य-ध्वनियाँ दूर-दूर जाती-सी, पारान्तर में विलीन हो गयीं ।...
ऋपभ अपने ध्रुव पर स्थिर, स्तम्भित-से देखते रह गये। पृथ्वी और अन्तरिक्ष में दूर-दूर तक उसका कोई चिह्न शेष नहीं रह गया था।
एक और नीलांजना : 61