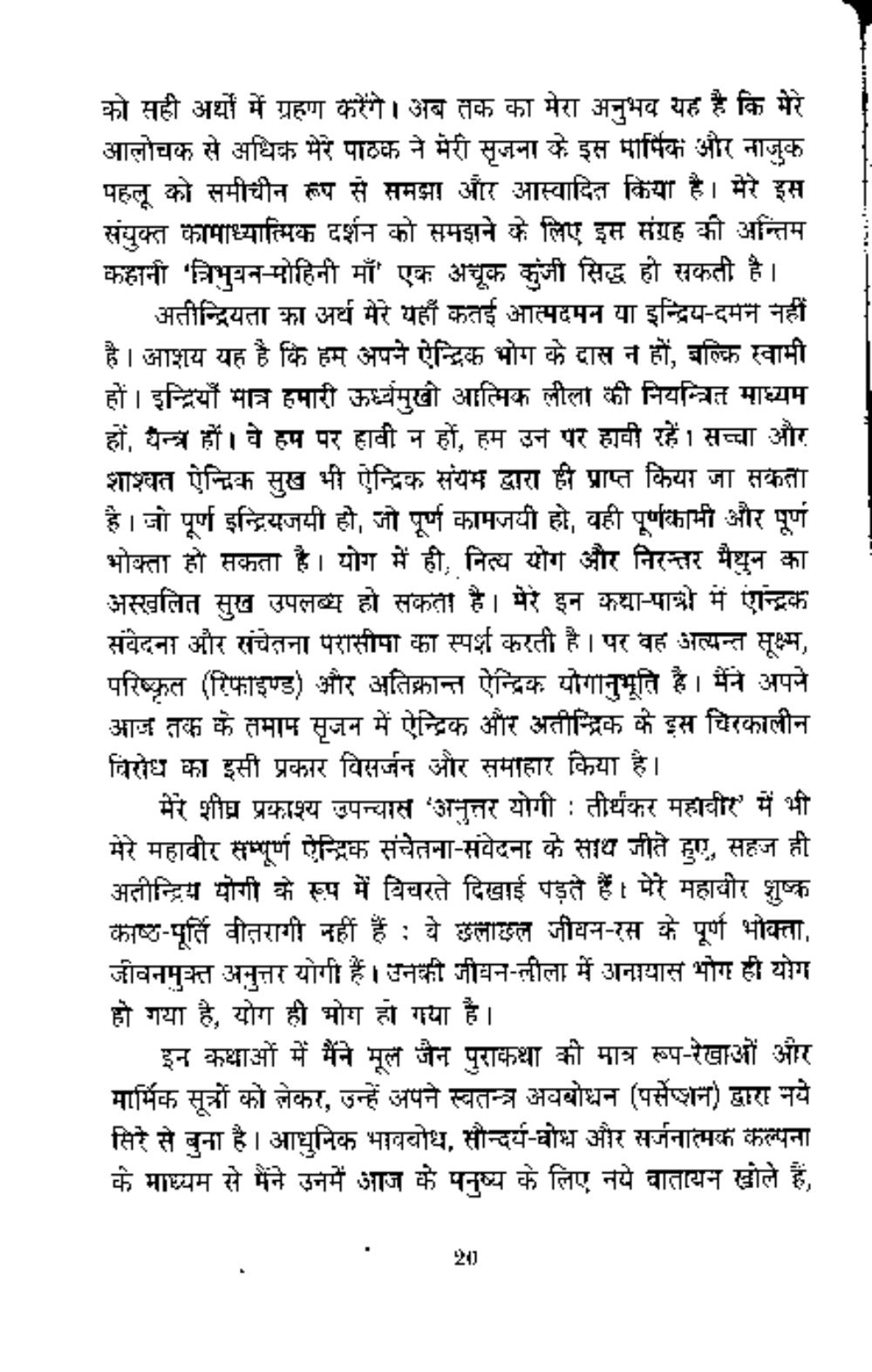________________
को सही अर्थों में ग्रहण करेंगे। अब तक का मेरा अनुभव यह है कि मेरे आलोचक से अधिक मेरे पाठक ने मेरी सृजना के इस मार्मिक और नाजुक पहलू को समीचीन रूप से समझा और आस्वादित किया है। मेरे इस संयुक्त कामाध्यात्मिक दर्शन को समझने के लिए इस संग्रह की अन्तिम कहानी 'त्रिभुवन-मोहिनी माँ' एक अचूक कुंजी सिद्ध हो सकती है।
अतीन्द्रियता का अर्थ मेरे यहाँ कतई आत्पदमन या इन्द्रिय-दमन नहीं है। आशय यह है कि हम अपने ऐन्द्रिक भोग के दास न हों, बल्कि स्वामी हों । इन्द्रियाँ मात्र हमारी ऊध्र्यमुखी आत्मिक लीला की नियन्त्रित माध्यम हों, यन्त्र हों। वे हम पर हावी न हों, हम उन पर हावी रहें। सच्चा और शाश्वत ऐन्द्रिक सुख भी ऐन्द्रिक संयम द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। जो पूर्ण इन्द्रियजयी हो, जो पूर्ण कामजयी हो, वही पूर्णकामी और पूर्ण भोक्ता हो सकता है। योग में ही, नित्य योग और निरन्तर मैथुन का अस्खलित सुख उपलब्ध हो सकता है। मेरे इन कथा-पात्रो में गन्द्रक संवेदना और संचेतना परासीपा का स्पर्श करती है। पर वह अत्यन्त सूक्ष्म, परिष्कृत (रिफाइण्ड) और अतिक्रान्त ऐन्द्रिक योगानुभूति है। मैंने अपने आज तक के तमाम सृजन में ऐन्द्रिक और अतीन्द्रिक के इस चिरकालीन विरोध का इसी प्रकार विसर्जन और समाहार किया है। ___ मेरे शीघ्र प्रकाश्य उपन्यास 'अनुत्तर योगी : तीर्थंकर महावीर' में भी मेरे महावीर सम्पूर्ण ऐन्द्रिक संचेतना-संवेदना के साथ जीते हुए, सहज ही अतीन्द्रिय योगी के रूप में विचरते दिखाई पड़ते हैं। मेरे महावीर शुष्क काष्ठ-पूर्ति वीतरागी नहीं हैं : ये छलाइल जीवन-रस के पूर्ण भोक्ता, जीवनमुक्त अनुत्तर योगी हैं। उनकी जीवन-लीला में अनायास भोग ही योग हो गया है, योग ही भोग हो गया है।
इन कथाओं में मैंने मूल जैन पुराकथा को मात्र रूप-रेखाओं और मार्मिक सूत्रों को लेकर, उन्हें अपने स्वतन्त्र अवबोधन (पर्सेशन) द्वारा नये सिरे से बुना है। आधुनिक भावबोध, सौन्दर्य-चोच और सर्जनात्मक कल्पना के माध्यम से मैंने उनमें आज के पनुष्य के लिए नये वातायन खोले हैं,
20