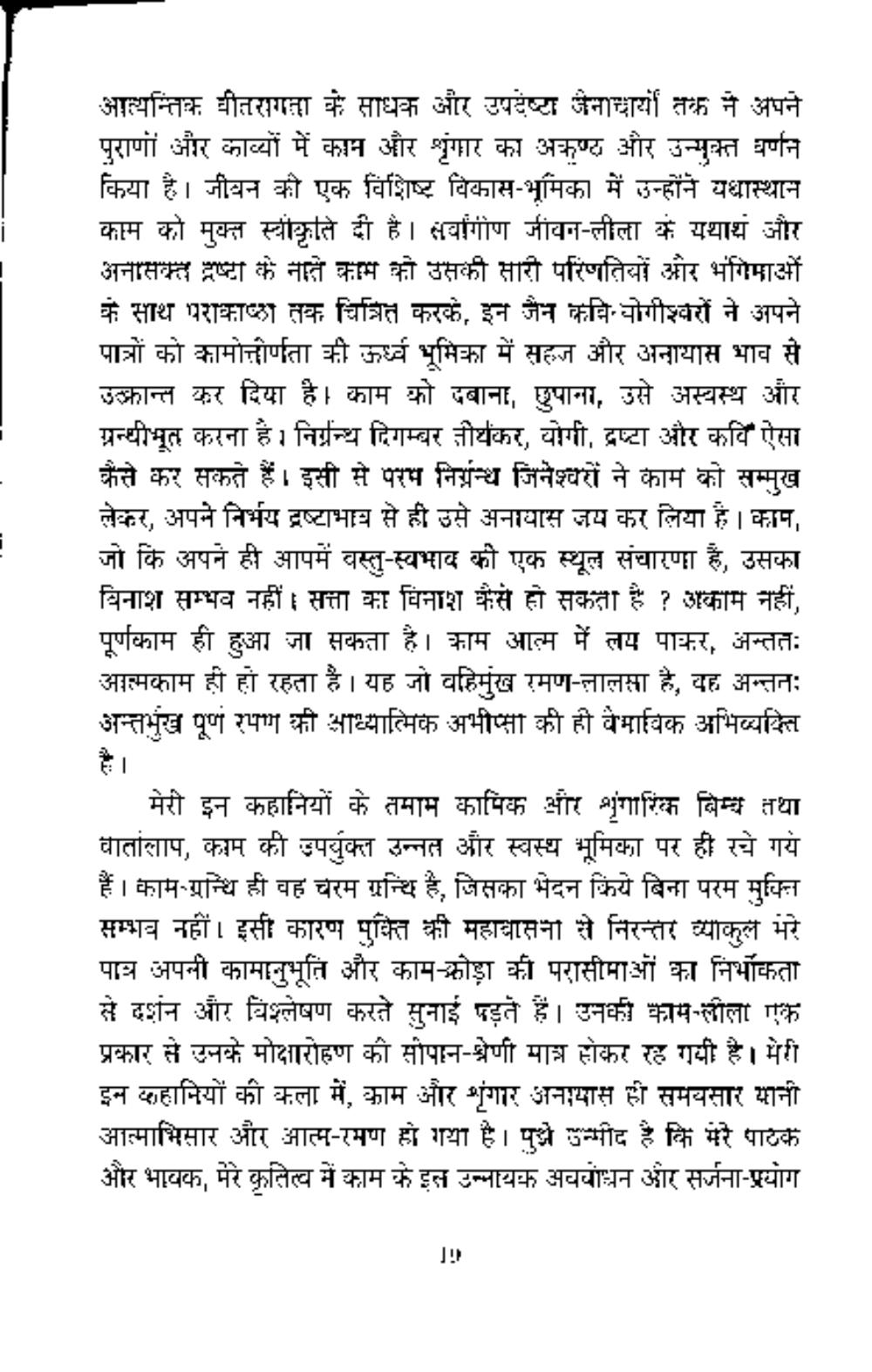________________
आत्यन्तिक वीतरागता के साधक और उपदेष्टा जैनाचार्यों तक ने अपने पुराणों और काव्यों में काम और शृंगार का अकण्ट और उन्मुक्त वर्णन किया है। जीवन की एक विशिष्ट विकास-भूमिका में उन्होंने यधास्थान काम को मुक्त स्वीकृति दी है। सांगीण जीवन-लीला के यथार्थ और अनासक्त द्रष्टा के नाते काम को उसकी सारी परिणतियों और भंगिमाओं के साथ पराकाष्ठा तक चित्रित करके, इन जैन कनि बोगीश्वरों ने अपने पात्रों को कामोत्तीर्णता की ऊर्ध्व भूमिका में सहज और अनायास भाव से उक्रान्त कर दिया है। काम को दबाना, छुपाना, उसे अस्वस्थ और ग्नन्धीभूत करना है। निर्ग्रन्थ दिगम्बर तीर्थकर, बोगी, द्रष्टा और कवि ऐसा बैत्ते कर सकते हैं। इसी से परम निग्रन्थ जिनेश्वरों ने काम को सम्मुख लेकर, अपने निर्भय द्रष्टाभाव से ही उसे अनायास जय कर लिया है। काम, जो कि अपने ही आपमें वस्तु-स्वभाव की एक स्थूल संचारणा हैं, उसका विनाश सम्भव नहीं । सत्ता का विनाश कैसे हो सकता है ? अकाम नहीं, पूर्णकाम ही हुआ जा सकता है। काम आत्म में लय पाकर, अन्ततः आत्मकाम ही हो रहता है। यह जो बहिर्मुख रमण-लालप्सा है, वह अन्ततः अन्तभुख पूर्ण रमण की आध्यात्मिक अभीप्सा की ही वैमाविक अभिव्यक्ति
मेरी इन कहानियों के तमाम कामिक और शृंगारिक बिम्ब तथा चातालाप, काम की उपर्युक्त उन्नत और स्वस्थ भूमिका पर ही रचे गये हैं । काम ग्रन्थि ही वह चरम ग्रन्थि है, जिसका भेदन किये बिना परम मुक्ति सम्भव नहीं। इसी कारण पुक्ति की महाबासना से निरन्तर व्याकुल भरे पात्र अपनी कामानुभूति और काम-झोड़ा की परासीमाओं का निर्भीकता से दर्शन और विश्लेषण करते सुनाई पड़ते हैं। उनकी काम-लीला एक प्रकार से उनके मोक्षारोहण की सोपान-श्रेणी मात्र होकर रह गयी है। मेरी इन कहानियों की कला में, काम और शृंगार अनायास ही समयसार यानी आत्माभिसार और आत्म-रमण हो गया है। पुझे उम्मीद है कि मेरे पाठक और भावक, मेरे कृतित्व में काम के इस उन्नायक अचांधन और सर्जना-प्रयोग