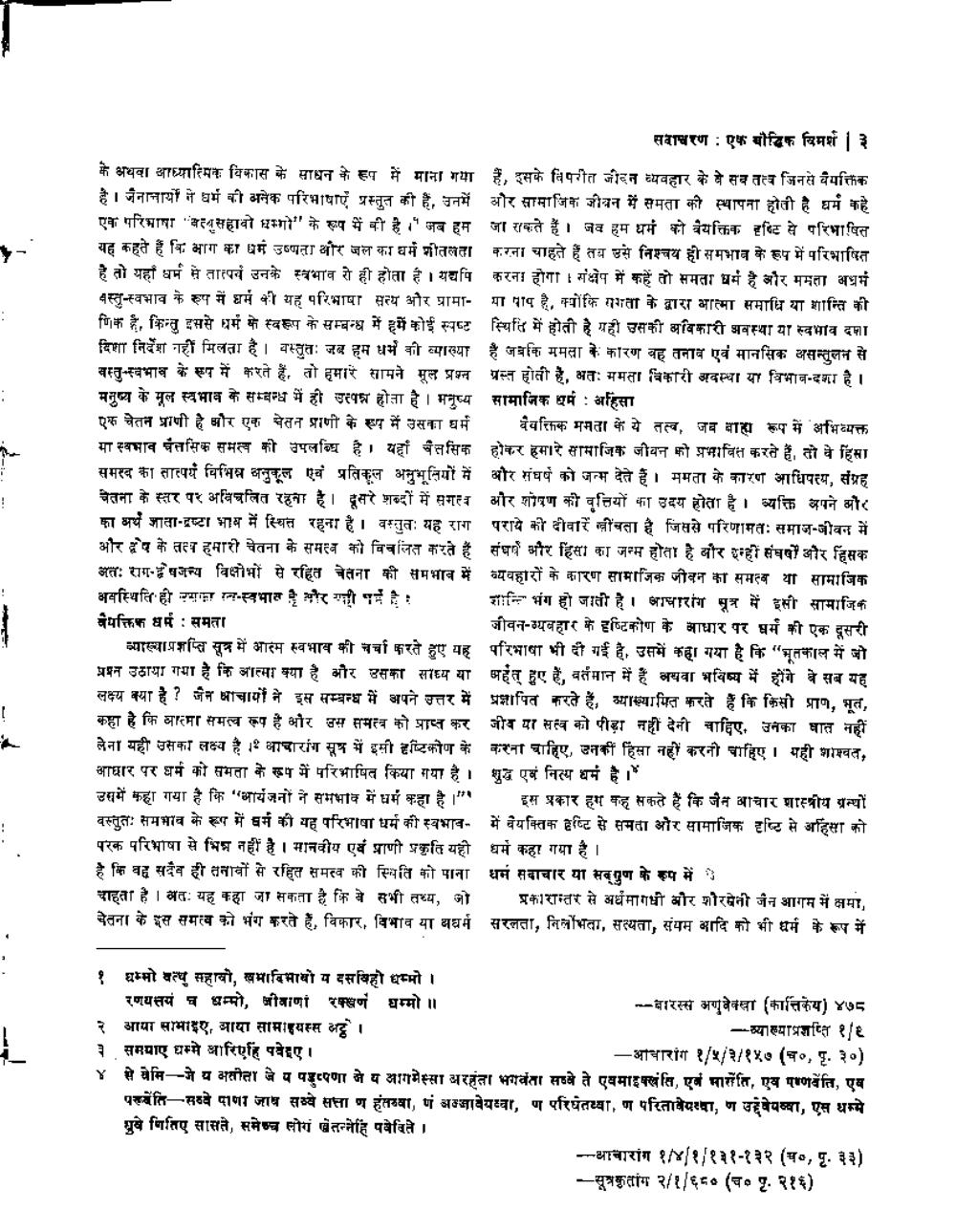________________
सवाचरण : एक बौद्धिक विमर्श | ३ के अथवा आध्यात्मिक विकास के साधन के रूप में माना गया है, इसके विपरीत जीवन व्यवहार के वे सब तत्व जिनसे वैयक्तिक है। जैनाचार्यों ने धर्म की अनेक परिभाषाएँ प्रस्तुत की हैं, उनमें और सामाजिक जीवन में समता की स्थापना होती है धर्म कहे एक परिभाषा "वत्सहाबो धम्गों" के रूप में की है। जब हम जा सकते हैं। जब हम धर्म को वैयक्तिक दृष्टि से परिभाषित यह कहते हैं कि आग का धर्म उष्णता और जल' का धर्म शीतलता करना चाहते हैं तब उसे निश्चय ही समभाव के रूप में परिभाषित है तो यहाँ धर्म में तात्पर्य उनके स्वभाव से ही होता है । यद्यपि करना होगा । संक्षेप में कहें तो समता धर्म है और ममता अधर्म वस्तु-स्वभाव के रूप में धर्म की यह परिभाषा सत्य और प्रामा- या पाप है, क्योंकि गगता के द्वारा भात्मा समाधि या शान्ति की णिक है, किन्तु इससे धर्म के स्वरूप के सम्बन्ध में हमें कोई स्पष्ट स्थिति में होती है यही उसकी अधिकारी अवस्था या स्वभाव दशा दिशा निर्देश नहीं मिलता है। वस्तुतः जब हम धर्म की व्याख्या है जबकि ममता के कारण वह तनाब एवं मानसिक असन्तुलन से वस्तु-स्वभाव के रूप में करते हैं, तो हमारे सामने मूल प्रश्न ग्रस्त होती है, अतः ममता विकारी अवस्था या विभाव-दशा है । मनुष्य के मूल स्वभाव के सम्बन्ध में ही उत्पन्न होता है। मनुष्य सामाजिक धर्म : अहिंसा एक चेतन प्राणी है और एक चेतन प्राणी के रूप में उसका धर्म वैवक्तिक ममता के ये तत्व, जब बाह्य रूप में अभिव्यक्त मा स्वभाव पत्तसिक समत्व की उपलब्धि है। यहाँ चैतसिक होकर हमारे सामाजिक जीवन को प्रभावित करते हैं, तो वे हिंसा समस्व का तात्पर्य विभिन्न अनुकूल एवं प्रतिकूल अनुभूतियों में और संघर्ष को जन्म देते हैं। ममता के कारण आधिपत्य, संग्रह चेतना के स्तर पर अविचलित रहना है। दूसरे शब्दों में संगत और शोषण को वृत्तियों का उदय होता है। व्यक्ति अपने और का अर्थ शाता-द्रष्टा भाष में स्थित रहना है। वस्तुतः यह राग पराये की दीवारें खींचता है जिससे परिणामतः समाज-जीवन में और द्वेष के तस हमारी चेतना के समत्व को विचलित करते हैं संघर्ष और हिंसा का जन्म होता है और इन्हीं संघर्षों और हिंसक अत: राग-द्वेषजन्य विक्षोभों से रहित चेतना की समभाव में व्यवहारों के कारण सामाजिक जीवन का समत्व या सामाजिक अवस्थिति ही जगमा रत्न-स्वभात और गही गई है। शानि" भंग हो जाती है। आचासंग भूत्र में इसी सामाजिक वैयक्तिक धर्म : समता
जीवन-व्यवहार के दृष्टिकोण के आधार पर धर्म की एक दूसरी व्याख्याप्राप्ति सूत्र में आत्म स्वभाव की चर्चा करते हुए यह परिभाषा भी दी गई है, उसमें कहा गया है कि "भूतकाल में जो प्रश्न उठाया गया है कि आत्मा क्या है और उसका साध्य या अहंत हुए हैं, वर्तमान में हैं अथवा भविष्य में होंगे वे सब यह लक्ष्य क्या है? जैन आचार्यों ने इस सम्बन्ध में अपने उत्तर में प्रशापित करते हैं, व्याख्यामित करते हैं कि किसी प्राण, भूत, कहा है कि पारमा समत्व रूप है और उस समत्व को प्राप्त कर जीव या सत्त्व को पीड़ा नहीं देनी चाहिए, उनका पात नहीं लेना यही उसका लक्ष्य है। आचारांग सूत्र में इसी दृष्टिकोण के करना चाहिए, उनकी हिंसा नहीं करनी चाहिए। यही शाश्वत, आधार पर धर्म को समता के रूप में परिभाषित किया गया है। शुद्ध एवं नित्य धर्म है। उसमें कहा गया है कि "आर्यजनों ने समभाव में धर्म कहा है। इस प्रकार हग कह सकते हैं कि जैन आचार शास्त्रीय ग्रन्थों वस्तुतः समभाव के रूप में धर्म की यह परिभाषा धर्म की स्वभाव- में वैयक्तिक दृष्टि से समता और सामाजिक दृष्टि से अहिंसा को परक परिभाषा से भिन्न नहीं है । मानवीय एवं प्राणी प्रकृति यही धर्म कहा गया है। है कि वह सदैव ही तनावों से रहित समत्व की स्थिति को पाना धर्म सदाचार या सदगुण के रूप में, चाहता है । अतः यह कहा जा सकता है कि ये सभी तथ्य, जो प्रकारान्तर से अर्धमागधी और शौरसेनी जैन आगम में क्षमा, चेतना के इस समत्व को भंग करते हैं, विकार, विभाव या अधर्म सरलता, निर्लोभता, सत्यता, संयम आदि को भी धर्म के रूप में
१ धम्मो वत्यु सहायो, खमाविभायो य यसविहो धम्मो । रणयतयं च धम्मो, जीवाणां रक्षण धम्मो ॥
---बारस्स अणुवेक्खा (कात्तिकेय) ४७८ २ आया सामाइए, आया सामायस्स अट्ट।
-व्याख्याप्रशस्ति १/ ३ समपाए धम्मे आरिएहि पवेदए।
-आधारांग १/५/३/१५७ (च०, पृ. ३०) ४ से येमि-जे य असीता जे व पप्पणा मे य आगमेस्सा अरहंता भगवंता सध्ये ते एबमाइपखंति, एवं माति, एव पाणवेंति, एव
परुति-सव्वे पाणा जाप सम्वे सत्ता ण हतया, अज्जावेयध्वा, ण परिघतथ्या, ण परितावेयरवा, ण उद्देवेयव्या, एस धम्मे घुवे णितिए सासते, समेच्च लोग खेतन्नेहि पवेविते ।
--आचारांग १/४/१/१३१-१३२ (१०, पृ. ३३) -सूत्रकृतांग २/३/६८० (च.. २१६)