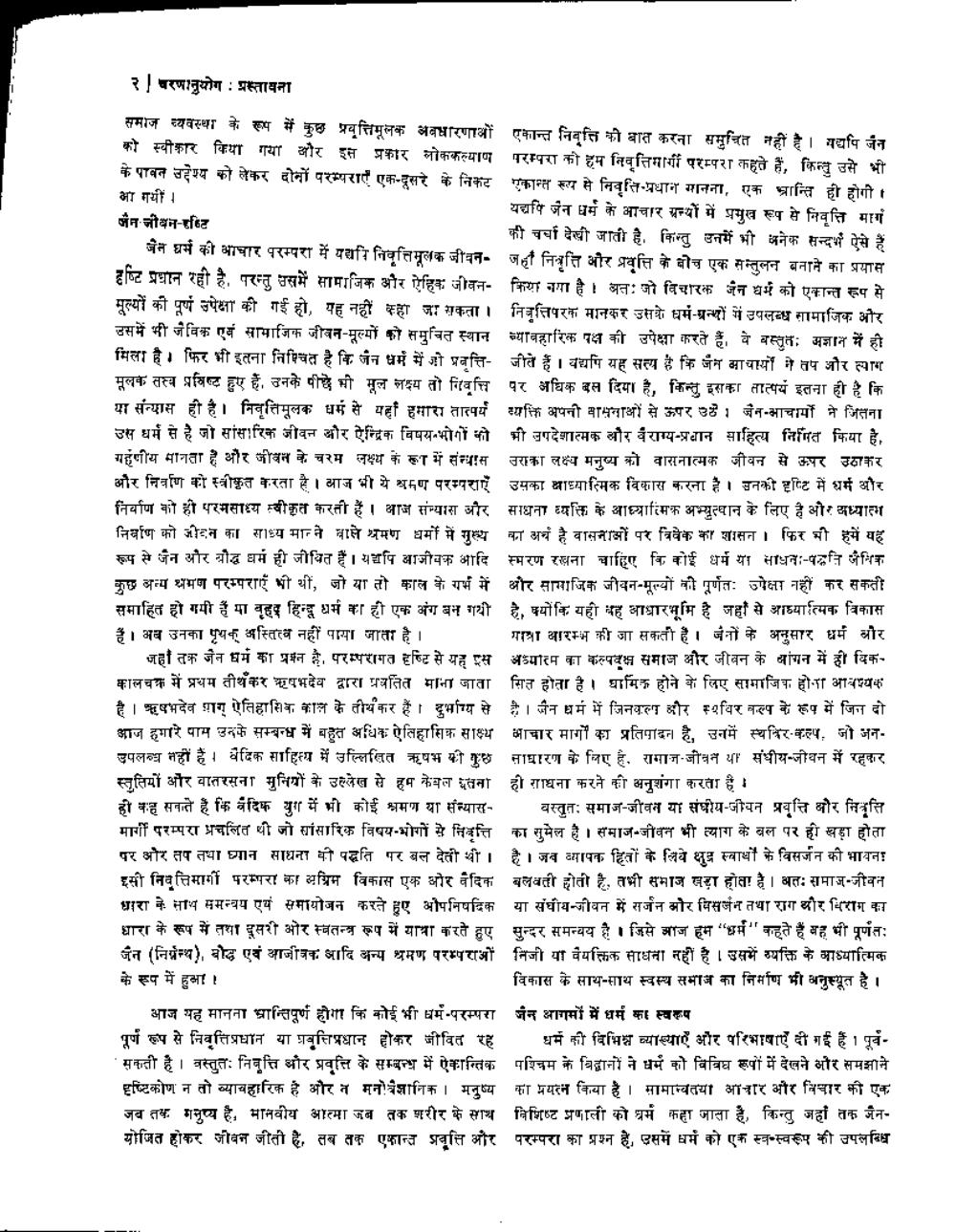________________
२ चरणानुयोग : प्रस्तावना समाज व्यवस्था के रूप में कुछ प्रवृत्तिमूलक अवधारणाओं एकान्त निवृत्ति की बात करना समुचित नहीं है। यद्यपि जैन को स्वीकार किया गया और इस प्रकार लोककल्याण परम्परा को हम निवृत्तिमार्गी परम्परा कहते हैं, किन्तु उसे भी के पावन उद्देश्य को लेकर दोनों परम्पराएं एक-दूसरे के निकट एकान्त रूप से निवृत्ति प्रधान मानना, एक भ्रान्ति ही होगी। आ गयीं।
यद्यपि जैन धर्म के आचार अन्यों में प्रमुख रूप से निवृत्ति मार्ग जैन-जीवन-दृष्टि
की चर्चा देखी जाती है, किन्तु उनमें भी अनेक सन्दर्भ ऐसे हैं जैन धर्म की भाचार परम्परा में यद्यपि निवृत्तिमूलक जीवन- जहाँ निवृत्ति और प्रवृत्ति के बीच एक सन्तुलन बनाने का प्रयास दृष्टि प्रधान रही है, परन्तु उसमें सामाजिक और ऐहिक जीवन- किया गया है। अतः जो विचारक जैन धर्म को एकान्त रूप से मूल्यों की पूर्ण उपेक्षा की गई हो, यह नहीं कहा जा सकता। निवृत्तिपरक मानकर उसके धर्म-ग्रन्थों में उपलब्ध सामाजिक और उसमें भी जैविक एवं सामाजिक जीवन-मूल्यों को समुचित स्थान व्यावहारिक पक्ष की उपेक्षा करते हैं, वे बस्तुतः अज्ञान में ही मिला है। फिर भी इतना निश्चित है कि जैन धर्म में जो प्रवृत्ति- जीते हैं । यद्यपि यह सत्य है कि जन आचार्यों ने तप और लाम मूलक तत्व प्रविष्ट हुए हैं, उनके पीछे भी मूल लक्ष्य तो निवृत्ति पर अधिक बल दिया है, किन्तु इसका तात्पर्य इतना ही है कि या संन्यास ही है। निवृत्तिमूलक धर्म से यहाँ हमारा तात्पर्य व्यक्ति अपनी वासनाओं से ऊपर उठे। जैन-आचार्यों ने जितना उस धर्म से है जो सांसारिक जीवन और ऐन्द्रिक विषय भोगों को भी उपदेशात्मक और वैराग्य-प्रधान साहित्य निर्मित किया है, गहणीय मानता है और जीवन के चरम लक्ष्य के रूप में संन्यास उराका लक्ष्य मनुष्य को वासनात्मक जीवन से ऊपर उठाकर
और निर्वाण को स्वीकृत करता है। आज भी ये श्रमण परम्पराएँ उसका बाध्यात्मिक विकास करना है। उनकी दृष्टि में धर्म और निर्वाण को ही परमसाध्य स्वीकृत करती हैं। आज संन्यास और साधना व्यक्ति के आध्यात्मिक अभ्युत्थान के लिए है और अध्यात्म निर्वाण को जीवन का साध्य मान्ने वाले श्रमण धर्मो में मुख्य का अर्थ है वासनाओं पर विवेक का शासन । फिर भी हमें यह रूप से जैन और बौद्ध धर्म ही जीवित हैं। यद्यपि आजीवक आदि स्मरण रखना चाहिए कि कोई धर्म या साधना-पदति जैविक कुछ अन्य श्रमण परम्पराएं भी थीं, जो या तो काल के गर्भ में और सामाजिक जीवन-मूल्यों की पूर्णतः उपेक्षा नहीं कर सकती समाहित हो गयी हैं या बृहद् हिन्दू धर्म का ही एक अंग बन गयी है, क्योंकि यही बह आधारभूमि है जहाँ से आध्यात्मिक विकास हैं। अब उनका पृथक् अस्तित्व नहीं पाया जाता है। यात्रा आरम्भ की जा सकती है। जैनों के अनुसार धर्म और
जहाँ तक जैन धर्म का प्रश्न है, परम्परागत दृष्टि से यह इस अध्यात्म का कल्पवृक्ष समाज और जीवन के आंगन में ही विककालचक्र में प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव द्वारा प्रवर्तित माना जाता सित होता है। धार्मिक होने के लिए सामाजिक होना आवश्यक है। ऋषभदेव शाग ऐतिहासिक काल के तीर्थकर हैं। दुर्भाग्य से है। जैन धर्म में जिनकाला और स्थविर बल्प के रूप में जिन दो आज हमारे पाम उनके सम्बन्ध में बहुत अधिक ऐतिहासिक साक्ष्य आचार मार्गों का प्रतिपादन है, उनमें स्थविर-कल्प, जो जनउपलब्ध नहीं हैं। वैदिक साहित्य में उल्लिखित ऋषभ की कुछ साधारण के लिए है, रामाज-जीवन या संधीय-जीवन में रहकर स्तुतियों और बातरसना मुनियों के उल्लेख से हम केवल इतना ही साधना करने की अनुशंगा करता है। ही कह सकते हैं कि वैदिक युग में भी कोई भ्रमण या संन्यास- वस्तुत: समाज-जीवन या संघीय-जीवन प्रवृत्ति बौर निवृत्ति मार्गी परम्परा प्रचलित थी जो सांसारिक विषय-भोगों से नित्ति का सुमेल है। समाज-जीवन भी त्याग के बल पर ही खड़ा होता पर और तप तथा ध्यान साधना वी पद्धति पर बल देती थी। है। जब व्यापक हितों के लिये क्षुद्र स्वार्थी के विसर्जन की भावना इसी निवृत्तिमार्गी परम्परा का अग्रिम विकास एक और वैदिक बलवती होती है, तभी समाज खड़ा होता है। अतः समाज-जीवन धारा के साथ समन्वय एवं समायोजन करते हुए ओपनिषदिक या संघीय-जीवन में सर्जन और विसर्जन तथा राग और चिराग का धारा के रूप में तथा दूसरी ओर स्वतन्त्र रूप में यात्रा करते हुए सुन्दर समन्वय है । जिसे आज हम "धर्म" कहते हैं मह भी पूर्णत: जैन (निम्रन्थ), बौद्ध एवं आजीवक आदि अन्य श्रमण परम्पराओं निजी या वैयक्तिक साधना नहीं है । उसमें व्यक्ति के आध्यात्मिक के रूप में हुआ।
विकास के साथ-साथ स्वस्थ समाज का निर्माण भी अनुस्यूत है। आज यह मानना भ्रान्तिपूर्ण होगा कि कोई भी धर्म-परम्परा जैन आगमों में धर्म का स्वरूप पूर्ण रूप से निवृत्तिप्रधान या प्रवृत्तिप्रधान होकर जीवित रह धर्म की विभिन्न व्याख्याएँ और परिभाषाएँ दी गई हैं। पूर्वसकती है। वस्तुतः निवृत्ति और प्रवृत्ति के सम्बन्ध में ऐकान्तिक पश्चिम के विद्वानों ने धर्म को विविध रूपों में देखने और समझाने दृष्टिकोण न तो व्यावहारिक है और न मनोवैज्ञानिक । मनुष्य का प्रयत्न किया है। सामान्यतया आचार और विचार की एक जब तक मनुष्य है, मानवीय आत्मा जब तक शरीर के साथ विशिष्ट प्रणाली को धर्म कहा जाता है, किन्तु जहाँ तक जनयोजित होकर जीवन जीती है, तब तक एकान्त प्रवृत्ति और परम्परा का प्रश्न है, उसमें धर्म को एक स्व-स्वरूप की उपलब्धि