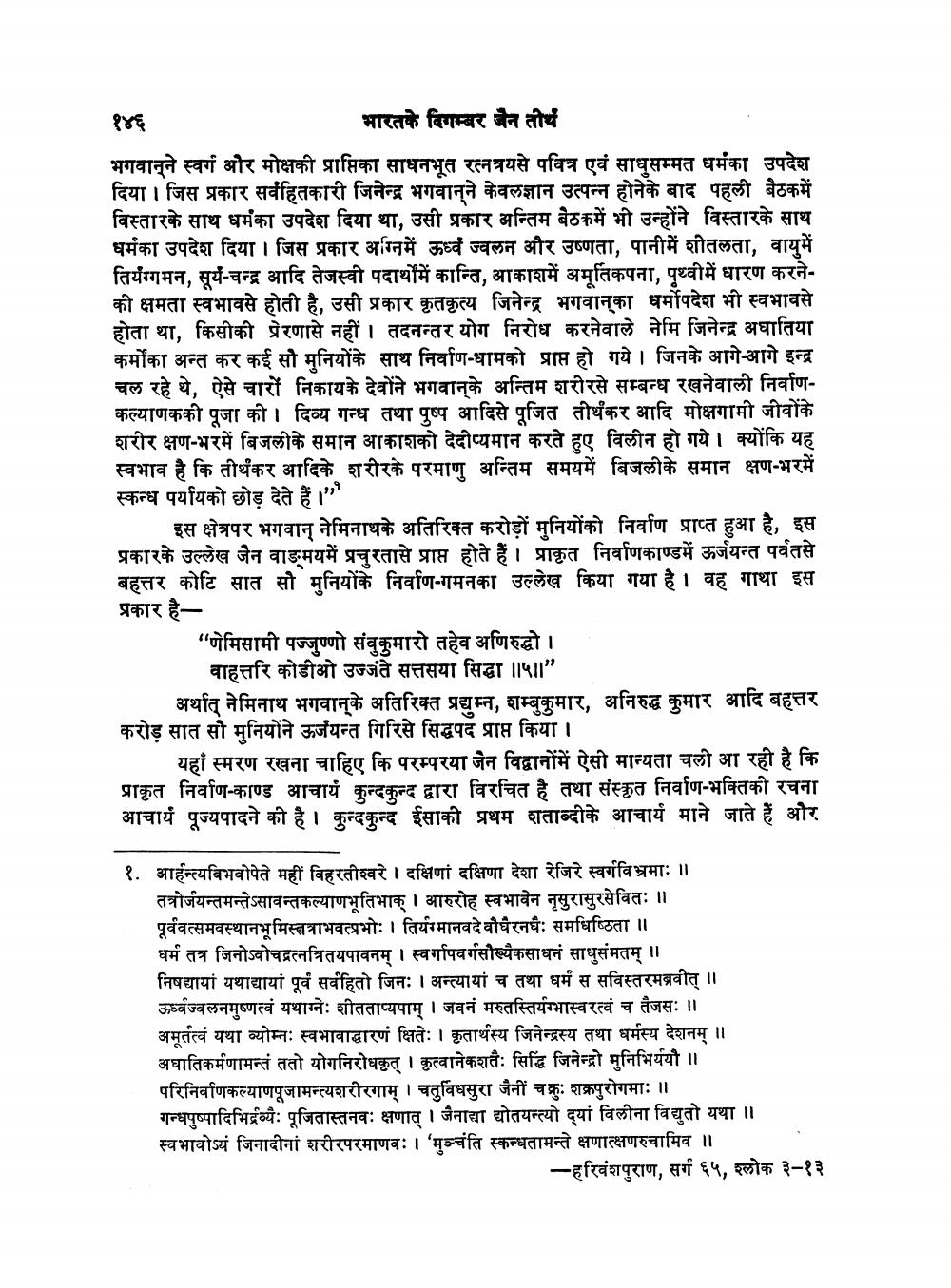________________
भारतके दिगम्बर जैन तीर्थ भगवान्ने स्वर्ग और मोक्षकी प्राप्तिका साधनभूत रत्नत्रयसे पवित्र एवं साधुसम्मत धर्मका उपदेश दिया। जिस प्रकार सर्वहितकारी जिनेन्द्र भगवान्ने केवलज्ञान उत्पन्न होनेके बाद पहली बैठकमें विस्तारके साथ धर्मका उपदेश दिया था, उसी प्रकार अन्तिम बैठकमें भी उन्होंने विस्तारके साथ धर्मका उपदेश दिया। जिस प्रकार अग्निमें ऊर्ध्व ज्वलन और उष्णता, पानीमें शीतलता, वायुमें तिर्यग्गमन, सूर्य-चन्द्र आदि तेजस्वी पदार्थों में कान्ति, आकाशमें अमूर्तिकपना, पृथ्वीमें धारण करनेकी क्षमता स्वभावसे होती है, उसी प्रकार कृतकृत्य जिनेन्द्र भगवान्का धर्मोपदेश भी स्वभावसे होता था, किसीकी प्रेरणासे नहीं। तदनन्तर योग निरोध करनेवाले नेमि जिनेन्द्र अघातिया कमौका अन्त कर कई सौ मुनियों के साथ निर्वाण-धामको प्राप्त हो गये। जिनके आगे-आगे इन्द्र चल रहे थे, ऐसे चारों निकायके देवोंने भगवान्के अन्तिम शरीरसे सम्बन्ध रखनेवाली निर्वाणकल्याणककी पूजा की। दिव्य गन्ध तथा पुष्प आदिसे पूजित तीर्थंकर आदि मोक्षगामी जीवोंके शरीर क्षण-भरमें बिजलीके समान आकाशको देदीप्यमान करते हुए विलीन हो गये। क्योंकि यह स्वभाव है कि तीर्थंकर आदिके शरीरके परमाणु अन्तिम समयमें बिजलीके समान क्षण-भरमें स्कन्ध पर्यायको छोड़ देते हैं।'
इस क्षेत्रपर भगवान् नेमिनाथके अतिरिक्त करोड़ों मुनियोंको निर्वाण प्राप्त हुआ है, इस रके उल्लेख जैन वाङमयमें प्रचरतासे प्राप्त होते हैं। प्राकृत निर्वाणकाण्डमें ऊर्जयन्त पर्वतसे बहत्तर कोटि सात सौ मुनियोंके निर्वाण-गमनका उल्लेख किया गया है। वह गाथा इस प्रकार है
"णेमिसामी पज्जुण्णो संवुकुमारो तहेव अणिरुद्धो।
वाहत्तरि कोडीओ उज्जते सत्तसया सिद्धा ॥५॥" अर्थात् नेमिनाथ भगवान्के अतिरिक्त प्रद्युम्न, शम्बुकुमार, अनिरुद्ध कुमार आदि बहत्तर करोड़ सात सौ मुनियोंने ऊर्जयन्त गिरिसे सिद्धपद प्राप्त किया।
यहाँ स्मरण रखना चाहिए कि परम्परया जैन विद्वानोंमें ऐसी मान्यता चली आ रही है कि प्राकृत निर्वाण-काण्ड आचार्य कुन्दकुन्द द्वारा विरचित है तथा संस्कृत निर्वाण-भक्तिकी रचना आचार्य पूज्यपादने की है । कुन्दकुन्द ईसाकी प्रथम शताब्दीके आचार्य माने जाते हैं और
१. आर्हन्त्यविभवोपेते महीं विहरतीश्वरे । दक्षिणां दक्षिणा देशा रेजिरे स्वर्गविभ्रमाः ॥
तत्रोर्जयन्तमन्तेऽसावन्तकल्याणभूतिभाक् । आरुरोह स्वभावेन नृसुरासुरसेवितः ॥ पूर्ववत्समवस्थानभूमिस्तत्राभवत्प्रभोः । तिर्यग्मानवदेवौधरनघः समधिष्ठिता ।। धर्म तत्र जिनोऽवोचद्रत्नत्रितयपावनम् । स्वर्गापवर्गसौख्यैकसाधनं साधुसंमतम् ।। निषद्यायां यथाद्यायां पूर्व सर्वहितो जिनः । अन्त्यायां च तथा धर्म स सविस्तरमब्रवीत् ।। ऊर्ध्वज्वलनमुष्णत्वं यथाग्नेः शीतताप्यपाम् । जवनं मरुतस्तिर्यग्भास्वरत्वं च तैजसः ॥ अमूर्तत्वं यथा व्योम्नः स्वभावाद्धारणं क्षितेः । कृतार्थस्य जिनेन्द्रस्य तथा धर्मस्य देशनम् ॥ अघातिकर्मणामन्तं ततो योगनिरोधकृत । कृत्वानेकशतैः सिद्धि जिनेन्द्रो मुनिभिर्ययौ ।। परिनिर्वाणकल्याणपूजामन्त्यशरीरगाम् । चतुर्विधसुरा जैनी चक्रुः शक्रपुरोगमाः ॥ गन्धपुष्पादिभिर्द्रव्यैः पूजितास्तनवः क्षणात् । जैनाद्या द्योतयन्त्यो द्यां विलीना विद्युतो यथा ॥ स्वभावोऽयं जिनादीनां शरीरपरमाणवः । 'मुञ्चति स्कन्धतामन्ते क्षणात्क्षणरुचामिव ॥
-हरिवंशपुराण, सर्ग ६५, श्लोक ३-१३