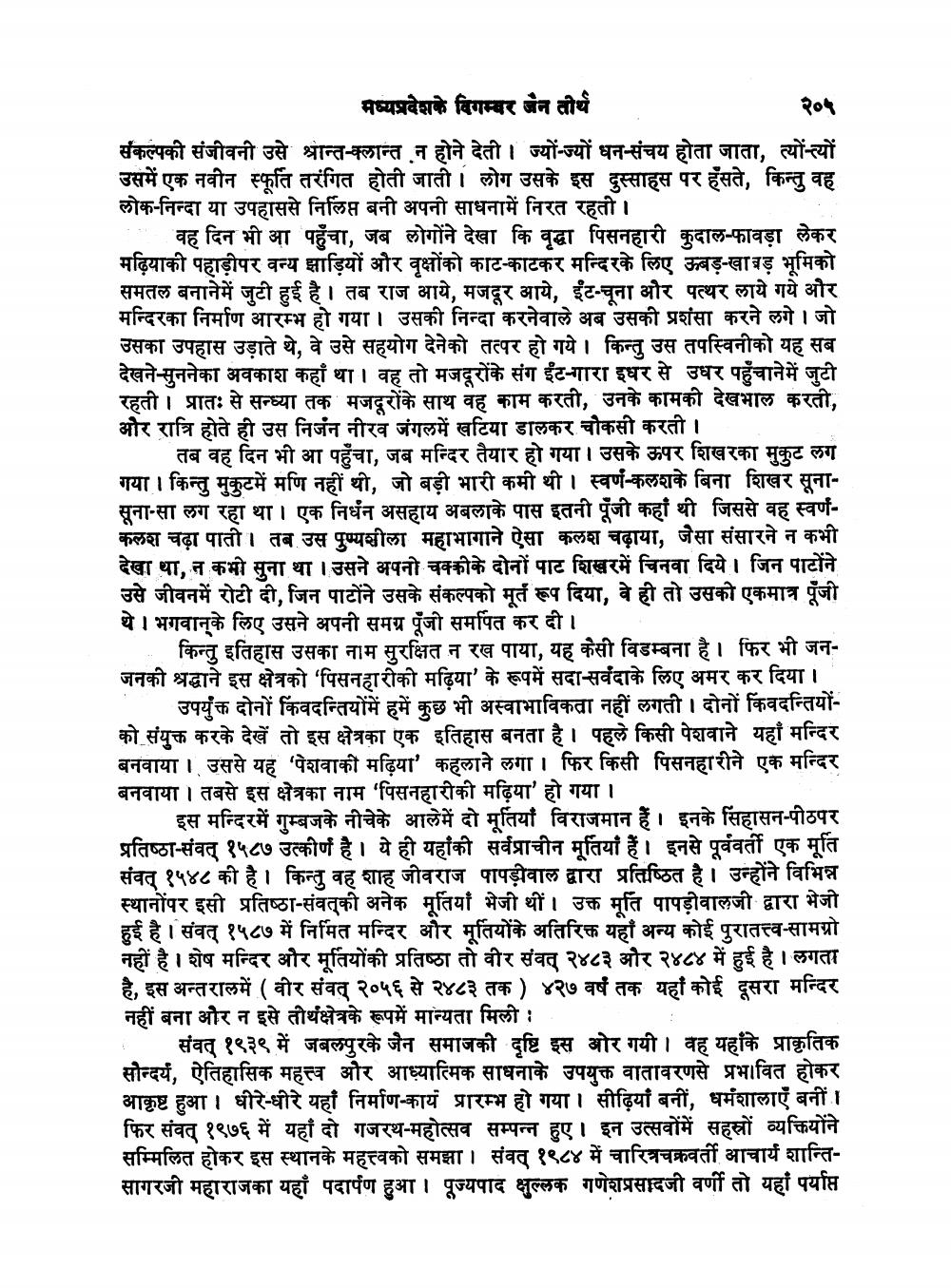________________
मध्यप्रदेशके विगम्बर जैन तीर्थ
२०५ संकल्पकी संजीवनी उसे श्रान्त-क्लान्त न होने देती। ज्यों-ज्यों धन-संचय होता जाता, त्यों-त्यों उसमें एक नवीन स्फूर्ति तरंगित होती जाती। लोग उसके इस दुस्साहस पर हँसते, किन्तु वह लोक-निन्दा या उपहाससे निलिप्त बनी अपनी साधनामें निरत रहती।
वह दिन भी आ पहँचा, जब लोगोंने देखा कि वद्धा पिसनहारी कदाल-फावडा लेकर मढ़ियाकी पहाड़ीपर वन्य झाड़ियों और वृक्षोंको काट-काटकर मन्दिरके लिए ऊबड़-खाबड़ भूमिको समतल बनानेमें जुटी हुई है। तब राज आये, मजदूर आये, इंट-चूना और पत्थर लाये गये और मन्दिरका निर्माण आरम्भ हो गया। उसकी निन्दा करनेवाले अब उसकी प्रशंसा करने लगे । जो उसका उपहास उड़ाते थे, वे उसे सहयोग देनेको तत्पर हो गये। किन्तु उस तपस्विनीको यह सब देखने-सुननेका अवकाश कहाँ था। वह तो मजदूरोंके संग ईंट-गारा इधर से उधर पहुंचानेमें जुटी रहती। प्रातः से सन्ध्या तक मजदूरोंके साथ वह काम करती, उनके कामकी देखभाल करती, और रात्रि होते ही उस निर्जन नीरव जंगलमें खटिया डालकर चौकसी करती।
तब वह दिन भी आ पहुंचा, जब मन्दिर तैयार हो गया। उसके ऊपर शिखरका मुकुट लग गया । किन्तु मुकुटमें मणि नहीं थी, जो बड़ी भारी कमी थी। स्वर्ण-कलशके बिना शिखर सूनासूना-सा लग रहा था। एक निधन असहाय अबलाके पास इतनी पूंजी कहां थी जिससे वह स्वर्णकलश चढ़ा पाती। तब उस पुण्यशीला महाभागाने ऐसा कलश चढ़ाया, जैसा संसारने न कभी देखा था, न कभी सुना था । उसने अपनी चक्कीके दोनों पाट शिखरमें चिनवा दिये। जिन पाटोंने उसे जीवनमें रोटी दी, जिन पाटोंने उसके संकल्पको मूर्त रूप दिया, वे ही तो उसको एकमात्र पूंजी थे। भगवान्के लिए उसने अपनी समग्र पूँजो समर्पित कर दी।
किन्तु इतिहास उसका नाम सुरक्षित न रख पाया, यह कैसी विडम्बना है। फिर भी जनजनकी श्रद्धाने इस क्षेत्रको 'पिसनहारीको मढ़िया' के रूपमें सदा-सर्वदाके लिए अमर कर दिया।
उपर्युक्त दोनों किंवदन्तियोंमें हमें कुछ भी अस्वाभाविकता नहीं लगती। दोनों किंवदन्तियोंको संयुक्त करके देखें तो इस क्षेत्रका एक इतिहास बनता है। पहले किसी पेशवाने यहाँ मन्दिर बनवाया। उससे यह 'पेशवाको मढ़िया' कहलाने लगा। फिर किसी पिसनहारीने एक मन्दिर बनवाया। तबसे इस क्षेत्रका नाम 'पिसनहारीकी मढ़िया' हो गया।
इस मन्दिरमें गुम्बजके नीचेके आले में दो मूर्तियां विराजमान हैं। इनके सिंहासन-पीठपर प्रतिष्ठा-संवत् १५८७ उत्कीर्ण है। ये ही यहांकी सर्वप्राचीन मूर्तियां हैं। इनसे पूर्ववर्ती एक मूर्ति संवत् १५४८ की है। किन्तु वह शाह जीवराज पापड़ीवाल द्वारा प्रतिष्ठित है। उन्होंने विभिन्न स्थानोंपर इसी प्रतिष्ठा-संवत्की अनेक मूर्तियां भेजी थीं। उक्त मूर्ति पापड़ीवालजी द्वारा भेजी हुई है। संवत् १५८७ में निर्मित मन्दिर और मूर्तियोंके अतिरिक्त यहाँ अन्य कोई पुरातत्त्व-सामग्रो नहीं है। शेष मन्दिर और मूर्तियोंकी प्रतिष्ठा तो वीर संवत् २४८३ और २४८४ में हुई है । लगता है, इस अन्तरालमें ( वीर संवत् २०५६ से २४८३ तक ) ४२७ वर्ष तक यहां कोई दूसरा मन्दिर नहीं बना और न इसे तीर्थक्षेत्रके रूपमें मान्यता मिली। । संवत् १९३९ में जबलपुरके जैन समाजकी दृष्टि इस ओर गयी। वह यहाँके प्राकृतिक सौन्दर्य, ऐतिहासिक महत्त्व और आध्यात्मिक साधनाके उपयुक्त वातावरणसे प्रभावित होकर आकृष्ट हुआ। धीरे-धीरे यहाँ निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया। सीढ़ियां बनीं, धर्मशालाएं बनीं। फिर संवत् १९७६ में यहां दो गजरथ-महोत्सव सम्पन्न हुए। इन उत्सवोंमें सहस्रों व्यक्तियोंने सम्मिलित होकर इस स्थानके महत्त्वको समझा। संवत् १९८४ में चारित्रचक्रवर्ती आचार्य शान्तिसागरजी महाराजका यहाँ पदार्पण हुआ। पूज्यपाद क्षुल्लक गणेशप्रसादजी वर्णी तो यहां पर्याप्त