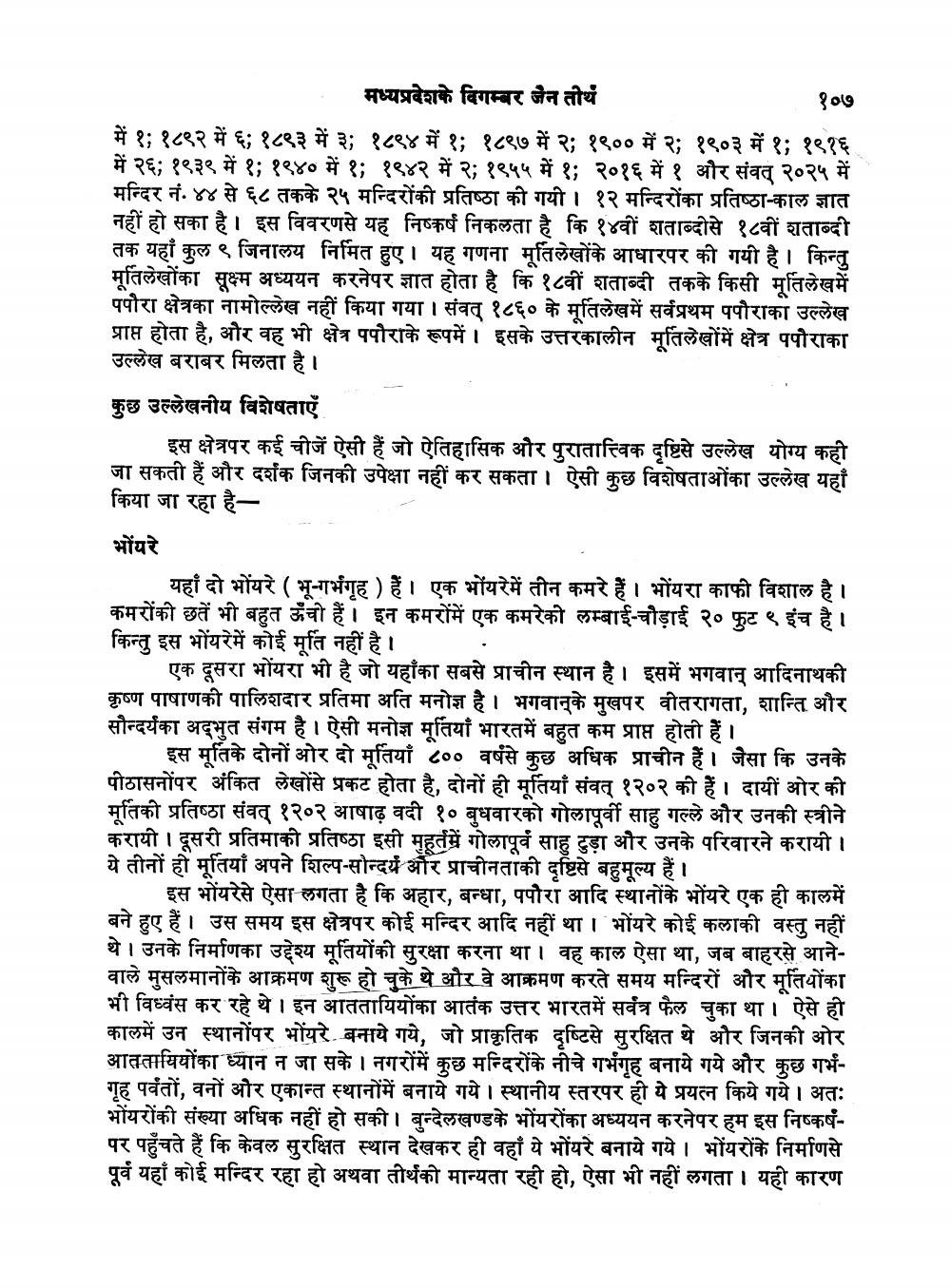________________
मध्यप्रदेशके दिगम्बर जैन तीर्थ
१०७ में १; १८९२ में ६; १८९३ में ३; १८९४ में १; १८९७ में २; १९०० में २; १९०३ में १; १९१६ में २६; १९३९ में १; १९४० में १; १९४२ में २; १९५५ में १; २०१६ में १ और संवत् २०२५ में मन्दिर नं. ४४ से ६८ तकके २५ मन्दिरोंकी प्रतिष्ठा की गयी। १२ मन्दिरोंका प्रतिष्ठा-काल ज्ञात नहीं हो सका है। इस विवरणसे यह निष्कर्ष निकलता है कि १४वीं शताब्दीसे १८वीं शताब्दी तक यहाँ कुल ९ जिनालय निर्मित हुए। यह गणना मूर्तिलेखोंके आधारपर की गयी है। किन्तु मूर्तिलेखोंका सूक्ष्म अध्ययन करनेपर ज्ञात होता है कि १८वीं शताब्दी तकके किसी मूर्तिलेखमें पपौरा क्षेत्रका नामोल्लेख नहीं किया गया। संवत् १८६० के मूर्तिलेखमें सर्वप्रथम पपौराका उल्लेख प्राप्त होता है, और वह भी क्षेत्र पपौराके रूपमें। इसके उत्तरकालीन मूर्तिलेखोंमें क्षेत्र पपौराका उल्लेख बराबर मिलता है। कुछ उल्लेखनीय विशेषताएँ
इस क्षेत्रपर कई चीजें ऐसी हैं जो ऐतिहासिक और पुरातात्त्विक दृष्टिसे उल्लेख योग्य कही जा सकती हैं और दर्शक जिनकी उपेक्षा नहीं कर सकता। ऐसी कुछ विशेषताओंका उल्लेख यहाँ किया जा रहा हैभोयरे
__यहाँ दो भोयरे ( भू-गर्भगृह ) हैं। एक भोयरे में तीन कमरे हैं। भोयरा काफी विशाल है। कमरोंकी छतें भी बहुत ऊँची हैं। इन कमरोंमें एक कमरेको लम्बाई-चौड़ाई २० फुट ९ इंच है। किन्तु इस भोयरेमें कोई मूर्ति नहीं है।
एक दूसरा भोयरा भी है जो यहाँका सबसे प्राचीन स्थान है। इसमें भगवान् आदिनाथकी कृष्ण पाषाणकी पालिशदार प्रतिमा अति मनोज्ञ है। भगवान्के मुखपर वीतरागता, शान्ति और सौन्दर्यका अद्भुत संगम है । ऐसी मनोज्ञ मूर्तियाँ भारतमें बहुत कम प्राप्त होती हैं।
इस मूर्तिके दोनों ओर दो मूर्तियाँ ८०० वर्षसे कुछ अधिक प्राचीन हैं। जैसा कि उनके पीठासनोंपर अंकित लेखोंसे प्रकट होता है, दोनों ही मूर्तियां संवत् १२०२ की हैं। दायीं ओर की मूर्तिकी प्रतिष्ठा संवत् १२०२ आषाढ़ वदी १० बुधवारको गोलापूर्वी साहु गल्ले और उनकी स्त्रीने करायी। दूसरी प्रतिमाको प्रतिष्ठा इसी मुहूर्तमें गोलापूर्व साहु टुड़ा और उनके परिवारने करायी। ये तीनों ही मूर्तियाँ अपने शिल्प-सौन्दर्य और प्राचीनताकी दृष्टिसे बहुमूल्य हैं।
इस भोयरेसे ऐसा लगता है कि अहार, बन्धा, पपौरा आदि स्थानोंके भोयरे एक ही कालमें बने हुए हैं। उस समय इस क्षेत्रपर कोई मन्दिर आदि नहीं था। भोयरे कोई कलाकी वस्तु नहीं थे। उनके निर्माणका उद्देश्य मूर्तियोंकी सुरक्षा करना था। वह काल ऐसा था, जब बाहरसे आनेवाले मुसलमानोंके आक्रमण शुरू हो चुके थे और वे आक्रमण करते समय मन्दिरों और मूर्तियोंका भी विध्वंस कर रहे थे। इन आततायियोंका आतंक उत्तर भारतमें सर्वत्र फैल चुका था। ऐसे ही कालमें उन स्थानोंपर भोयरे बनाये गये, जो प्राकृतिक दृष्टिसे सुरक्षित थे और जिनकी ओर आततायियोंका ध्यान न जा सके । नगरोंमें कुछ मन्दिरोंके नीचे गर्भगृह बनाये गये और कुछ गर्भगृह पर्वतों, वनों और एकान्त स्थानोंमें बनाये गये । स्थानीय स्तरपर ही ये प्रयत्न किये गये। अतः भोंयरोंकी संख्या अधिक नहीं हो सकी। बुन्देलखण्डके भोंयरोंका अध्ययन करनेपर हम इस निष्कर्षपर पहुंचते हैं कि केवल सुरक्षित स्थान देखकर ही वहाँ ये भोयरे बनाये गये । भोंयरोंके निर्माणसे पूर्व यहाँ कोई मन्दिर रहा हो अथवा तीर्थको मान्यता रही हो, ऐसा भी नहीं लगता। यही कारण