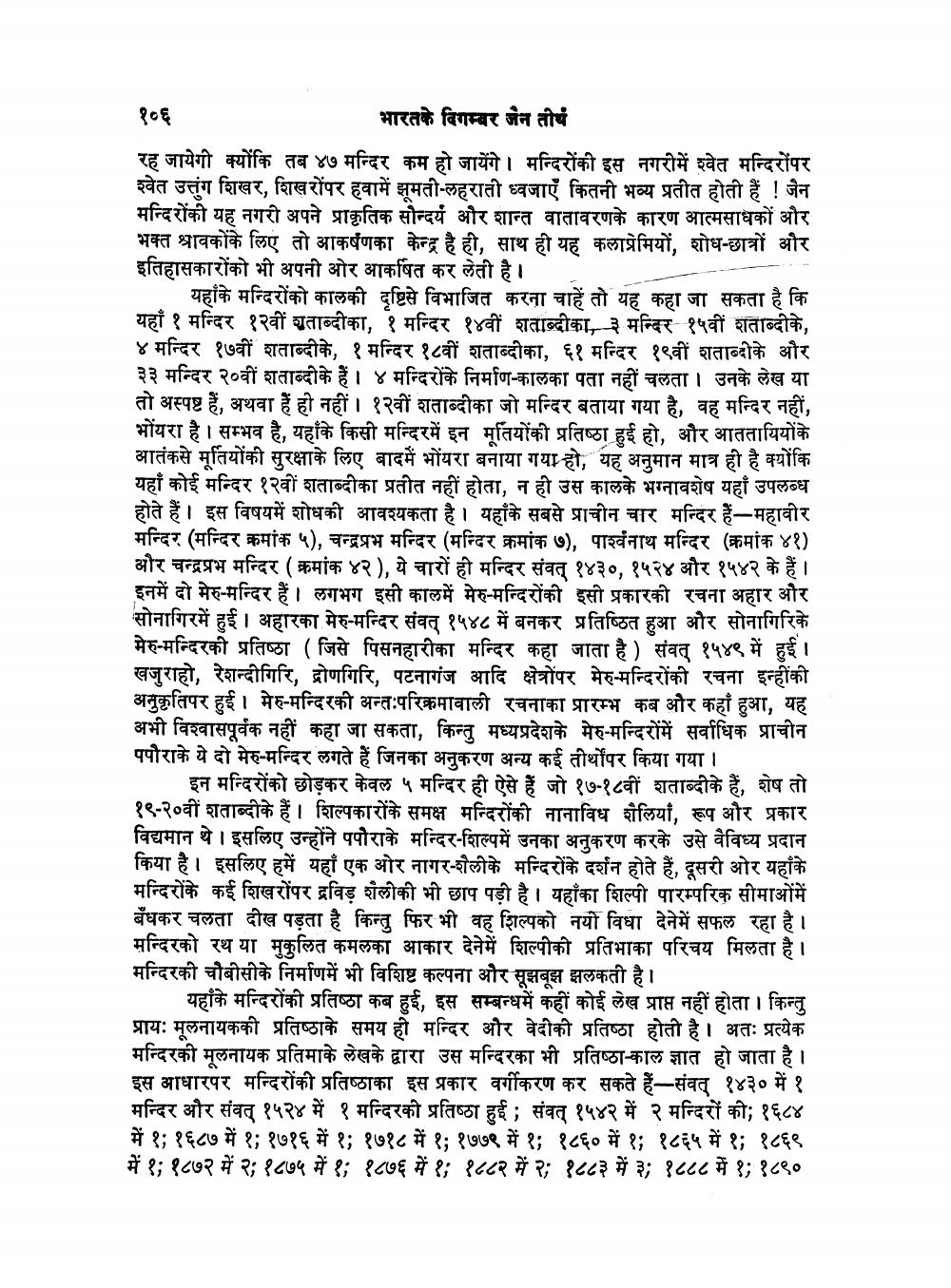________________
१०६
भारतके दिगम्बर जैन तीर्थ रह जायेगी क्योंकि तब ४७ मन्दिर कम हो जायेंगे। मन्दिरोंकी इस नगरीमें श्वेत मन्दिरोंपर श्वेत उत्तुंग शिखर, शिखरोंपर हवा में झूमती-लहराती ध्वजाएं कितनी भव्य प्रतीत होती हैं ! जैन मन्दिरोंकी यह नगरी अपने प्राकृतिक सौन्दर्य और शान्त वातावरणके कारण आत्मसाधकों और भक्त श्रावकोंके लिए तो आकर्षणका केन्द्र है ही, साथ ही यह कलाप्रेमियों, शोध-छात्रों और इतिहासकारोंको भी अपनी ओर आकर्षित कर लेती है।
यहाँके मन्दिरोंको कालकी दृष्टिसे विभाजित करना चाहें तो यह कहा जा सकता है कि यहाँ १ मन्दिर १२वीं शताब्दीका, १ मन्दिर १४वीं शताब्दीका, ३ मन्दिर १५वीं शताब्दीके, ४ मन्दिर १७वीं शताब्दीके, १ मन्दिर १८वीं शताब्दीका, ६१ मन्दिर १९वीं शताब्दीके और ३३ मन्दिर २०वीं शताब्दीके हैं। ४ मन्दिरोंके निर्माण-कालका पता नहीं चलता। उनके लेख या तो अस्पष्ट हैं, अथवा हैं ही नहीं। १२वीं शताब्दीका जो मन्दिर बताया गया है, वह मन्दिर नहीं, भोयरा है। सम्भव है, यहाँके किसी मन्दिरमें इन मूर्तियोंकी प्रतिष्ठा हुई हो, और आततायियोंके आतंकसे मूर्तियोंकी सुरक्षाके लिए बादमें भोयरा बनाया गया हो, यह अनुमान मात्र ही है क्योंकि यहाँ कोई मन्दिर १२वीं शताब्दीका प्रतीत नहीं होता, न ही उस कालके भग्नावशेष यहाँ उपलब्ध होते हैं। इस विषयमें शोधकी आवश्यकता है। यहाँके सबसे प्राचीन चार मन्दिर हैं-महावीर मन्दिर (मन्दिर क्रमांक ५), चन्द्रप्रभ मन्दिर (मन्दिर क्रमांक ७), पाश्र्वनाथ मन्दिर (क्रमांक ४१) और चन्द्रप्रभ मन्दिर (क्रमांक ४२), ये चारों ही मन्दिर संवत् १४३०, १५२४ और १५४२ के हैं। इनमें दो मेरु-मन्दिर हैं। लगभग इसी कालमें मेरु-मन्दिरोंकी इसी प्रकारकी रचना अहार और सोनागिरमें हुई। अहारका मेरु-मन्दिर संवत् १५४८ में बनकर प्रतिष्ठित हुआ और सोनागिरिके मेरु-मन्दिरकी प्रतिष्ठा ( जिसे पिसनहारीका मन्दिर कहा जाता है ) संवत् १५४९ में हुई। खजुराहो, रेशन्दीगिरि, द्रोणगिरि, पटनागंज आदि क्षेत्रोंपर मेरु-मन्दिरोंकी रचना इन्हींकी अनुकृतिपर हुई। मेरु-मन्दिरकी अन्तःपरिक्रमावाली रचनाका प्रारम्भ कब और कहाँ हुआ, यह अभी विश्वासपूर्वक नहीं कहा जा सकता, किन्तु मध्यप्रदेशके मेरु-मन्दिरोंमें सर्वाधिक प्राचीन पपौराके ये दो मेरु-मन्दिर लगते हैं जिनका अनुकरण अन्य कई तीर्थोपर किया गया।
इन मन्दिरोंको छोड़कर केवल ५ मन्दिर ही ऐसे हैं जो १७-१८वीं शताब्दीके हैं, शेष तो १९-२०वीं शताब्दीके हैं। शिल्पकारोंके समक्ष मन्दिरोंकी नानाविध शैलियाँ, रूप और प्रकार विद्यमान थे। इसलिए उन्होंने पपौराके मन्दिर-शिल्पमें उनका अनुकरण करके उसे वैविध्य प्रदान किया है। इसलिए हमें यहाँ एक ओर नागर-शैलीके मन्दिरोंके दर्शन होते हैं, दूसरी ओर यहाँके मन्दिरोंके कई शिखरोंपर द्रविड़ शैलीकी भी छाप पड़ी है। यहाँका शिल्पी पारम्परिक सीमाओंमें बँधकर चलता दीख पड़ता है किन्तु फिर भी वह शिल्पको नयो विधा देनेमें सफल रहा है। मन्दिरको रथ या मुकुलित कमलका आकार देने में शिल्पीकी प्रतिभाका परिचय मिलता है। मन्दिरकी चौबीसीके निर्माणमें भी विशिष्ट कल्पना और सूझबूझ झलकती है।
यहाँके मन्दिरोंकी प्रतिष्ठा कब हुई, इस सम्बन्धमें कहीं कोई लेख प्राप्त नहीं होता। किन्तु प्रायः मूलनायककी प्रतिष्ठाके समय ही मन्दिर और वेदीकी प्रतिष्ठा होती है। अतः प्रत्येक मन्दिरकी मलनायक प्रतिमाके लेखके द्वारा उस मन्दिरका भी प्रतिष्ठा-काल ज्ञात हो जाता है। इस आधारपर मन्दिरोंकी प्रतिष्ठाका इस प्रकार वर्गीकरण कर सकते हैं-संवत् १४३० में १ मन्दिर और संवत् १५२४ में १ मन्दिरको प्रतिष्ठा हुई ; संवत् १५४२ में २ मन्दिरों की; १६८४ में १; १६८७ में १; १७१६ में १; १७१८ में १, १७७९ में १; १८६० में १; १८६५ में १; १८६९ में १; १८७२ में २; १८७५ में १; १८७६ में १, १८८२ में २; १८८३ में ३; १८८८ में १; १८९०