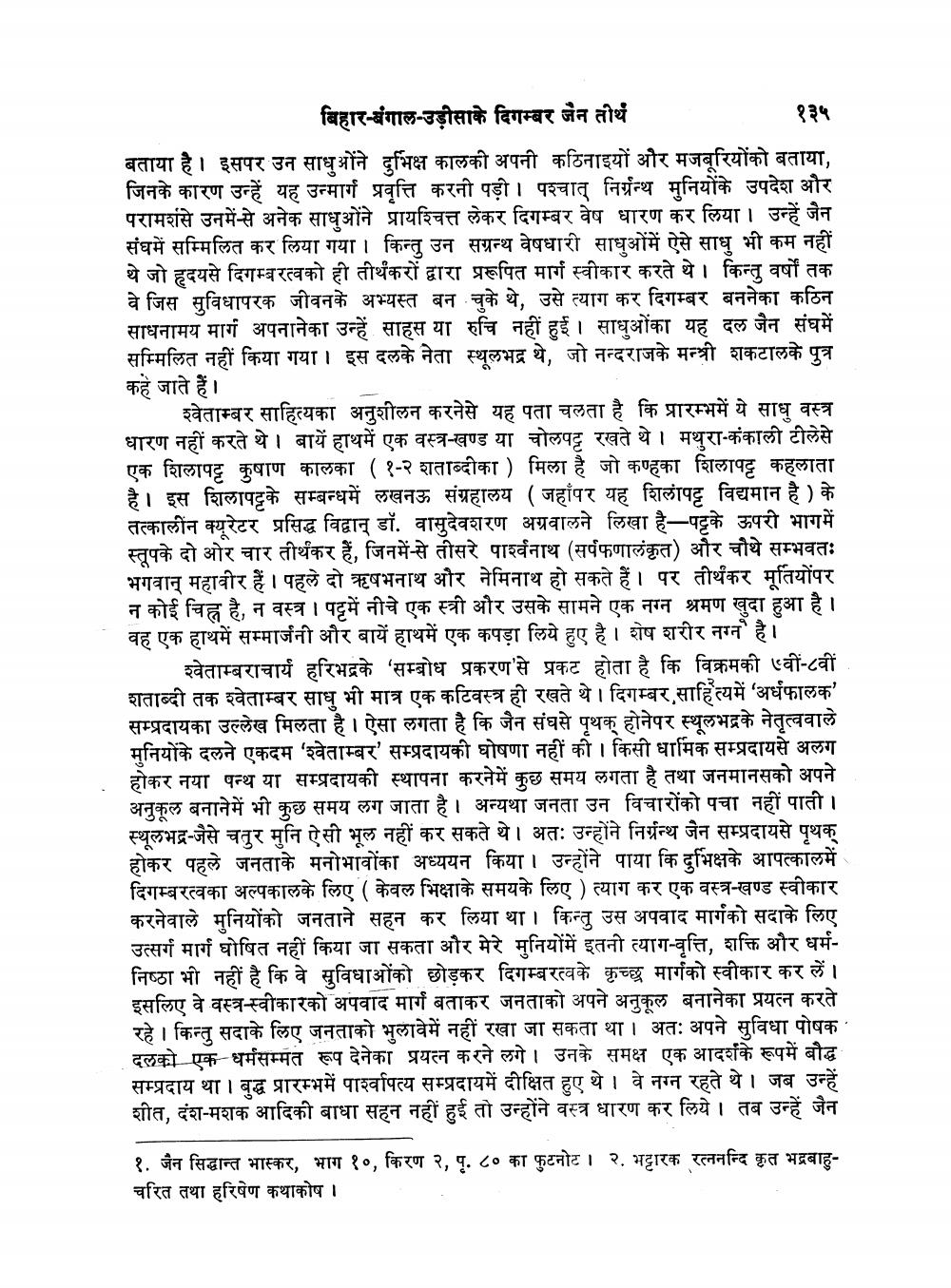________________
बिहार-बंगाल-उड़ीसाके दिगम्बर जैन तीर्थ
१३५ बताया है। इसपर उन साधुओंने दुभिक्ष कालकी अपनी कठिनाइयों और मजबूरियोंको बताया,
नके कारण उन्हें यह उन्मार्ग प्रवत्ति करनी पड़ी। पश्चात् निर्ग्रन्थ मनियोंके उपदेश और परामर्शसे उनमें से अनेक साधुओंने प्रायश्चित्त लेकर दिगम्बर वेष धारण कर लिया। उन्हें जैन संघमें सम्मिलित कर लिया गया। किन्तु उन सग्रन्थ वेषधारी साधुओंमें ऐसे साधु भी कम नहीं थे जो हृदयसे दिगम्बरत्वको ही तीर्थंकरों द्वारा प्ररूपित मार्ग स्वीकार करते थे। किन्तु वर्षों तक वे जिस सुविधापरक जीवनके अभ्यस्त बन चुके थे, उसे त्याग कर दिगम्बर बननेका कठिन साधनामय मार्ग अपनानेका उन्हें साहस या रुचि नहीं हुई। साधुओंका यह दल जैन संघमें सम्मिलित नहीं किया गया। इस दलके नेता स्थलभद्र थे, जो नन्दराजके मन्त्री शकटालके पूत्र कहे जाते हैं।
श्वेताम्बर साहित्यका अनुशीलन करनेसे यह पता चलता है कि प्रारम्भमें ये साधु वस्त्र धारण नहीं करते थे। बायें हाथमें एक वस्त्र-खण्ड या चोलपट्ट रखते थे। मथुरा-कंकाली टीलेसे एक शिलापट्ट कुषाण कालका (१-२ शताब्दीका ) मिला है जो कण्हका शिलापट्ट कहलाता है। इस शिलापट्टके सम्बन्धमें लखनऊ संग्रहालय ( जहाँपर यह शिलापट्ट विद्यमान है ) के तत्कालीन क्यूरेटर प्रसिद्ध विद्वान् डॉ. वासूदेवशरण अग्रवालने लिखा है-पटके ऊपरी भागमें स्तूपके दो ओर चार तीर्थंकर हैं, जिनमें से तीसरे पार्श्वनाथ (सर्पफणालंकृत) और चौथे सम्भवतः भगवान् महावीर हैं। पहले दो ऋषभनाथ और नेमिनाथ हो सकते हैं। पर तीर्थंकर मूर्तियोंपर न कोई चिह्न है, न वस्त्र । पट्टमें नीचे एक स्त्री और उसके सामने एक नग्न श्रमण खुदा हुआ है। वह एक हाथमें सम्मार्जनी और बायें हाथमें एक कपड़ा लिये हुए है। शेष शरीर नग्न' है।
__ श्वेताम्बराचार्य हरिभद्रके 'सम्बोध प्रकरण'से प्रकट होता है कि विक्रमकी ७वी-८वीं शताब्दी तक श्वेताम्बर साधु भी मात्र एक कटिवस्त्र ही रखते थे। दिगम्बर साहित्यमें 'अर्धफालक' सम्प्रदायका उल्लेख मिलता है। ऐसा लगता है कि जैन संघसे पृथक् होनेपर स्थूलभद्रके नेतृत्ववाले मुनियोंके दलने एकदम 'श्वेताम्बर' सम्प्रदायकी घोषणा नहीं की। किसी धार्मिक सम्प्रदायसे अलग होकर नया पन्थ या सम्प्रदायकी स्थापना करने में कुछ समय लगता है तथा जनमानसको अपने अनुकूल बनाने में भी कुछ समय लग जाता है। अन्यथा जनता उन विचारोंको पचा नहीं पाती। स्थूलभद्र-जैसे चतुर मुनि ऐसी भूल नहीं कर सकते थे। अतः उन्होंने निर्ग्रन्थ जैन सम्प्रदायसे पृथक होकर पहले जनताके मनोभावोंका अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि दुर्भिक्षके आपत्कालमें दिगम्बरत्वका अल्पकालके लिए ( केवल भिक्षाके समयके लिए ) त्याग कर एक वस्त्र-खण्ड स्वीकार करनेवाले मुनियोंको जनताने सहन कर लिया था। किन्तु उस अपवाद मार्गको सदाके लिए उत्सर्ग मार्ग घोषित नहीं किया जा सकता और मेरे मुनियोंमें इतनी त्याग-वृत्ति, शक्ति और धर्मनिष्ठा भी नहीं है कि वे सुविधाओंको छोड़कर दिगम्बरत्वके कृच्छ्र मार्गको स्वीकार कर लें। इसलिए वे वस्त्र-स्वीकारको अपवाद मार्ग बताकर जनताको अपने अनुकूल बनानेका प्रयत्न करते रहे । किन्तु सदाके लिए जनताको भुलावेमें नहीं रखा जा सकता था। अतः अपने सुविधा पोषक दलको एक धर्मसम्मत रूप देनेका प्रयत्न करने लगे। उनके समक्ष एक आदर्शके रूपमें बौद्ध सम्प्रदाय था। बुद्ध प्रारम्भमें पापित्य सम्प्रदायमें दीक्षित हुए थे। वे नग्न रहते थे। जब उन्हें शीत, दंश-मशक आदिकी बाधा सहन नहीं हुई तो उन्होंने वस्त्र धारण कर लिये। तब उन्हें जैन
१. जैन सिद्धान्त भास्कर, भाग १०, किरण २, पृ. ८० का फुटनोट । २. भट्टारक रत्ननन्दि कृत भद्रबाहुचरित तथा हरिषेण कथाकोष ।