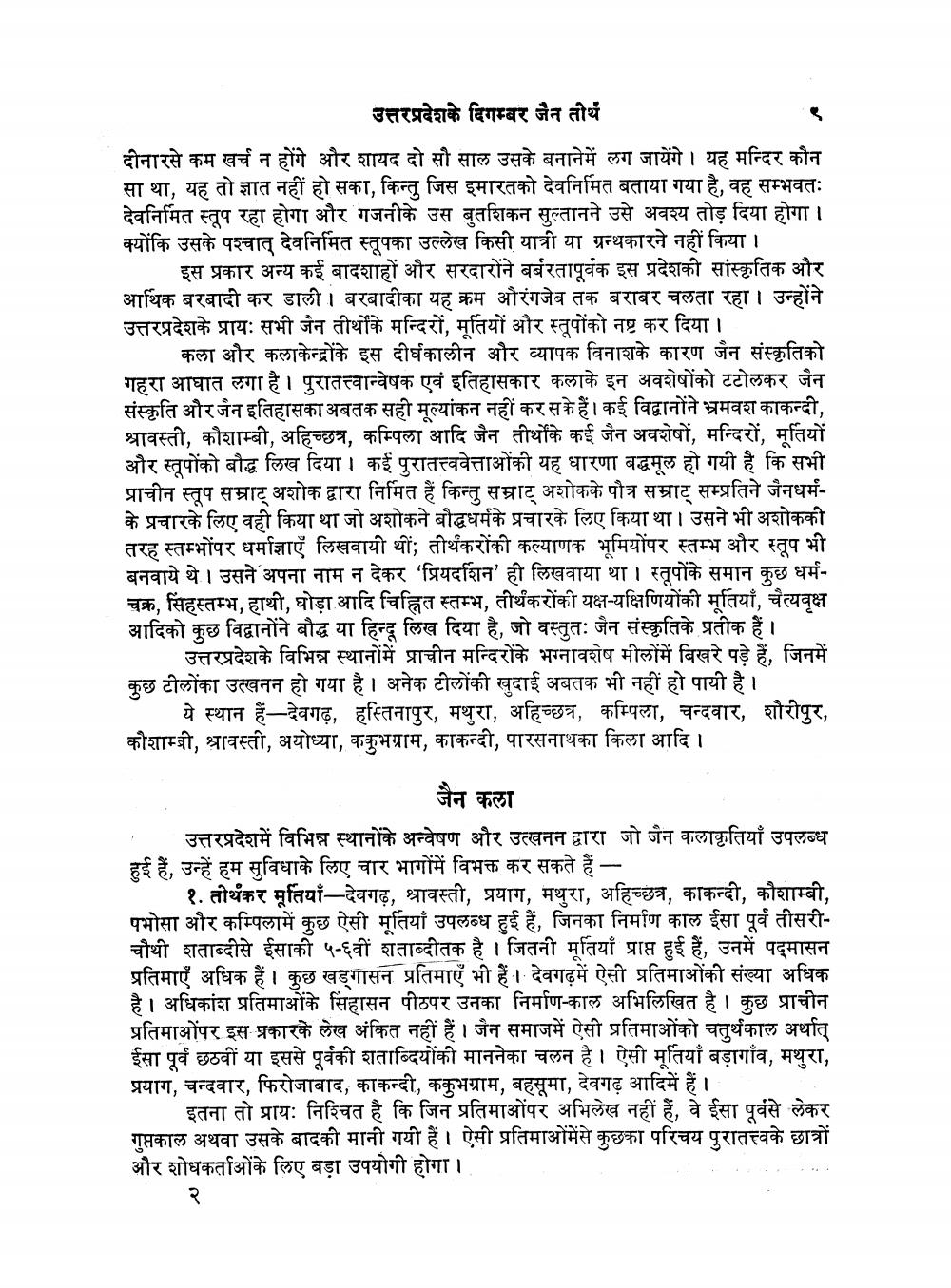________________
उत्तरप्रदेशके दिगम्बर जैन तीर्थ
दीनारसे कम खर्च न होंगे और शायद दो सौ साल उसके बनानेमें लग जायेंगे। यह मन्दिर कौन सा था, यह तो ज्ञात नहीं हो सका, किन्तु जिस इमारतको देवनिर्मित बताया गया है, वह सम्भवतः देवनिर्मित स्तूप रहा होगा और गजनीके उस बुतशिकन सुल्तानने उसे अवश्य तोड़ दिया होगा। क्योंकि उसके पश्चात् देवनिर्मित स्तूपका उल्लेख किसी यात्री या ग्रन्थकारने नहीं किया।
इस प्रकार अन्य कई बादशाहों और सरदारोंने बर्बरतापूर्वक इस प्रदेशको सांस्कृतिक और आर्थिक बरबादी कर डाली। बरबादीका यह क्रम औरंगजेब तक बराबर चलता रहा। उन्होंने उत्तरप्रदेशके प्रायः सभी जैन तीर्थोके मन्दिरों, मूर्तियों और स्तूपोंको नष्ट कर दिया।
कला और कलाकेन्द्रोंके इस दीर्घकालीन और व्यापक विनाशके कारण जैन संस्कृतिको गहरा आघात लगा है। पुरातत्त्वान्वेषक एवं इतिहासकार कलाके इन अवशेषोंको टटोलकर जैन संस्कृति और जैन इतिहासका अबतक सही मूल्यांकन नहीं कर सके हैं। कई विद्वानोंने भ्रमवश काकन्दी, श्रावस्ती, कौशाम्बी, अहिच्छत्र, कम्पिला आदि जैन तीर्थोके कई जैन अवशेषों, मन्दिरों, मूर्तियों और स्तपोंको बौद्ध लिख दिया। कई पुरातत्त्ववेत्ताओंकी यह धारणा बद्धमल हो गयी है कि सभी प्राचीन स्तूप सम्राट अशोक द्वारा निर्मित हैं किन्तु सम्राट अशोकके पौत्र सम्राट् सम्प्रतिने जैनधर्मके प्रचारके लिए वही किया था जो अशोकने बौद्धधर्मके प्रचारके लिए किया था। उसने भी अशोककी तरह स्तम्भोंपर धर्माज्ञाएँ लिखवायी थीं; तीर्थंकरोंकी कल्याणक भूमियोंपर स्तम्भ और स्तूप भी बनवाये थे। उसने अपना नाम न देकर 'प्रियदर्शिन' ही लिखवाया था। स्तूपोंके समान कुछ धर्मचक्र, सिंहस्तम्भ, हाथी, घोड़ा आदि चिह्नित स्तम्भ, तीर्थंकरोंकी यक्ष-यक्षिणियोंकी मूर्तियाँ, चैत्यवृक्ष आदिको कुछ विद्वानोंने बौद्ध या हिन्दू लिख दिया है, जो वस्तुतः जैन संस्कृतिके प्रतीक हैं।
उत्तरप्रदेशके विभिन्न स्थानोंमें प्राचीन मन्दिरोंके भग्नावशेष मीलोंमें बिखरे पड़े हैं, जिनमें कुछ टीलोंका उत्खनन हो गया है। अनेक टीलोंकी खुदाई अबतक भी नहीं हो पायी है।
ये स्थान हैं-देवगढ़, हस्तिनापुर, मथुरा, अहिच्छत्र, कम्पिला, चन्दवार, शौरीपुर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, अयोध्या, ककुभग्राम, काकन्दी, पारसनाथका किला आदि।
जैन कला उत्तरप्रदेशमें विभिन्न स्थानोंके अन्वेषण और उत्खनन द्वारा जो जैन कलाकृतियाँ उपलब्ध हुई हैं, उन्हें हम सुविधाके लिए चार भागोंमें विभक्त कर सकते हैं -
१. तीर्थकर मूर्तियाँ-देवगढ़, श्रावस्ती, प्रयाग, मथुरा, अहिच्छत्र, काकन्दी, कौशाम्बी, पभोसा और कम्पिलामें कुछ ऐसी मूर्तियाँ उपलब्ध हुई हैं, जिनका निर्माण काल ईसा पूर्व तीसरीचौथी शताब्दीसे ईसाकी ५-६वीं शताब्दीतक है । जितनी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, उनमें पद्मासन प्रतिमाएँ अधिक हैं। कुछ खड्गासन प्रतिमाएं भी हैं। देवगढ़में ऐसी प्रतिमाओंकी संख्या अधिक है। अधिकांश प्रतिमाओंके सिंहासन पीठपर उनका निर्माण-काल अभिलिखित है। कुछ प्राचीन प्रतिमाओंपर इस प्रकारके लेख अंकित नहीं हैं। जैन समाजमें ऐसी प्रतिमाओंको चतुर्थकाल अर्थात् ईसा पूर्व छठवीं या इससे पूर्वकी शताब्दियोंकी माननेका चलन है। ऐसी मूर्तियाँ बड़ागाँव, मथुरा, प्रयाग, चन्दवार, फिरोजाबाद, काकन्दी, ककुभग्राम, बहसूमा, देवगढ़ आदिमें हैं।
इतना तो प्रायः निश्चित है कि जिन प्रतिमाओंपर अभिलेख नहीं हैं, वे ईसा पूर्वसे लेकर गुप्तकाल अथवा उसके बादकी मानी गयी हैं। ऐसी प्रतिमाओंमेंसे कुछका परिचय पुरातत्त्वके छात्रों और शोधकर्ताओंके लिए बड़ा उपयोगी होगा।