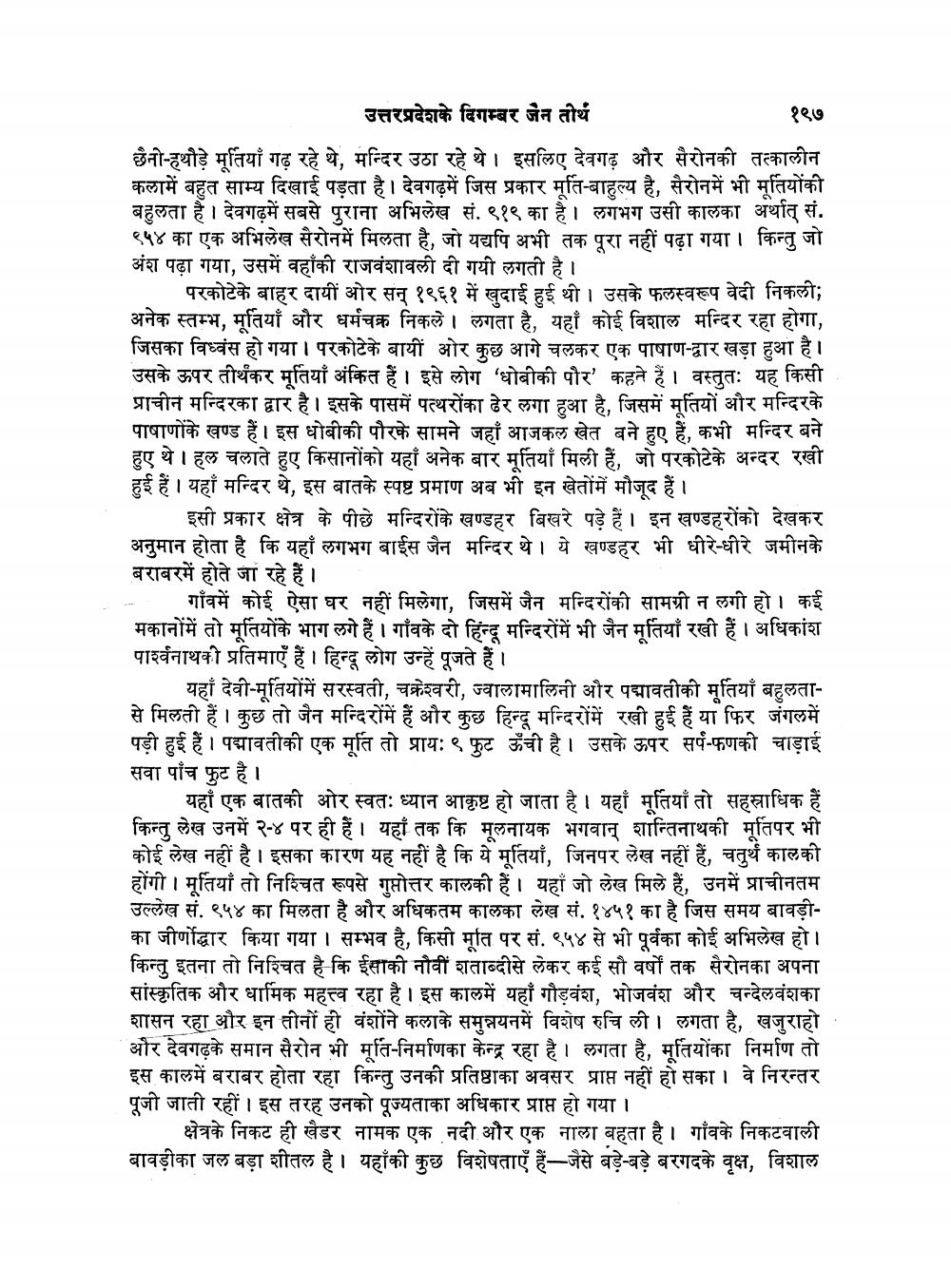________________
उत्तरप्रदेशके दिगम्बर जैन तीर्थ छैनो-हथौड़े मूर्तियाँ गढ़ रहे थे, मन्दिर उठा रहे थे। इसलिए देवगढ़ और सैरोनकी तत्कालीन कलामें बहुत साम्य दिखाई पड़ता है। देवगढ़में जिस प्रकार मूर्ति-बाहुल्य है, सैरोनमें भी मूर्तियोंकी बहुलता है। देवगढ़में सबसे पुराना अभिलेख सं. ९१९ का है। लगभग उसी कालका अर्थात् सं. ९५४ का एक अभिलेख सैरोनमें मिलता है, जो यद्यपि अभी तक पूरा नहीं पढ़ा गया। किन्तु जो अंश पढ़ा गया, उसमें वहाँकी राजवंशावली दी गयी लगती है।
परकोटेके बाहर दायीं ओर सन् १९६१ में खुदाई हुई थी। उसके फलस्वरूप वेदी निकली; अनेक स्तम्भ, मूर्तियाँ और धर्मचक्र निकले। लगता है, यहाँ कोई विशाल मन्दिर रहा होगा, जिसका विध्वंस हो गया। परकोटेके बायीं ओर कुछ आगे चलकर एक पाषाण-द्वार खड़ा हुआ है। उसके ऊपर तीर्थंकर मूर्तियाँ अंकित हैं। इसे लोग 'धोबीकी पौर' कहते हैं। वस्तुतः यह किसी प्राचीन मन्दिरका द्वार है। इसके पासमें पत्थरोंका ढेर लगा हुआ है, जिसमें मूर्तियों और मन्दिरके पाषाणोंके खण्ड हैं। इस धोबीकी पौरके सामने जहाँ आजकल खेत बने हुए हैं, कभी मन्दिर बने हुए थे। हल चलाते हुए किसानोंको यहाँ अनेक बार मूर्तियाँ मिली हैं, जो परकोटेके अन्दर रखी हुई हैं । यहाँ मन्दिर थे, इस बातके स्पष्ट प्रमाण अब भी इन खेतोंमें मौजूद हैं।
इसी प्रकार क्षेत्र के पीछे मन्दिरोंके खण्डहर बिखरे पड़े हैं। इन खण्डहरोंको देखकर अनुमान होता है कि यहाँ लगभग बाईस जैन मन्दिर थे। ये खण्डहर भी धीरे-धीरे जमीनके बराबरमें होते जा रहे हैं।
गाँवमें कोई ऐसा घर नहीं मिलेगा, जिसमें जैन मन्दिरोंकी सामग्री न लगी हो। कई मकानोंमें तो मूर्तियोंके भाग लगे हैं । गाँवके दो हिन्दू मन्दिरोंमें भी जैन मूर्तियाँ रखी हैं । अधिकांश पार्श्वनाथकी प्रतिमाएँ हैं । हिन्दू लोग उन्हें पूजते हैं।
यहाँ देवी-मूर्तियोंमें सरस्वती, चक्रेश्वरी, ज्वालामालिनी और पद्मावतीकी मूर्तियाँ बहुलतासे मिलती हैं । कुछ तो जैन मन्दिरोंमें हैं और कुछ हिन्दू मन्दिरोंमें रखी हुई हैं या फिर जंगल में पड़ी हुई हैं । पद्मावतीकी एक मूर्ति तो प्रायः ९ फुट ऊँची है। उसके ऊपर सर्प-फणकी चाड़ाई सवा पाँच फुट है।
यहाँ एक बातकी ओर स्वतः ध्यान आकृष्ट हो जाता है। यहाँ मूर्तियाँ तो सहस्राधिक हैं किन्तु लेख उनमें २-४ पर ही हैं। यहाँ तक कि मूलनायक भगवान् शान्तिनाथकी मूर्तिपर भी कोई लेख नहीं है। इसका कारण यह नहीं है कि ये मूर्तियाँ, जिनपर लेख नहीं हैं, चतुर्थ कालकी होंगी। मूर्तियाँ तो निश्चित रूपसे गुप्तोत्तर कालकी हैं। यहाँ जो लेख मिले हैं, उनमें प्राचीनतम उल्लेख सं. ९५४ का मिलता है और अधिकतम कालका लेख सं. १४५१ का है जिस समय बावड़ीका जीर्णोद्धार किया गया। सम्भव है, किसी मूति पर सं. ९५४ से भी पूर्वका कोई अभिलेख हो। किन्तु इतना तो निश्चित है कि ईसाकी नौवीं शताब्दीसे लेकर कई सौ वर्षों तक सैरोनका अपना सांस्कृतिक और धार्मिक महत्त्व रहा है। इस कालमें यहाँ गौड़वंश, भोजवंश और चन्देलवंशका शासन रहा और इन तीनों ही वंशोंने कलाके समुन्नयनमें विशेष रुचि ली। लगता है, खजुराहो और देवगढ़के समान सैरोन भी मूर्ति-निर्माणका केन्द्र रहा है। लगता है, मूर्तियोंका निर्माण तो इस कालमें बराबर होता रहा किन्तु उनकी प्रतिष्ठाका अवसर प्राप्त नहीं हो सका। वे निरन्तर पूजी जाती रहीं। इस तरह उनको पूज्यताका अधिकार प्राप्त हो गया।
क्षेत्रके निकट ही खैडर नामक एक नदी और एक नाला बहता है। गाँवके निकटवाली बावड़ीका जल बड़ा शीतल है। यहाँको कुछ विशेषताएँ हैं-जैसे बड़े-बड़े बरगदके वृक्ष, विशाल