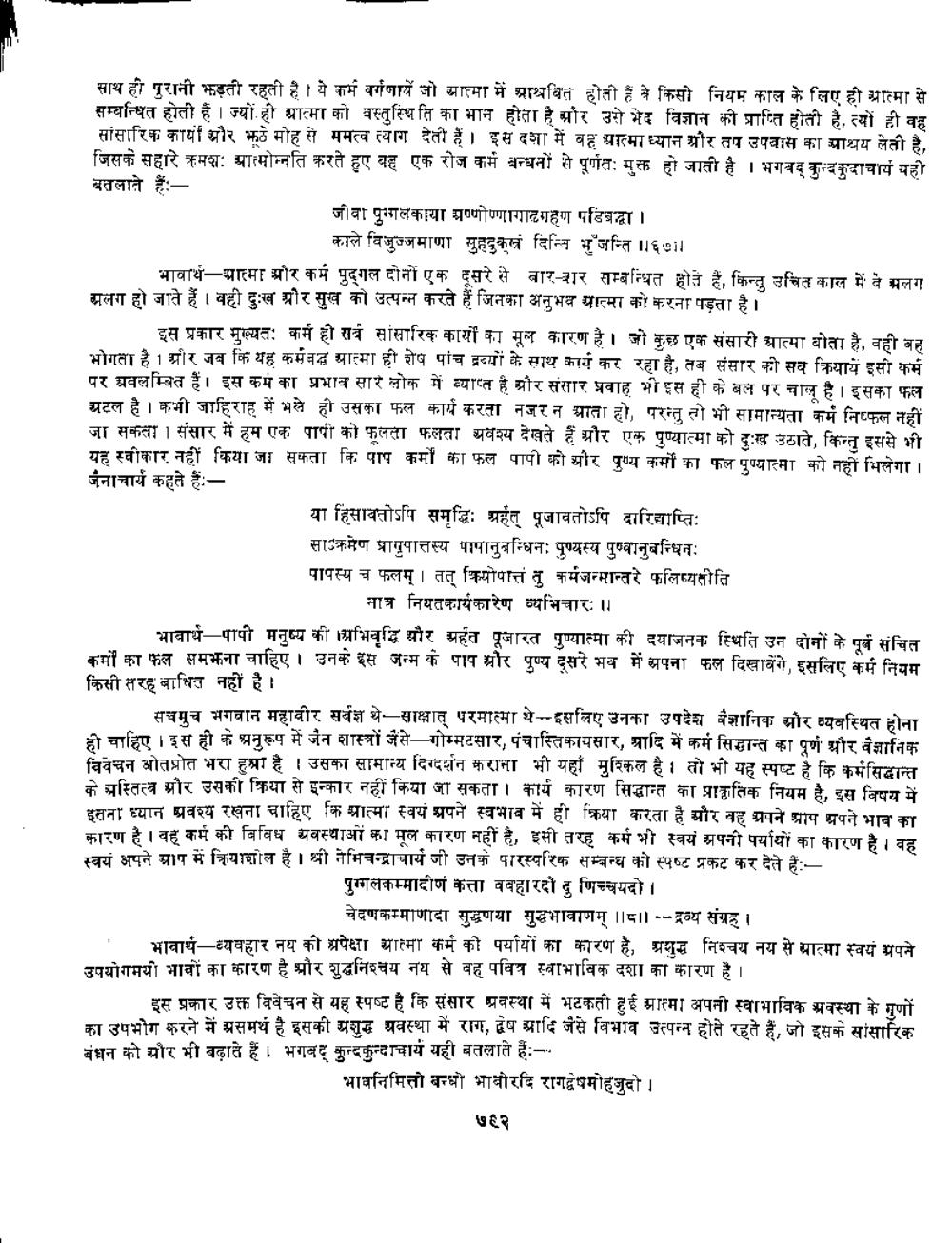________________
साथ ही पुरानी झड़ती रहती है। ये कर्म वर्गणायें जो आत्मा में प्राश्रवित होती हैं वे किसो नियम काल के लिए ही आत्मा से सम्बन्धित होती है । ज्यों ही प्रात्मा को वस्तुस्थिति का भान होता है और उसे भेद विज्ञान की प्राप्ति होती है, त्यों ही वह सांसारिक कार्यों और झठे मोह से ममत्व त्याग देती हैं। इस दशा में बहात्मा ध्यान और तप उपवास का पाश्चय लेती है, जिसके सहारे क्रमश: आत्मोन्नति करते हुए बह एक रोज कर्म बन्धनों से पूर्णत: मुक्त हो जाती है । भगवद् कुन्दकुदाचार्य यही बतलाते हैं:
जीवा पुमालकाया अण्णोण्णागाढ ग्रहण पडिबद्धा।
काले विजुज्जमाणा सुदुक्खं दिन्ति भुजन्ति ।।६७।। भावार्थ-आत्मा और कर्म पुद्गल दोनों एक दूसरे से बार-बार सम्बन्धित होते हैं, किन्तु उचित काल में वे अलग अलग हो जाते हैं । वही दुःख और सुख को उत्पन्न करते हैं जिनका अनुभव प्रात्मा को करना पड़ता है।
इस प्रकार मुख्यत: कर्म ही सर्व सांसारिक कार्यों का मूल कारण है। जो कुछ एक संसारी आत्मा बोता है, वही वह भोगता है। श्रीर जब कि यह कर्मबद्ध आत्मा ही शेष पांच द्रव्यों के साथ कार्य कर रहा है, तब संसार की सब क्रियायें इसी कर्म पर अवलम्बित हैं। इस कम का प्रभाव सारे लोक में व्याप्त है और संसार प्रवाह भी इस ही के बल पर चालू है। इसका फल अटल है। कभी जाहिराह में भले ही उसका फल कार्य करता नजर न आता हो, परन्तु तो भी सामान्यता कम निष्फल नहीं जा सकता । संसार में हम एक पापी को फलता फलता अवश्य देखते हैं और एक पुण्यात्मा को दुःख उठाते, किन्तु इससे भी यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि पाप कर्मों का फल पापी को और पुण्य कर्मों का फल पुण्यात्मा को नहीं मिलेगा। जैनाचार्य कहते हैं:
या हिंसावतोऽपि समृद्धिः अर्हत् पूजावतोऽपि दारिद्याप्तिः साक्रमेण प्रागपात्तस्य पापानुबन्धिनः पुण्यस्य पुण्वानुबन्धिन पापस्य च फलम् । तत् क्रियोपात्तं तु कर्मजन्मान्तरे फलिण्यतीति
नात्र नियतकार्यकारेण व्यभिचारः ।। भावार्थ-पापी मनुष्य की अभिवृद्धि और अहंत पूजारत पुण्यात्मा की दयाजनक स्थिति उन दोनों के पूर्व संचित कमाँ का फल समझना चाहिए। उनके इस जन्म के पाप और पुण्य दूसरे भव में अपना फल दिखावेगे, इसलिए कर्म नियम किसी तरह बाधित नहीं है।
सचमुच भगवान महावीर सर्वज्ञ थे-साक्षात् परमात्मा थे इसलिए उनका उपदेश वैज्ञानिक और व्यवस्थित होना ही चाहिए। इस ही के अनुरूप में जैन शास्त्रों जैसे-गोम्मटसार, पंचास्तिकायसार, प्रादि में कर्म सिद्धान्त का पूर्ण और वैज्ञानिक विवेचन ओतप्रोत भरा हमा है । उसका सामान्य दिग्दर्शन कराना भी यहाँ मुश्किल है। तो भी यह स्पष्ट है कि कर्मसिद्धान्त के अस्तित्व और उसकी क्रिया से इन्कार नहीं किया जा सकता। कार्य कारण सिद्धान्त का प्राकृतिक नियम है, इस विषय में अपना ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि आत्मा स्वयं अपने स्वभाव में ही क्रिया करता है और वह अपने पाप अपने भाव का
बह कर्म की बिबिध अवस्थाओं का मूल कारण नहीं है, इसी तरह कर्म भी स्वयं अपनी पर्यायों का कारण है। वह व अपने ग्राप में क्रियाशील है। श्री नेमिचन्द्राचार्य जी उनके पारस्परिक सम्बन्ध को स्पष्ट प्रकट कर देते हैं:
पुग्गलकम्मादीणं कत्ता वबहारदो दु णिच्चयदो।
चेदणकम्माणादा सुद्धणया सुद्धभावाणम् ।।८।। ---द्रव्य संग्रह । । भावार्थ-व्यवहार नय की अपेक्षा मात्मा कर्म को पर्यायों का कारण है, अशुद्ध निश्चय नय से प्रात्मा स्वयं अपने उपयोगमयी भावों का कारण है और शुद्धनिश्चय नय से बह पवित्र स्वाभाविक दशा का कारण है।
इस प्रकार उक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि संसार अवस्था में भटकती हुई प्रात्मा अपनी स्वाभाविक अवस्था के गुणों का उपभोग करने में असमर्थ है इसकी अशुद्ध अवस्था में राग, द्वेष आदि जैसे विभाव उत्पन्न होते रहते हैं, जो इसके सांसारिक बंधन को और भी बढ़ाते हैं। भगवद कुन्दकुन्दाचार्य यही बतलाते हैं:
भावनिमित्तो बन्धो भावोरदि रागद्वेषमोहजुदो ।
७६२