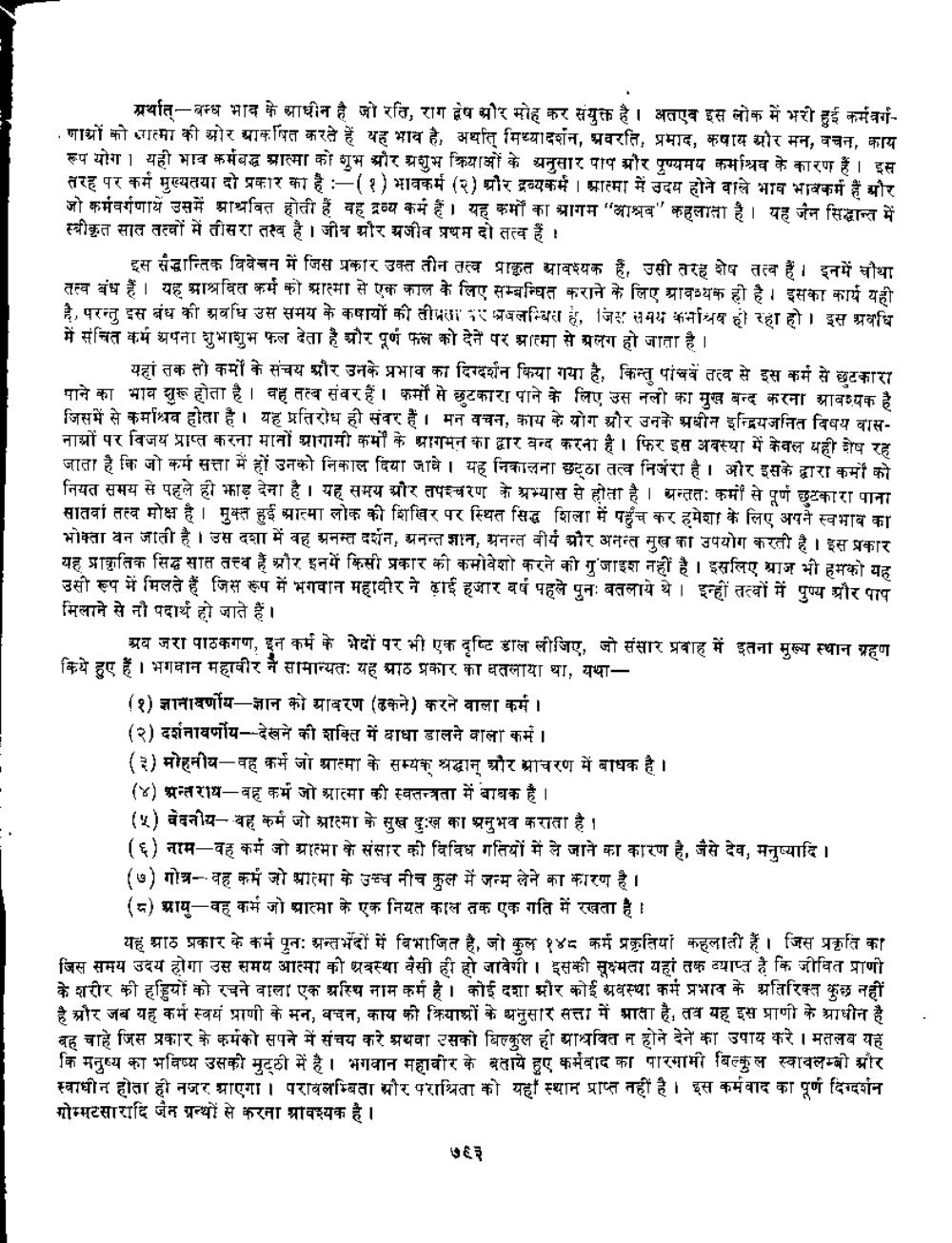________________
अर्थात्-बन्ध भाद के आधीन है जो रति, राग द्वेष और मोह कर संयुक्त है। अतएव इस लोक में भरी हुई कर्मवर्ग.णाओं को आत्मा की ओर याकर्षित करते हैं यह भाव है, अर्थात् मिथ्यादर्शन, प्रवरति, प्रमाद, कषाय मौर मन, वचन, काय रूप योग । यही भाव कर्मबद्ध प्रात्मा को शुभ और अशुभ क्रियाओं के अनुसार पाप और पुण्यमय कश्रिव के कारण हैं। इस तरह पर कर्म मुख्यतया दो प्रकार का है :-(१) भावकर्म (२) और द्रव्यकर्म । प्रात्मा में उदय होने वाले भाव भावकर्म हैं और जो कर्मवर्गणायें उसमें प्रावित होती हैं वह द्रव्य कर्म हैं। यह कर्मों का आगम "आश्रब" कहलाता है। यह जैन सिद्धान्त में स्वीकृत सात तत्वों में तीसरा तस्व है। जीव और अजीव प्रथम दो तत्व हैं।
इस संद्धान्तिक विवेचन में जिस प्रकार उक्त तीन तत्व प्राकृत यावश्यक हैं, उसी तरह शेष तत्व हैं। इनमें चौथा तत्व बंध हैं। यह पाश्रवित कर्म को प्रात्मा से एक काल के लिए सम्बन्धित कराने के लिए आवश्यक ही है। इसका कार्य यही है, परन्तु इस बंध की अवधि उस समय के कषायों की तीव्रता र अवलम्बित है, जिस समय कश्रिवा ही रहा हो। इस अवधि में संचित कर्म अपना शुभाशुभ फल देता है और पूर्ण फल को देने पर प्रात्मा से अलग हो जाता है।
यहां तक तो कर्मों के संचय और उनके प्रभाव का दिग्दर्शन किया गया है, किन्तु पांच तत्व से इस कर्म से छुटकारा पाने का भाव शुरू होता है। वह तत्व संवर हैं। कर्मों से छुटकारा पाने के लिए उस नली का मुख बन्द करना आवश्यक है जिसमें से कर्माधव होता है। यह प्रतिरोध ही संवर है। मन वचन, काय के योग और उनके अधीन इन्द्रियजनित विषय वासनारों पर विजय प्राप्त करना मानों प्रागामी कर्मों के प्रागमन का द्वार बन्द करना है। फिर इस अवस्था में केवल यही शेष रह जाता है कि जो कर्म सत्ता में हों उनको निकाल दिया जावे। यह निकालना छठा तत्व निर्जरा है। और इसके द्वारा कर्मों को नियत समय से पहले ही झाड़ देना है। यह समय और तपश्चरण के अभ्यास से होता है। अन्ततः कमी से पूर्ण छुटकारा पाना सातवां तत्व मोक्ष है। मुक्त हुई पात्मा लोक की शिखिर पर स्थित सिद्ध शिला में पहुंच कर हमेशा के लिए अपने स्वभाव का भोक्ता बन जाती है । उस दशा में वह अनन्त दर्शन, अनन्त शान, अनन्त वीर्य और अनन्त मुख का उपयोग करती है। इस प्रकार यह प्राकृतिक सिद्ध सात तत्व है और इनमें किसी प्रकार की कमोवेशो करने की गुजाइश नहीं है। इसलिए आज भी हमको यह उसी रूप में मिलते हैं जिस रूप में भगवान महावीर ने ढाई हजार वर्ष पहले पुनः बतलाये थे। इन्हीं तत्वों में पुण्य और पाप मिलाने से नौ पदार्थ हो जाते हैं।
अब जरा पाठकगण, इन कर्म के भेदों पर भी एक दृष्टि डाल लीजिए, जो संसार प्रवाह में इतना मुख्य स्थान ग्रहण किये हुए हैं। भगवान महावीर ने सामान्यतः यह पाठ प्रकार का बतलाया था, यथा
(१) ज्ञानावर्णीय-ज्ञान को पावरण (ढकने) करने वाला कर्म । (२) दर्शनावर्णीय-देखने की शक्ति में बाधा डालने वाला कर्म । (३) मोहनीय-वह कर्म जो प्रात्मा के सम्यक् श्रद्धान् और पाचरण में बाधक है। (४) अन्तराय-बह कर्म जो आत्मा की स्वतन्त्रता में बाधक है। (५) वेदनीय- बह कर्म जो प्रात्मा के सुख दुःख का अनुभव कराता है। (६) नाम-वह कर्म जो प्रात्मा के संसार की विविध गतियों में ले जाने का कारण है, जैसे देव, मनुष्यादि । (७) गोत्र-- वह कर्म जो प्रात्मा के उच्च नीच कूल में जन्म लेने का कारण है। (८) मायु-वह कर्म जो पात्मा के एक नियत काल तक एक गति में रखता है।
यह पाठ प्रकार के कर्म पुन: अन्तभेदों में विभाजित है, जो कुल १४८ कर्म प्रकृतियों कहलाती हैं। जिस प्रकृति का जिस समय उदय होगा उस समय आत्मा की अवस्था वैसी ही हो जावेगी। इसकी सूक्ष्मता यहां तक व्याप्त है कि जीवित प्राणी के शरीर की हड्डियों को रचने वाला एक अस्थि नाम कर्म है। कोई दशा मौर कोई अवस्था कर्म प्रभाव के अतिरिक्त कुछ नहीं है और जब यह कर्म स्वयं प्राणी के मन, वचन, काय की क्रियानों के अनुसार सत्ता में आता है, तब यह इस प्राणी के आधीन है वह चाहे जिस प्रकार के कर्मको सपने में संचय करे अथवा रसको बिल्कुल ही यायवित न होने देने का उपाय करे । मतलब यह कि मनुष्य का भविष्य उसकी मुट्ठी में है। भगवान महावीर के बताये हुए कर्मवाद का पारगामी बिल्कुल स्वावलम्बी और स्वाधीन होता ही नजर पाएगा। परावलम्बिता और पराश्रिता को यहाँ स्थान प्राप्त नहीं है। इस कर्मवाद का पूर्ण दिग्दर्शन गोम्मटसारादि जैन ग्रन्थों से करना आवश्यक है।