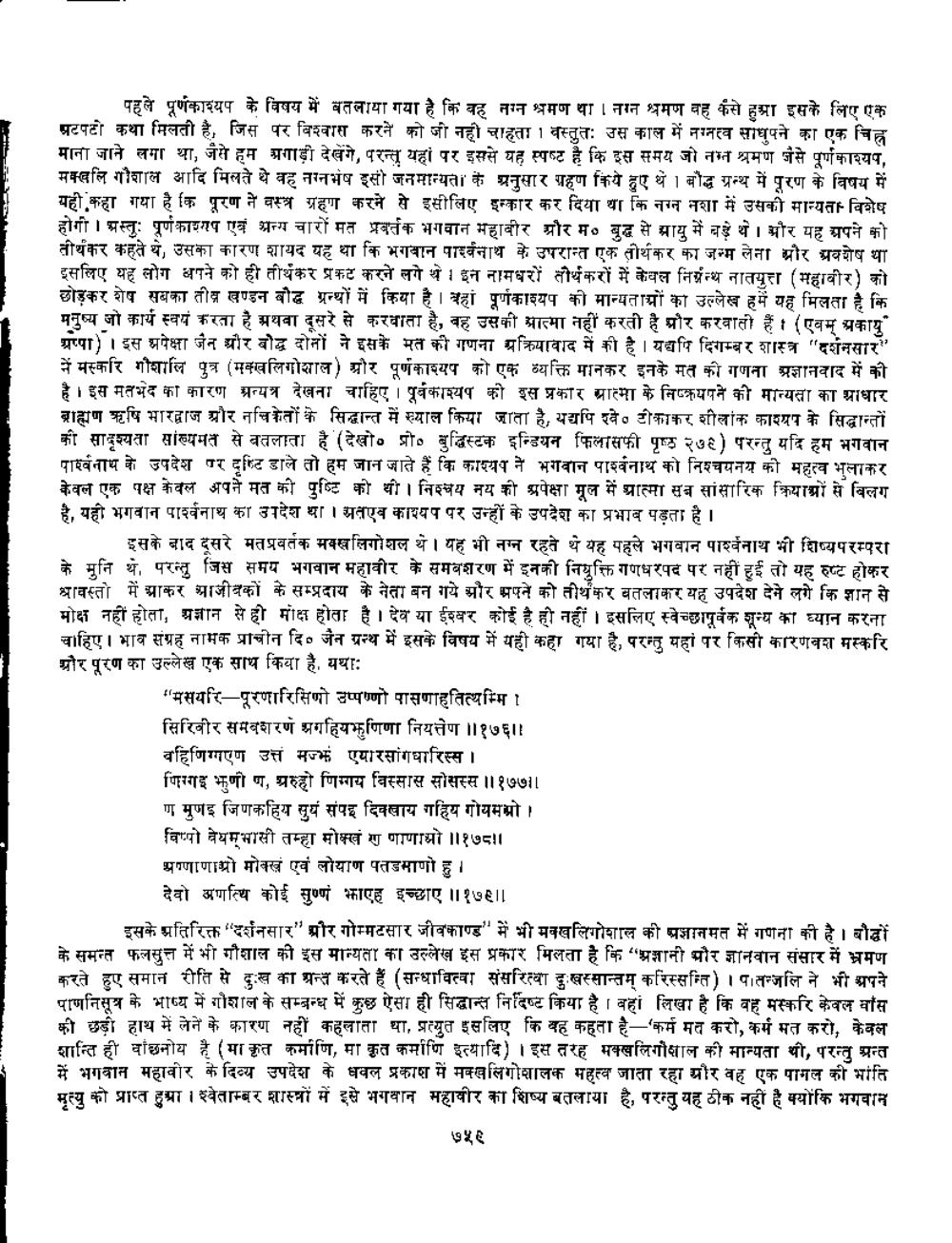________________
1
पहले पूर्णकाश्यप के विषय में बतलाया गया है कि वह नग्न श्रमण था । नग्न श्रमण वह कैसे हुआ इसके लिए एक घटपट कथा मिलती है, जिस पर विश्वास करने को जी नही चाहता वस्तुतः उस काल में ममत्व साधुपने का एक मिल माना जाने लगा था, जैसे हम बगाड़ी देखेंगे, परन्तु यहां पर इससे यह स्पष्ट है कि इस समय जो न श्रमण जैसे पूर्णकाश्यप, नक्सल गौपाल आदि मिलते थे वह नग्नमेष इसी जनमान्यता के अनुसार ग्रहण किये हुए थे। बौद्ध ग्रन्थ में पूरण के विषय में यही कहा गया है कि पुरण ने वस्त्र ग्रहण करने से इसीलिए इन्कार कर दिया था कि नग्न नशा में उसकी मान्यता विशेष होगी । अस्तुः पूर्णकाप एवं अन्य चारों मत प्रवर्तक भगवान महावीर और म० बुद्ध से प्रायु में बड़े थे। और यह अपने को तीर्थकर कहते थे, उसका कारण शायद यह था कि भगवान पार्श्वनाथ के उपरान्त एक तीर्थंकर का जन्म लेना और अवशेष पा इसलिए यह लोग अपने को ही तीर्थंकर प्रकट करने लगे थे। इन नामधरों तीर्थकरों में केवल निर्ब्रन्थ नातयुक्त ( महावीर ) को छोड़कर शेष सबका तीव्र खण्डन बौद्ध ग्रन्थों में किया है। वहां पूर्णकाश्यप की मान्यताओं का उल्लेख हमें यह मिलता है कि मनुष्य जो कार्य स्वयं करता है अथवा दूसरे से करवाता है, वह उसकी आत्मा नहीं करती है और करवाती हैं। (एवम् प्रकायु थप्पा)। इस अपेक्षा जैन बीर बौद्ध दोनों ने इसके मत की गणना क्रियावाद में की है। यद्यपि दिगम्बर शास्त्र " दर्शनसार" में मस्करि गौवादि पुत्र ( मखलिगोशाल) पीर पूर्णकास्यप को एक व्यक्ति मानकर इनके गत की गणना अज्ञानवाद में की है। इस मतभेद का कारण प्रत्यत्र देखना चाहिए। पूर्वकाश्यप की इस प्रकार मात्मा के निष्क्रयपने की मान्यता का साधार ब्राह्मण ऋषि भारद्वाज और नचिकेतों के सिद्धान्त में ख्याल किया जाता है, यद्यपि वे टीकाकर शीलांक काश्यप के सिद्धान्तों की सावृश्यता सांख्यमत से बतलाता है (देखो० प्रो० बुद्धिस्टक इन्डियन फिलासफी पृष्ठ २७९) परन्तु यदि हम भगवान पार्श्वनाथ के उपदेश पर दृष्टि डाले तो हम जान जाते हैं कि काश्वव ने भगवान पार्श्वनाथ को निश्चय की महत्व भुलाकर केवल एक पक्ष केवल अपने मत की पुष्टि की थी । निश्चय नय की अपेक्षा मूल में ग्रात्मा सब सांसारिक क्रियाओं से बिलग है, यही भगवान पार्श्वनाथ का उपदेश था। अतएव काश्यप पर उन्हों के उपदेश का प्रभाव पड़ता है।
०
इसके बाद दूसरे मतप्रवर्तक मक्खलिगोशल थे। यह भी नग्न रहते थे यह पहले भगवान पार्श्वनाथ भी शिष्यपरम्परा के मुनि थे परन्तु जिस समय भगवान महावीर के समवशरण में इनकी नियुक्ति गणधरपद पर नहीं हुई तो यह रूष्ट होकर श्रावस्ती में ग्राकर धाजीवकों के सम्प्रदाय के नेता बन गये और अपने को तीर्थकर बतलाकर यह उपदेश देने लगे कि ज्ञान से मोक्ष नहीं होता, समान से ही मोक्ष होता है। देव या ईश्वर कोई है ही नहीं इसलिए स्वेच्छापूर्वक शून्य का ध्यान करना चाहिए। भाव संग्रह नामक प्राचीन दि० जैन ग्रन्थ में इसके विषय में यही कहा गया है, परन्तु यहां पर किसी कारणवश मस्करि और पूरण का उल्लेख एक साथ किया है. यथा:
"मसर- पूरणारिसियो उप्पण्णोपासणाहुतित्यम्म
सिरिवीर समवशरणं अमहियभुणिना नियतेण ॥ १७६ ।।
वहिणिग्गएण उत्त मज्भं एयारसांगधारिस्स ।
गिग्ग भूणी व मरुहो निमाय विरसास सोसरस ।। १७७।।
मुणइ जिणकहिय सुर्य संपद्म दिवखाय गहिय गोयमम्रो ।
विप्पो वेभासी तम्हा मोष णानाओ || १७८॥
可
अण्णाणाओ मोक्तं एवं लोयाण पतडमाणो हु ।
देवो अगत्य कोई सुगं काह इच्छाए ।। १७९।।
इसके अतिरिक्त दर्शनसार" और गोम्मटसार जीवकाण्ड" में भी मसलिगोपाल की अज्ञानमत में गणना की है। बीढों के समन्त फलत में भी गौशाल की इस मान्यता का उल्लेख इस प्रकार मिलता है कि "अज्ञानी और ज्ञानवान संसार में भ्रमण करते हुए समान रीति से दुःख का अन्त करते हैं (सन्धावित्वा संसारित्वा दुःखस्सान्तम् करिस्सन्ति ) । पतन्जलि ने भी अपने पाणनिसूत्र के भाग्य में गोशाल के सम्बन्ध में कुछ ऐसा ही सिद्धान्त निर्दिष्ट किया है। वहां लिखा है कि वह मस्करि केवल वांस की छड़ी हाथ में लेने के कारण नहीं कहलाता था, प्रत्युत इसलिए कि वह कहता है- 'कर्म मत करो, कर्म मत करो, केवल शान्ति ही वांछनीय है ( माकृत कर्माणि मा कृत कर्माणि इत्यादि)। इस तरह खनियाल की मान्यता थी, परन्तु मन्त में भगवान महावीर के दिव्य उपदेश के धवल प्रकाश में मक्ख लिगोशालक महत्व जाता रहा और वह एक पागल की भांति मृत्यु को प्राप्त हुआ । श्वेताम्बर शास्त्रों में इसे भगवान महावीर का शिष्य बतलाया है, परन्तु यह ठीक नहीं है क्योंकि भगवान
७५६