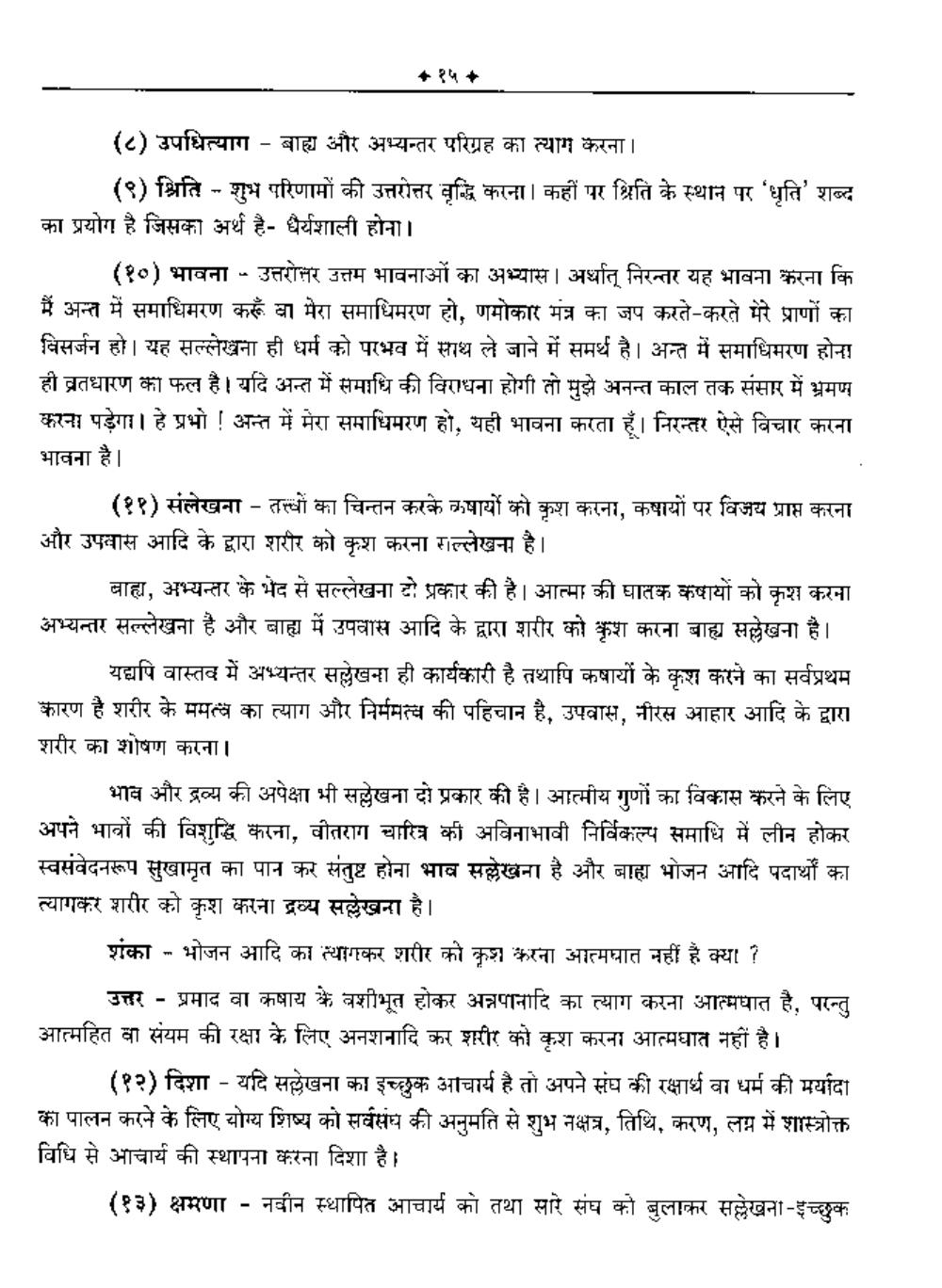________________
(८) उपधित्याग - बाह्य और अभ्यन्तर परिग्रह का त्याग करना।
(९) श्रिति - शुभ परिणामों की उत्तरोत्तर वृद्धि करना । कहीं पर श्रिति के स्थान पर 'धृति' शब्द का प्रयोग है जिसका अर्थ है- धैर्यशाली होना।
(१०) भावना - उत्तरोत्तर उत्तम भावनाओं का अभ्यास । अर्थात् निरन्तर यह भावना करना कि मैं अन्त में समाधिमरण करूँ वा मेरा समाधिमरण हो, णमोकार मंत्र का जप करते-करते मेरे प्राणों का विसर्जन हो। यह सल्लेखना ही धर्म को परभव में साथ ले जाने में समर्थ है। अन्त में समाधिमरण होना ही व्रतधारण का फल है। यदि अन्त में समाधि की विराधना होगी तो मुझे अनन्त काल तक संसार में भ्रमण करना पड़ेगा। हे प्रभो ! अन्त में मेरा समाधिमरण हो, यही भावना करता हूँ। निरन्तर ऐसे विचार करना भावना है।
(११) संलेखना - तत्त्वों का चिन्तन करके कषायों को कृश करना, कषायों पर विजय प्राप्त करना और उपवास आदि के द्वारा शरीर को कृश करना सल्लेखना है।
बाह्य, अभ्यन्तर के भेद से सल्लेखना दो प्रकार की है। आत्मा की घातक कषायों को कृश करना अभ्यन्तर सल्लेखना है और बाह्य में उपवास आदि के द्वारा शरीर को कृश करना बाह्य सल्लेखना है।
यद्यपि वास्तव में अभ्यन्तर सल्लेखना ही कार्यकारी है तथापि कषायों के कृश करने का सर्वप्रथम कारण है शरीर के ममत्व का त्याग और निर्ममत्व की पहिचान है, उपवास, नीरस आहार आदि के द्वारा शरीर का शोषण करना।
__ भाव और द्रव्य की अपेक्षा भी सल्लेखना दो प्रकार की है। आत्मीय गुणों का विकास करने के लिए अपने भावों की विशुद्धि करना, वीतराग चारित्र की अविनाभावी निर्विकल्प समाधि में लीन होकर स्वसंवेदनरूप सुखामृत का पान कर संतुष्ट होना भाव सल्लेखना है और बाह्य भोजन आदि पदार्थों का त्यागकर शरीर को कृश करना द्रव्य सल्लेखना है।
शंका - भोजन आदि का त्यागकर शरीर को कृश करना आत्मघात नहीं है क्या ?
उत्तर - प्रमाद वा कषाय के वशीभूत होकर अन्नपानादि का त्याग करना आत्मघात है, परन्तु आत्महित वा संयम की रक्षा के लिए अनशनादि कर शरीर को कृश करना आत्मघात नहीं है।
(१२) दिशा - यदि सल्लेखना का इच्छुक आचार्य है तो अपने संघ की रक्षार्थ वा धर्म की मर्यादा का पालन करने के लिए योग्य शिष्य को सर्वसंघ की अनुमति से शुभ नक्षत्र, तिथि, करण, लग्न में शास्त्रोक्त विधि से आचार्य की स्थापना करना दिशा है।
(१३) क्षमणा - नवीन स्थापित आचार्य को तथा सारे संघ को बुलाकर सल्लेखना-इच्छुक