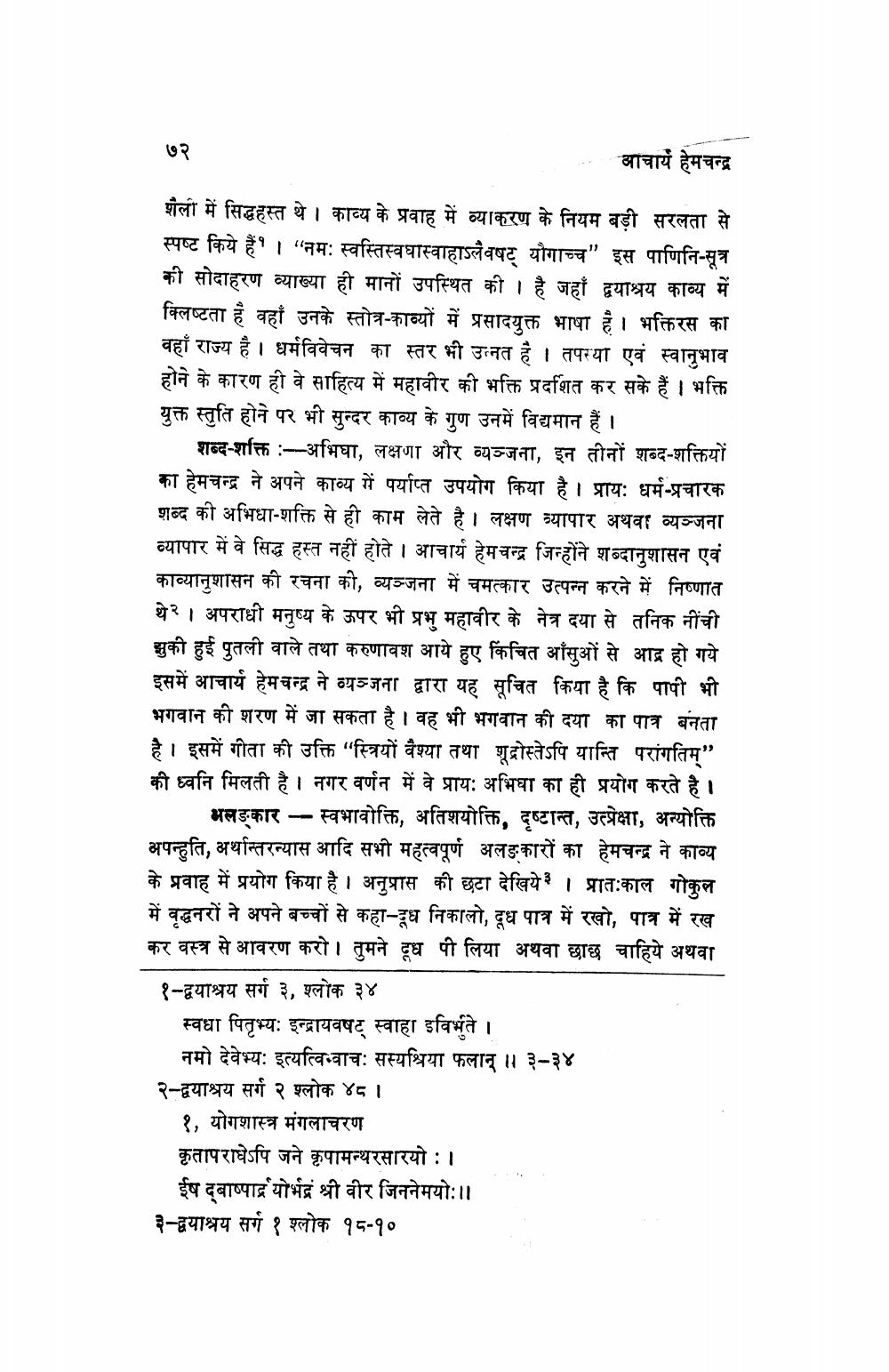________________
७२
... आचार्य हेमचन्द्र
शैली में सिद्धहस्त थे। काव्य के प्रवाह में व्याकरण के नियम बड़ी सरलता से स्पष्ट किये हैं । "नमः स्वस्तिस्वघास्वाहाऽलैवषट् यौगाच्च" इस पाणिनि-सूत्र की सोदाहरण व्याख्या ही मानों उपस्थित की । है जहाँ द्वयाश्रय काव्य में क्लिष्टता है वहाँ उनके स्तोत्र-काव्यों में प्रसादयुक्त भाषा है। भक्तिरस का वहाँ राज्य है। धर्मविवेचन का स्तर भी उन्नत है । तपस्या एवं स्वानुभाव होने के कारण ही वे साहित्य में महावीर की भक्ति प्रदर्शित कर सके हैं । भक्ति युक्त स्तुति होने पर भी सुन्दर काव्य के गुण उनमें विद्यमान हैं।
शब्द-शक्ति :-अभिघा, लक्षणा और व्यञ्जना, इन तीनों शब्द-शक्तियों का हेमचन्द्र ने अपने काव्य में पर्याप्त उपयोग किया है। प्रायः धर्म-प्रचारक शब्द की अभिधा-शक्ति से ही काम लेते है। लक्षण व्यापार अथवा व्यञ्जना व्यापार में वे सिद्ध हस्त नहीं होते । आचार्य हेमचन्द्र जिन्होंने शब्दानुशासन एवं काव्यानुशासन की रचना की, व्यञ्जना में चमत्कार उत्पन्न करने में निष्णात थे । अपराधी मनुष्य के ऊपर भी प्रभु महावीर के नेत्र दया से तनिक नींची झुकी हुई पुतली वाले तथा करुणावश आये हुए किंचित आँसुओं से आद्र हो गये इसमें आचार्य हेमचन्द्र ने व्यञ्जना द्वारा यह सूचित किया है कि पापी भी भगवान की शरण में जा सकता है । वह भी भगवान की दया का पात्र बनता है। इसमें गीता की उक्ति "स्त्रियों वैश्या तथा शूद्रोस्तेऽपि यान्ति परांगतिम्" की ध्वनि मिलती है। नगर वर्णन में वे प्रायः अभिघा का ही प्रयोग करते है।
भलङ्कार - स्वभावोक्ति, अतिशयोक्ति, दृष्टान्त, उत्प्रेक्षा, अन्योक्ति अपन्हुति, अर्थान्तरन्यास आदि सभी महत्वपूर्ण अलङकारों का हेमचन्द्र ने काव्य के प्रवाह में प्रयोग किया है । अनुप्रास की छटा देखिये । प्रातःकाल गोकुल में वृद्धनरों ने अपने बच्चों से कहा-दूध निकालो, दूध पात्र में रखो, पात्र में रख कर वस्त्र से आवरण करो। तुमने दूध पी लिया अथवा छाछ चाहिये अथवा १-द्वयाश्रय सर्ग ३, श्लोक ३४ स्वधा पितृभ्यः इन्द्रायवषट् स्वाहा इविर्भुते ।
नमो देवेभ्यः इत्यत्वि-वाचः सस्यश्रिया फलान् ।। ३-३४ २-द्वयाश्रय सर्ग २ श्लोक ४८ ।
१, योगशास्त्र मंगलाचरण कृतापराधेऽपि जने कृपामन्थरसारयो :।
ईष द्बाष्पा योभद्रं श्री वीर जिननेमयोः।। ३-द्वयाश्रय सर्ग १ श्लोक १८-१०