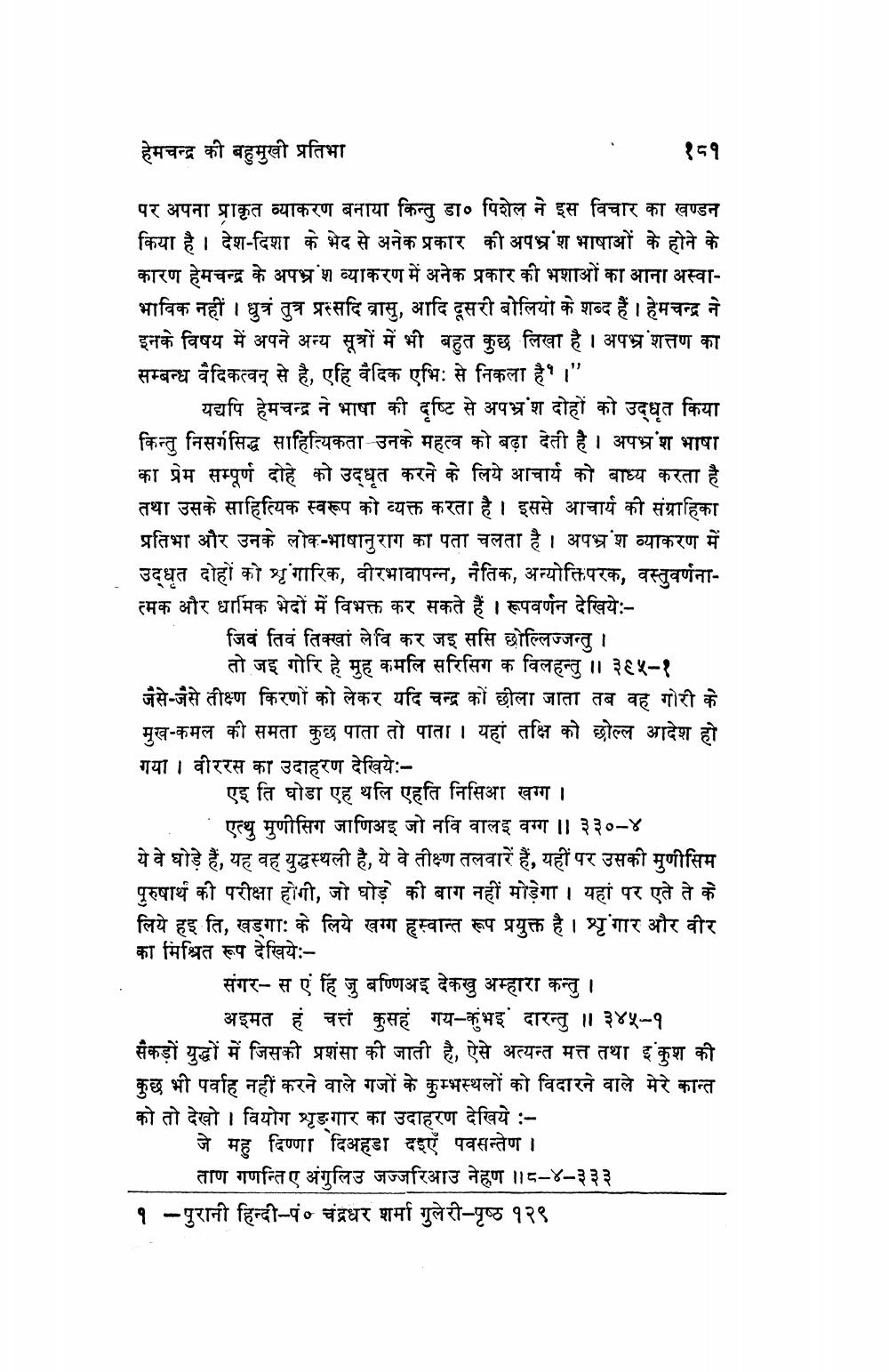________________
हेमचन्द्र की बहुमुखी प्रतिभा
पर अपना प्राकृत व्याकरण बनाया किन्तु डा० पिशेल ने इस विचार का खण्डन किया है। देश-दिशा के भेद से अनेक प्रकार की अपभ्रंश भाषाओं के होने के कारण हेमचन्द्र के अपभ्रश व्याकरण में अनेक प्रकार की भशाओं का आना अस्वाभाविक नहीं । धुत्रं तुत्र प्रत्सदि वासु, आदि दूसरी बोलियो के शब्द हैं । हेमचन्द्र ने इनके विषय में अपने अन्य सूत्रों में भी बहुत कुछ लिखा है । अपभ्रंशत्तण का सम्बन्ध वैदिकत्वन् से है, एहि वैदिक एभिः से निकला है।"
यद्यपि हेमचन्द्र ने भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश दोहों को उद्धृत किया किन्तु निसर्गसिद्ध साहित्यिकता उनके महत्व को बढ़ा देती है। अपभ्रंश भाषा का प्रेम सम्पूर्ण दोहे को उद्धृत करने के लिये आचार्य को बाध्य करता है तथा उसके साहित्यिक स्वरूप को व्यक्त करता है। इससे आचार्य की संग्राहिका प्रतिभा और उनके लोक-भाषानुराग का पता चलता है। अपभ्रंश व्याकरण में उद्धृत दोहों को शृंगारिक, वीरभावापन्न, नैतिक, अन्योक्तिपरक, वस्तुवर्णनात्मक और धार्मिक भेदों में विभक्त कर सकते हैं । रूपवर्णन देखिये:
जिवं तिवं तिक्खां लेवि कर जइ ससि छोल्लिज्जन्तु ।
तो जइ गोरि हे मुह कमलि सरिसिग क विलहन्तु ।। ३६५-१ जैसे-जैसे तीक्ष्ण किरणों को लेकर यदि चन्द्र को छीला जाता तब वह गोरी के मुख-कमल की समता कुछ पाता तो पाता। यहां तक्षि को छोल्ल आदेश हो गया। वीररस का उदाहरण देखिये:
एइ ति घोडा एह थलि एहति निसिआ खग्ग ।
- एत्थु मुणीसिग जाणिअइ जो नवि वालइ वग्ग ।। ३३०-४ ये वे घोड़े हैं, यह वह युद्धस्थली है, ये वे तीक्ष्ण तलवारें हैं, यहीं पर उसकी मुणीसिम पुरुषार्थ की परीक्षा होगी, जो घोड़े की बाग नहीं मोड़ेगा। यहां पर एते ते के लिये हइ ति, खड्गा: के लिये खग्ग हस्वान्त रूप प्रयुक्त है । शृंगार और वीर का मिश्रित रूप देखिये:
संगर- स एं हिं जु बण्णिअइ देकखु अम्हारा कन्तु ।
अइमत हं चत्तं कुसहं गय-कुंभइ दारन्तु ॥ ३४५-१ सैकड़ों युद्धों में जिसकी प्रशंसा की जाती है, ऐसे अत्यन्त मत्त तथा इकुश की कुछ भी पर्वाह नहीं करने वाले गजों के कुम्भस्थलों को विदारने वाले मेरे कान्त को तो देखो। वियोग शृङगार का उदाहरण देखिये :
जे महु दिण्णा दिअहडा दइएँ पवसन्तेण ।
ताण गणन्ति ए अंगुलिउ जज्जरिआउ नेहण ॥८-४-३३३ १ -पुरानी हिन्दी-पं० चंद्रधर शर्मा गुलेरी-पृष्ठ १२९