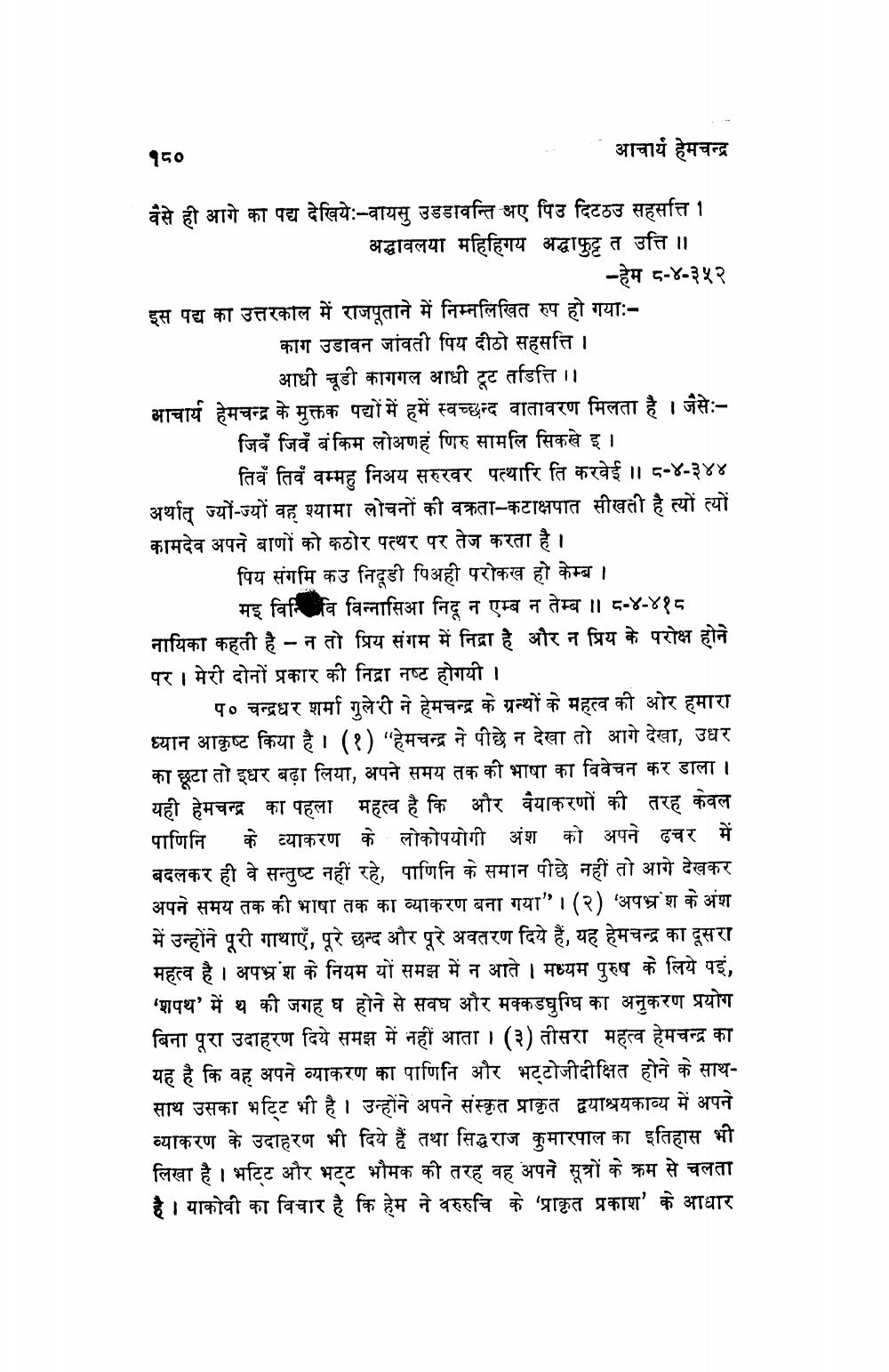________________
आचार्य हेमचन्द्र
वैसे ही आगे का पद्य देखिये :- वायसु उडडावन्ति अए पिउ दिटठउ सहसत्ति 1 अद्धा लया महिहिगय अद्धाफुट्ट त उत्ति ॥ - हेम ८-४-३५२
इस पद्य का उत्तरकाल में राजपूताने में निम्नलिखित रुप हो गया :काग उडावन जांवती पिय दीठो सहसति । आधी चूडी कागगल आधी टूट तडित्ति ।।
आचार्य हेमचन्द्र के मुक्तक पद्यों में हमें स्वच्छन्द वातावरण मिलता है । जैसे:जिवँ जिवँ बंकिम लोअणहं णिरु सामलि सिकखे इ ।
१८०
ति तिवँ वम्महु निअय सरुरवर पत्थारि ति करवेई ।। ८-४-३४४ अर्थात् ज्यों-ज्यों वह श्यामा लोचनों की वक्रता - कटाक्षपात सीखती है त्यों त्यों कामदेव अपने बाणों को कठोर पत्थर पर तेज करता है ।
पिय संगम कउ निदूडी पिअही परोकख हो केम्ब ।
इविवि विन्नासिआ निदू न एम्ब न तेम्ब ।। ८-४-४१८ नायिका कहती है - न तो प्रिय संगम में निद्रा है और न प्रिय के परोक्ष होने पर। मेरी दोनों प्रकार की निद्रा नष्ट होगयी ।
प० चन्द्रधर शर्मा गुलेरी ने हेमचन्द्र के ग्रन्थों के महत्व की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है । (१) "हेमचन्द्र ने पीछे न देखा तो आगे देखा, उधर का छूटा तो इधर बढ़ा लिया, अपने समय तक की भाषा का विवेचन कर डाला । यही हेमचन्द्र का पहला महत्व है कि और वैयाकरणों की तरह केवल पाणिनि के व्याकरण के लोकोपयोगी अंश को अपने दचर में बदलकर ही वे सन्तुष्ट नहीं रहे, पाणिनि के समान पीछे नहीं तो आगे देखकर अपने समय तक की भाषा तक का व्याकरण बना गया" । (२) 'अपभ्रंश के अंश में उन्होंने पूरी गाथाएँ, पूरे छन्द और पूरे अवतरण दिये हैं, यह हेमचन्द्र का दूसरा महत्व है | अपभ्रंश के नियम यों समझ में न आते । मध्यम पुरुष के लिये पई, 'शपथ' में थ की जगह घ होने से सवघ और मक्कडघुग्धि का अनुकरण प्रयोग बिना पूरा उदाहरण दिये समझ में नहीं आता । ( ३ ) तीसरा महत्व हेमचन्द्र का यह है कि वह अपने व्याकरण का पाणिनि और भट्टोजीदीक्षित होने के साथसाथ उसका भट्टि भी है । उन्होंने अपने संस्कृत प्राकृत द्वयाश्रयकाव्य में अपने व्याकरण के उदाहरण भी दिये हैं तथा सिद्धराज कुमारपाल का इतिहास भी लिखा है । भट्टि और भट्ट भौमक की तरह वह अपने सूत्रों के क्रम से चलता है । याकोवी का विचार है कि हम ने वरुरुचि के 'प्राकृत प्रकाश' के आधार