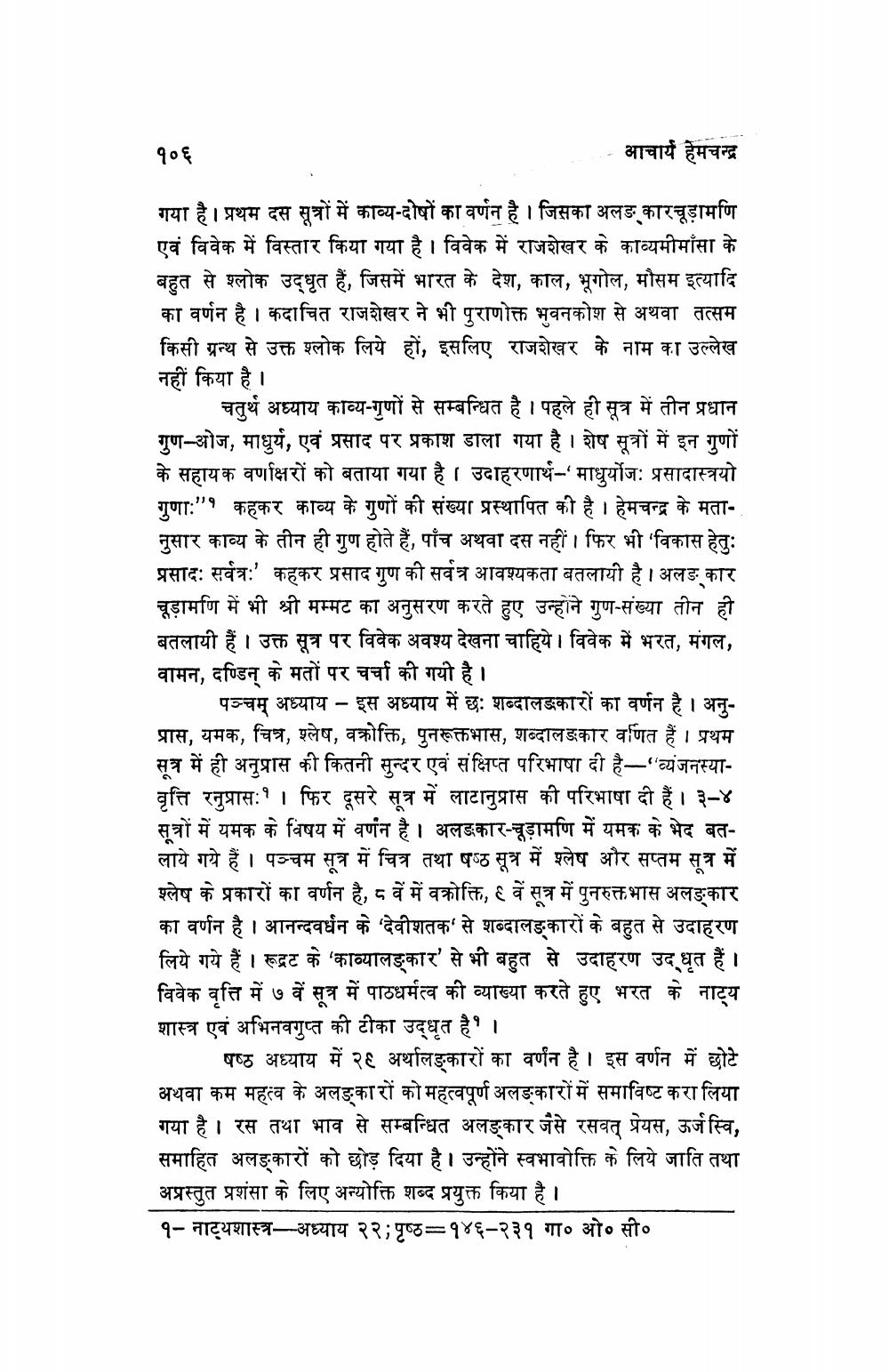________________
१०६
आचार्य हेमचन्द्र
गया है। प्रथम दस सूत्रों में काव्य-दोषों का वर्णन है । जिसका अलङ कारचूड़ामणि एवं विवेक में विस्तार किया गया है। विवेक में राजशेखर के काव्यमीमांसा के बहुत से श्लोक उद्धृत हैं, जिसमें भारत के देश, काल, भूगोल, मौसम इत्यादि का वर्णन है । कदाचित राजशेखर ने भी पुराणोक्त भुवनकोश से अथवा तत्सम किसी ग्रन्थ से उक्त श्लोक लिये हों, इसलिए राजशेखर के नाम का उल्लेख नहीं किया है।
__ चतुर्थ अध्याय काव्य-गुणों से सम्बन्धित है । पहले ही सूत्र में तीन प्रधान गुण-ओज, माधुर्य, एवं प्रसाद पर प्रकाश डाला गया है । शेष सूत्रों में इन गुणों के सहायक वर्णाक्षरों को बताया गया है । उदाहरणार्थ-' माधुर्योज: प्रसादास्त्रयो गुणाः"१ कहकर काव्य के गुणों की संख्या प्रस्थापित की है । हेमचन्द्र के मतानुसार काव्य के तीन ही गुण होते हैं, पाँच अथवा दस नहीं। फिर भी 'विकास हेतुः प्रसादः सर्वत्रः' कहकर प्रसाद गुण की सर्वत्र आवश्यकता बतलायी है। अलङ कार चूड़ामणि में भी श्री मम्मट का अनुसरण करते हुए उन्होंने गुण-संख्या तीन ही बतलायी हैं । उक्त सूत्र पर विवेक अवश्य देखना चाहिये। विवेक में भरत, मंगल, वामन, दण्डिन् के मतों पर चर्चा की गयी है।
__ पञ्चम् अध्याय - इस अध्याय में छः शब्दालङकारों का वर्णन है । अनुप्रास, यमक, चित्र, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरूक्तभास, शब्दालङकार वर्णित हैं । प्रथम सूत्र में ही अनुप्रास की कितनी सुन्दर एवं संक्षिप्त परिभाषा दी है- "व्यंजनस्यावृत्ति रनुप्रासः । फिर दूसरे सूत्र में लाटानुप्रास की परिभाषा दी हैं। ३-४ सूत्रों में यमक के विषय में वर्णन है। अलङकार-चूड़ामणि में यमक के भेद बतलाये गये हैं। पञ्चम सूत्र में चित्र तथा षष्ठ सूत्र में श्लेष और सप्तम सूत्र में श्लेष के प्रकारों का वर्णन है, ८ वें में वक्रोक्ति, ६ वें सूत्र में पुनरुक्तभास अलङ्कार का वर्णन है । आनन्दवर्धन के 'देवीशतक' से शब्दालङ्कारों के बहुत से उदाहरण लिये गये हैं । रूद्रट के 'काव्यालङ्कार' से भी बहुत से उदाहरण उद धृत हैं। विवेक वृत्ति में ७ वें सूत्र में पाठधर्मत्व की व्याख्या करते हुए भरत के नाट्य शास्त्र एवं अभिनवगुप्त की टीका उद्धृत है ।
___षष्ठ अध्याय में २६ अर्थालङ्कारों का वर्णन है। इस वर्णन में छोटे अथवा कम महत्व के अलङ्कारों को महत्वपूर्ण अलङ्कारों में समाविष्ट करा लिया गया है। रस तथा भाव से सम्बन्धित अलङ्कार जैसे रसवत् प्रेयस, ऊर्जस्वि, समाहित अलङ्कारों को छोड़ दिया है। उन्होंने स्वभावोक्ति के लिये जाति तथा अप्रस्तुत प्रशंसा के लिए अन्योक्ति शब्द प्रयुक्त किया है। १- नाट्यशास्त्र अध्याय २२; पृष्ठ= १४६-२३१ गा० ओ० सी०