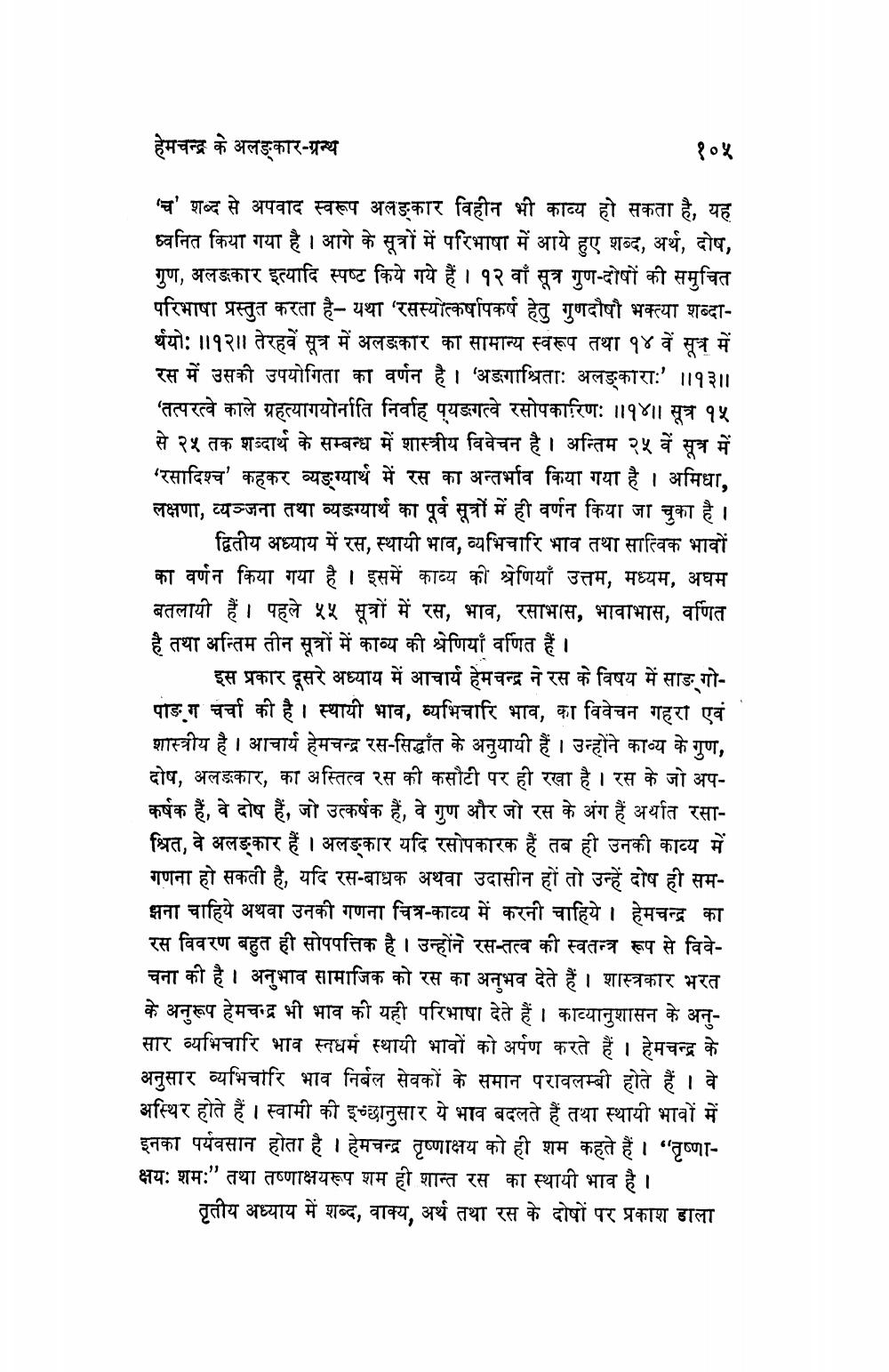________________
हेमचन्द्र के अलङ्कार-ग्रन्थ
१०५
'च' शब्द से अपवाद स्वरूप अलङ्कार विहीन भी काव्य हो सकता है, यह ध्वनित किया गया है । आगे के सूत्रों में परिभाषा में आये हुए शब्द, अर्थ, दोष, गुण, अलङकार इत्यादि स्पष्ट किये गये हैं । १२ वाँ सूत्र गुण-दोषों की समुचित परिभाषा प्रस्तुत करता है- यथा 'रसस्योत्कर्षापकर्ष हेतु गुणदोषौ भक्त्या शब्दार्थयोः ॥१२॥ तेरहवें सूत्र में अलङकार का सामान्य स्वरूप तथा १४ वें सूत्र में रस में उसकी उपयोगिता का वर्णन है। 'अङगाश्रिताः अलङ्काराः' ॥१३॥ 'तत्परत्वे काले ग्रहत्यागयो ति निर्वाह प्यङगत्वे रसोपकारिणः ॥१४॥ सूत्र १५ से २५ तक शब्दार्थ के सम्बन्ध में शास्त्रीय विवेचन है। अन्तिम २५ वें सूत्र में 'रसादिश्च' कहकर व्यङ्ग्यार्थ में रस का अन्तर्भाव किया गया है । अमिधा, लक्षणा, व्यञ्जना तथा व्यङग्यार्थ का पूर्व सूत्रों में ही वर्णन किया जा चुका है ।
द्वितीय अध्याय में रस, स्थायी भाव, व्यभिचारि भाव तथा सात्विक भावों का वर्णन किया गया है । इसमें काव्य की श्रेणियाँ उत्तम, मध्यम, अघम बतलायी हैं। पहले ५५ सूत्रों में रस, भाव, रसाभास, भावाभास, वणित है तथा अन्तिम तीन सूत्रों में काव्य की श्रेणियाँ वर्णित हैं।
इस प्रकार दूसरे अध्याय में आचार्य हेमचन्द्र ने रस के विषय में साङ गोपाङ ग चर्चा की है। स्थायी भाव, व्यभिचारि भाव, का विवेचन गहरा एवं शास्त्रीय है । आचार्य हेमचन्द्र रस-सिद्धांत के अनुयायी हैं । उन्होंने काव्य के गुण, दोष, अलङ्कार, का अस्तित्व रस की कसौटी पर ही रखा है । रस के जो अपकर्षक हैं, वे दोष हैं, जो उत्कर्षक हैं, वे गुण और जो रस के अंग हैं अर्थात रसाश्रित, वे अलङ्कार हैं । अलङ्कार यदि रसोपकारक हैं तब ही उनकी काव्य में गणना हो सकती है, यदि रस-बाधक अथवा उदासीन हों तो उन्हें दोष ही समझना चाहिये अथवा उनकी गणना चित्र-काव्य में करनी चाहिये । हेमचन्द्र का रस विवरण बहुत ही सोपपत्तिक है। उन्होंने रस-तत्व की स्वतन्त्र रूप से विवेचना की है। अनुभाव सामाजिक को रस का अनुभव देते हैं। शास्त्रकार भरत के अनुरूप हेमचन्द्र भी भाव की यही परिभाषा देते हैं । काव्यानुशासन के अनुसार व्यभिचारि भाव स्नधर्म स्थायी भावों को अर्पण करते हैं । हेमचन्द्र के अनुसार व्यभिचारि भाव निर्बल सेवकों के समान परावलम्बी होते हैं । वे अस्थिर होते हैं । स्वामी की इच्छानुसार ये भाव बदलते हैं तथा स्थायी भावों में इनका पर्यवसान होता है । हेमचन्द्र तृष्णाक्षय को ही शम कहते हैं । "तृष्णाक्षयः शमः" तथा तष्णाक्षयरूप शम ही शान्त रस का स्थायी भाव है।
तृतीय अध्याय में शब्द, वाक्य, अर्थ तथा रस के दोषों पर प्रकाश डाला