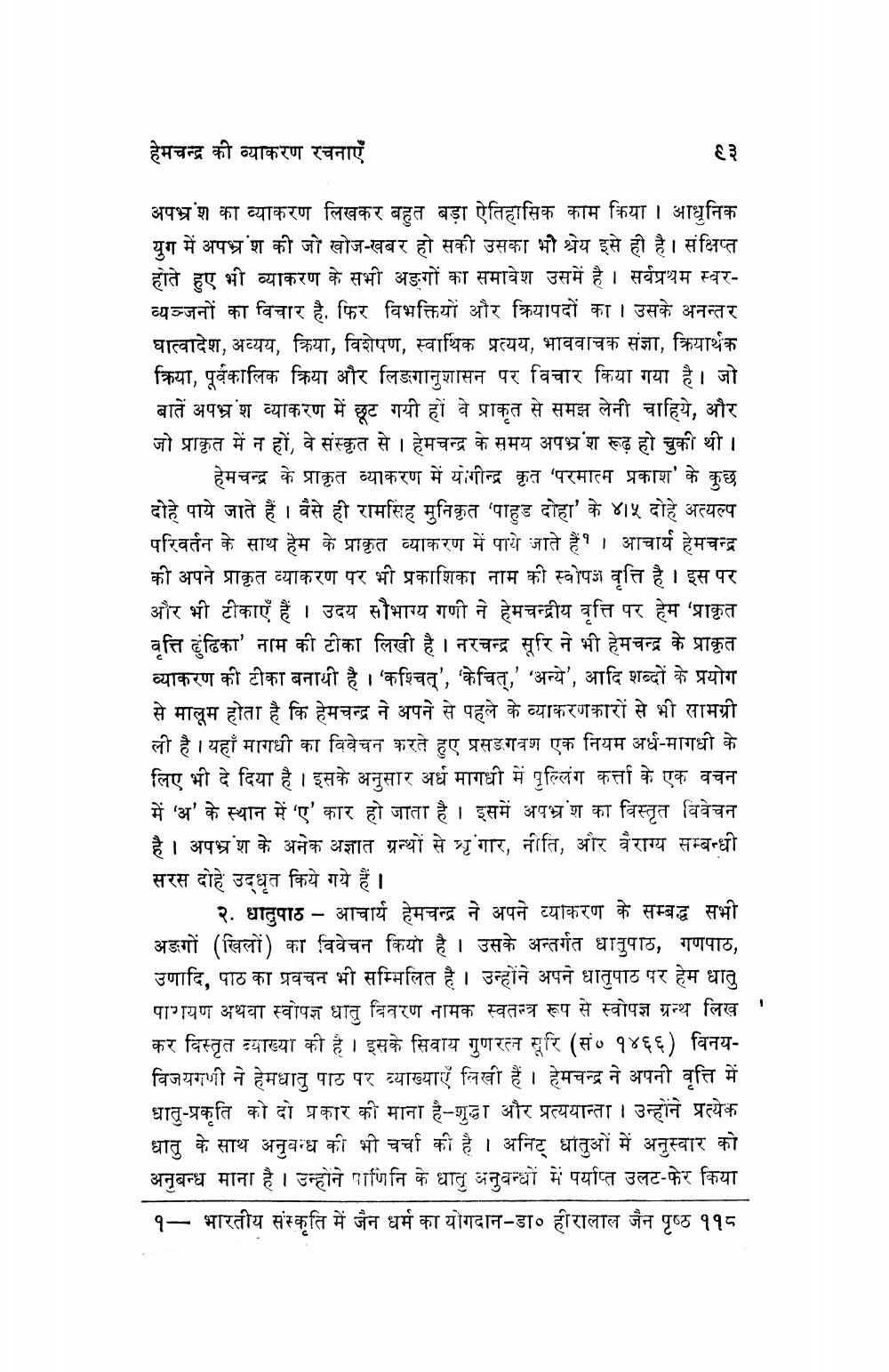________________
हेमचन्द्र की व्याकरण रचनाएँ
अपभ्रश का व्याकरण लिखकर बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम किया । आधुनिक युग में अपभ्रश की जो खोज-खबर हो सकी उसका भी श्रेय इसे ही है। संक्षिप्त होते हुए भी व्याकरण के सभी अङगों का समावेश उसमें है। सर्वप्रथम स्वरव्यञ्जनों का विचार है. फिर विभक्तियों और क्रियापदों का । उसके अनन्तर घात्वादेश, अव्यय, क्रिया, विशेषण, स्वार्थिक प्रत्यय, भाववाचक संज्ञा, क्रियार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और लिङगानुशासन पर विचार किया गया है। जो बातें अपभ्रश व्याकरण में छूट गयी हों वे प्राकृत से समझ लेनी चाहिये, और जो प्राकृत में न हों, वे संस्कृत से । हेमचन्द्र के समय अपभ्रंश रूढ़ हो चुकी थी।
हेमचन्द्र के प्राकृत व्याकरण में योगीन्द्र कृत 'परमात्म प्रकाश' के कुछ दोहे पाये जाते हैं । वैसे ही रामसिंह मुनिकृत 'पाहुड दोहा' के ४।५ दोहे अत्यल्प परिवर्तन के साथ हेम के प्राकृत व्याकरण में पाये जाते हैं । आचार्य हेमचन्द्र की अपने प्राकृत व्याकरण पर भी प्रकाशिका नाम की स्वोपन वृत्ति है । इस पर और भी टीकाएँ हैं । उदय सौभाग्य गणी ने हेमचन्द्रीय वृत्ति पर हेम 'प्राकृत वृत्ति ढुंढिका' नाम की टीका लिखी है । नरचन्द्र सूरि ने भी हेमचन्द्र के प्राकृत व्याकरण की टीका बनायी है । 'कश्चित्', 'केचित्,' 'अन्ये', आदि शब्दों के प्रयोग से मालूम होता है कि हेमचन्द्र ने अपने से पहले के व्याकरणकारों से भी सामग्री ली है । यहाँ मागधी का विवेचन करते हुए प्रसङगवश एक नियम अर्ध-मागधी के लिए भी दे दिया है । इसके अनुसार अर्ध मागधी में पुल्लिंग कर्ता के एक वचन में 'अ' के स्थान में 'ए' कार हो जाता है। इसमें अपभ्रश का विस्तृत विवेचन है। अपभ्रश के अनेक अज्ञात ग्रन्थों से शृगार, नीति, और वैराग्य सम्बन्धी सरस दोहे उद्धृत किये गये हैं।
२. धातुपाठ - आचार्य हेमचन्द्र ने अपने व्याकरण के सम्बद्ध सभी अङगों (खिलों) का विवेचन कियो है । उसके अन्तर्गत धातुपाठ, गणपाठ, उणादि, पाठ का प्रवचन भी सम्मिलित है। उन्होंने अपने धातुपाठ पर हेम धातु पारायण अथवा स्वोपज्ञ धातु विवरण नामक स्वतन्त्र रूप से स्वोपज्ञ ग्रन्थ लिख । कर विस्तृत व्याख्या की है । इसके सिवाय गुणरत्न सूरि (सं० १४६६) विनयविजयगणी ने हेमधातु पाठ पर व्याख्याएँ लिखी हैं । हेमचन्द्र ने अपनी वृत्ति में धातु-प्रकृति को दो प्रकार की माना है-शुद्धा और प्रत्ययान्ता । उन्होंने प्रत्येक धातु के साथ अनुबन्ध की भी चर्चा की है । अनिट् धातुओं में अनुस्वार को अनुबन्ध माना है । उन्होंने पाणिनि के धातु अनुबन्धों में पर्याप्त उलट-फेर किया १- भारतीय संस्कृति में जैन धर्म का योगदान-डा० हीरालाल जैन पृष्ठ ११८