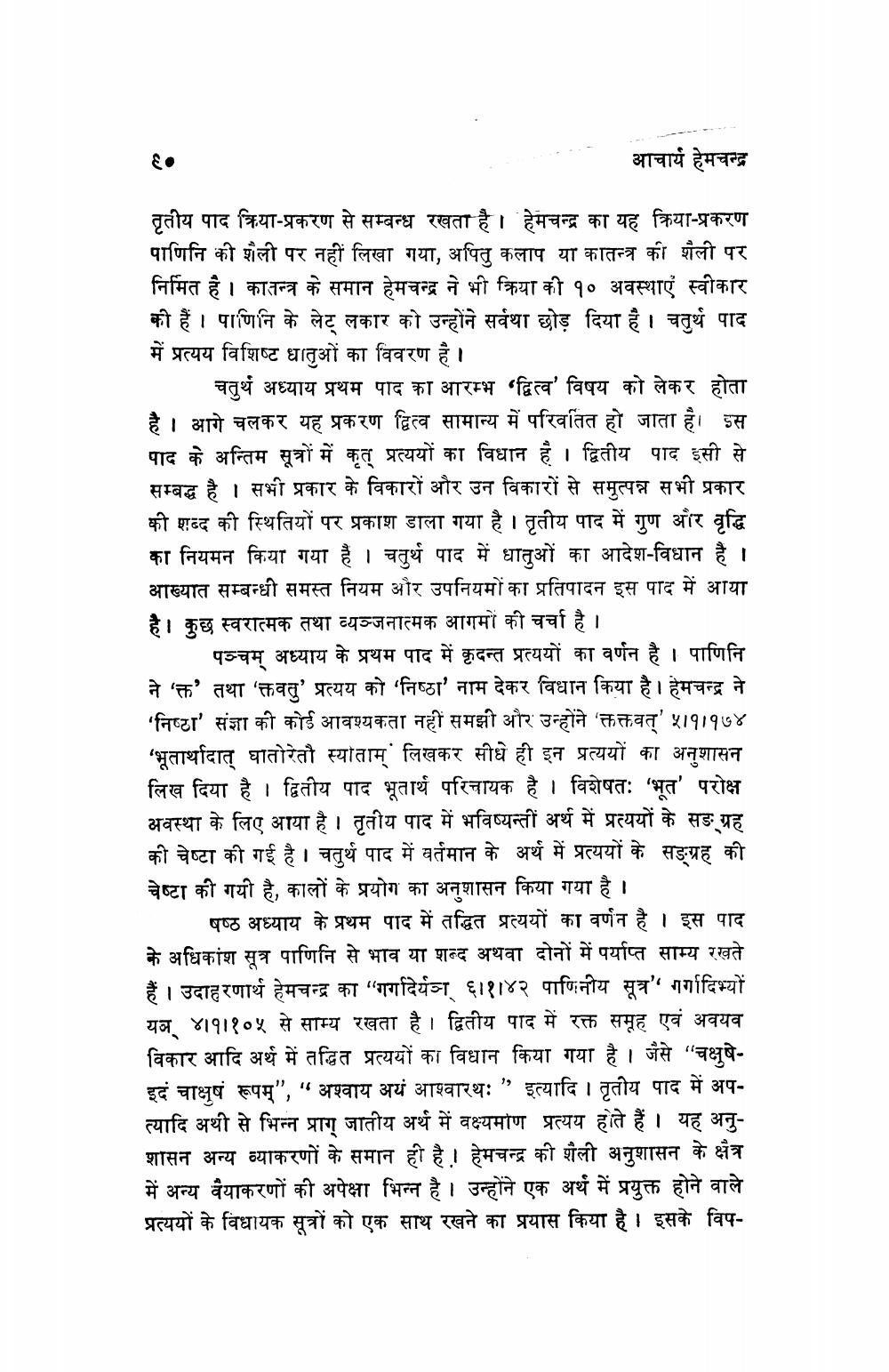________________
आचार्य हेमचन्द्र
तृतीय पाद क्रिया-प्रकरण से सम्बन्ध रखता है। हेमचन्द्र का यह क्रिया-प्रकरण पाणिनि की शैली पर नहीं लिखा गया, अपितु कलाप या कातन्त्र की शैली पर निर्मित है। कातन्त्र के समान हेमचन्द्र ने भी क्रिया की १० अवस्थाएं स्वीकार की हैं । पाणिनि के लेट् लकार को उन्होंने सर्वथा छोड़ दिया है। चतुर्थ पाद में प्रत्यय विशिष्ट धातुओं का विवरण है।
चतुर्थ अध्याय प्रथम पाद का आरम्भ 'द्वित्व' विषय को लेकर होता है। आगे चलकर यह प्रकरण द्वित्व सामान्य में परिवर्तित हो जाता है। इस पाद के अन्तिम सूत्रों में कृत् प्रत्ययों का विधान है । द्वितीय पाद इसी से सम्बद्ध है । सभी प्रकार के विकारों और उन विकारों से समुत्पन्न सभी प्रकार की शब्द की स्थितियों पर प्रकाश डाला गया है । तृतीय पाद में गुण और वृद्धि का नियमन किया गया है । चतुर्थ पाद में धातुओं का आदेश-विधान है । आख्यात सम्बन्धी समस्त नियम और उपनियमों का प्रतिपादन इस पाद में आया है। कुछ स्वरात्मक तथा व्यञ्जनात्मक आगमों की चर्चा है ।
पञ्चम् अध्याय के प्रथम पाद में कृदन्त प्रत्ययों का वर्णन है । पाणिनि ने 'क्त' तथा 'क्तवतु' प्रत्यय को 'निष्ठा' नाम देकर विधान किया है। हेमचन्द्र ने 'निष्ठा' संज्ञा की कोई आवश्यकता नहीं समझी और उन्होंने 'क्तक्तवत्' ५।१।१७४ 'भूतार्थादात् घातोरेतौ स्योताम् लिखकर सीधे ही इन प्रत्ययों का अनुशासन लिख दिया है । द्वितीय पाद भूतार्थ परिचायक है । विशेषत: 'भूत' परोक्ष अवस्था के लिए आया है। तृतीय पाद में भविष्यन्ती अर्थ में प्रत्ययों के सङ ग्रह की चेष्टा की गई है। चतुर्थ पाद में वर्तमान के अर्थ में प्रत्ययों के सङ्ग्रह की चेष्टा की गयी है, कालों के प्रयोग का अनुशासन किया गया है ।
षष्ठ अध्याय के प्रथम पाद में तद्धित प्रत्ययों का वर्णन है । इस पाद के अधिकांश सूत्र पाणिनि से भाव या शब्द अथवा दोनों में पर्याप्त साम्य रखते हैं । उदाहरणार्थ हेमचन्द्र का “गर्गादेर्यञ ६।१।४२ पाणिनीय सूत्र'' गर्गादिभ्यों या ४।१।१०५ से साम्य रखता है। द्वितीय पाद में रक्त समूह एवं अवयव विकार आदि अर्थ में तद्धित प्रत्ययों का विधान किया गया है। जैसे "चक्षुषेइदं चाक्षुषं रूपम्", " अश्वाय अयं आश्वारथः” इत्यादि । तृतीय पाद में अपत्यादि अथी से भिन्न प्राग् जातीय अर्थ में वक्ष्यमाण प्रत्यय होते हैं। यह अनुशासन अन्य व्याकरणों के समान ही है । हेमचन्द्र की शैली अनुशासन के क्षेत्र में अन्य वैयाकरणों की अपेक्षा भिन्न है। उन्होंने एक अर्थ में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों के विधायक सूत्रों को एक साथ रखने का प्रयास किया है। इसके विप