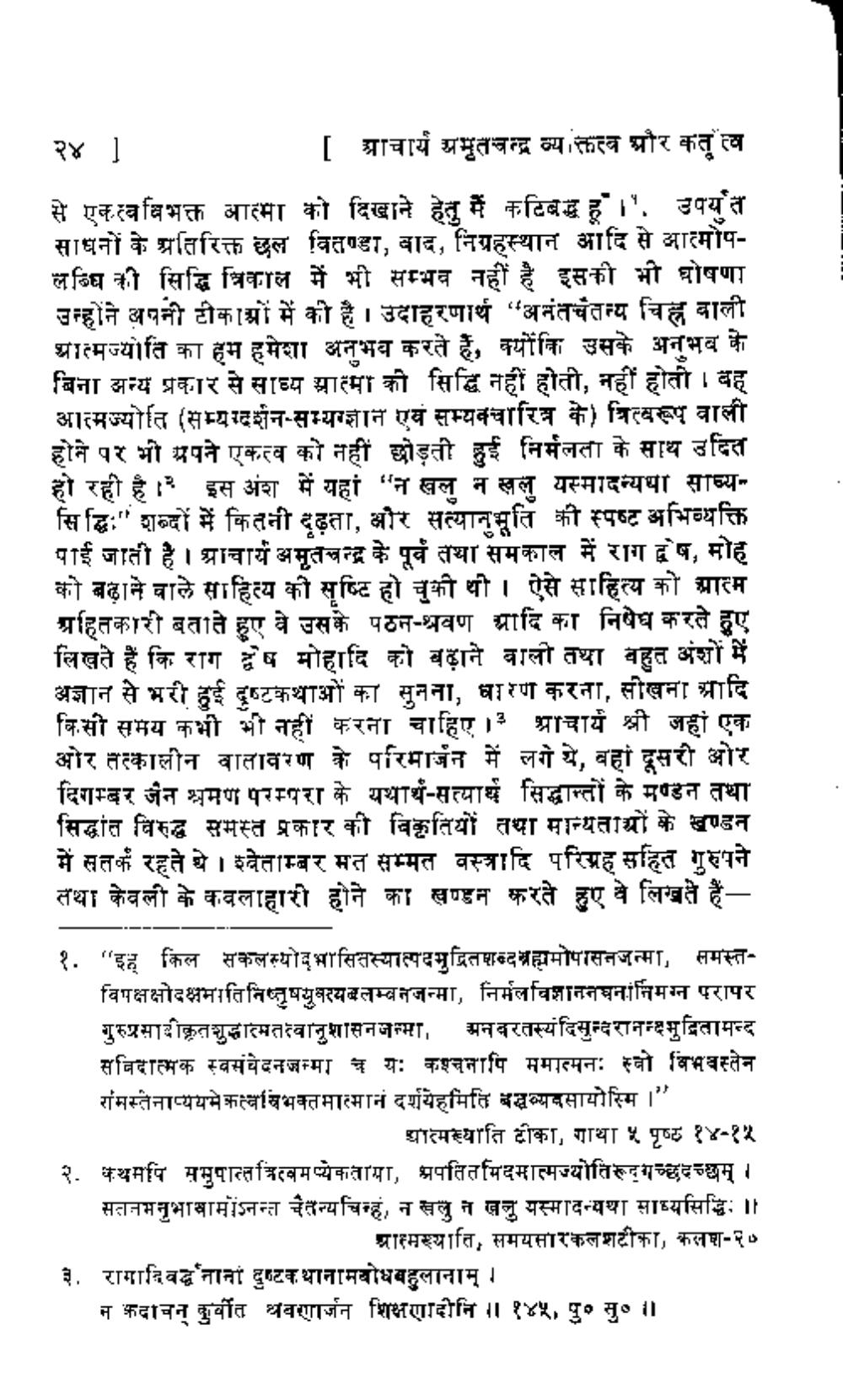________________
२४ ]
[ प्राचार्य अमृतचन्द्र व्यक्तित्व और कतु त्व से एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाने हेतु में कटिबद्ध हूँ।'. उपर्युत साधनों के अतिरिक्त छल वितण्डा, वाद, निग्रहस्थान आदि से आत्मोपलब्धि की सिद्धि त्रिकाल में भी सम्भव नहीं है इसकी भी घोषणा उन्होंने अपनी टीकाओं में की है। उदाहरणार्थ "अनंतचतन्य चिह्न वाली प्रात्मज्योति का हम हमेशा अनुभव करते हैं, क्योंकि उसके अनुभव के बिना अन्य प्रकार से साध्य नात्मा की सिद्धि नहीं होती, नहीं होती । वह आत्मज्योति (सम्यग्दर्शन-सम्यग्ज्ञान एवं सम्यक्चारित्र के) त्रित्वरूप वाली होने पर भी अपने एकत्व को नहीं छोड़ती हुई निर्मलता के साथ उदित हो रही है। इस अंश' में यहां "न खल न खल यस्मादन्यथा साध्यसिद्धिः" शब्दों में कितनी दढ़ता, और सत्यानभूति की स्पष्ट अभिव्यक्ति पाई जाती है । प्राचार्य अमृतचन्द्र के पूर्व तथा समकाल में राग द्वेष, मोह को बढ़ाने वाले साहित्य की सृष्टि हो चुकी थी। ऐसे साहित्य को प्रात्म अहितकारी बताते हुए वे उसके पठन-श्रवण आदि का निषेध करते हुए लिखते हैं कि राग द्वेष मोहादि को बढ़ाने वाली तथा वहत अंशों में अज्ञान से भरी हुई दुष्टकथाओं का सुनना, धारण करना, सीखना आदि किसी समय कभी भी नहीं करना चाहिए। प्राचार्य श्री जहां एक
ओर तत्कालीन वातावरण के परिमार्जन में लगे थे, वहां दूसरी ओर दिगम्बर जैन श्चमण परम्परा के यथार्थ-सत्यार्थ सिद्धान्तों के मण्डन तथा सिद्धांत विरुद्ध समस्त प्रकार की विकृतियों तथा मान्यताओं के खण्डन में सतर्क रहते थे। श्वेताम्बर मत सम्मत वस्त्रादि परिग्रह सहित गुरुपने तथा केवली के कवलाहारी होने का खण्डन करते हुए वे लिखते हैं
१. "इह किल सकलस्योद्भासितस्यात्पदमुद्रितशब्दब्रह्ममोपासनजन्मा, समस्त
विपक्षक्षोदक्षमातिनिष्तुषयुवस्यबलम्बनजन्मा, निर्मलविज्ञाननघनानिमग्न परापर गुरुप्रसादीकृतशुद्धात्मतत्वानुशासनजन्मा, अनवरतस्यंदिसुन्दरानन्दमुद्रितामन्द सविदात्मक स्वसंवेदनजन्मा च यः कश्चनापि ममात्मनः स्वो विभवस्तेन रांमस्तनाप्ययमेकत्वविभक्तमात्मानं दर्शयेहमिति बसव्यवसायोस्मि ।"
__ यात्मख्याति टीका, गाथा ५ पृष्ठ १४-१५ २. कथमपि ममुपान्तत्रित्वमप्येकतामा, अपतितमिदमात्मज्योतिरूद्गच्छदच्छम् । सतनमनुभाषामोऽनन्त चैतन्य चिन्हं, न खलु न खलु यस्मादन्यथा साध्यसिद्धिः ।।
प्रास्मस्याति, समयसारकलशटीका, कलश-२० ३. रागादिवर्द्धनाना दुष्टक थानामबोधबहुलानाम् ।
न कदाचन कुर्वीत श्रवणार्जन शिक्षणादीनि ।। १४५, पु० सु० ॥