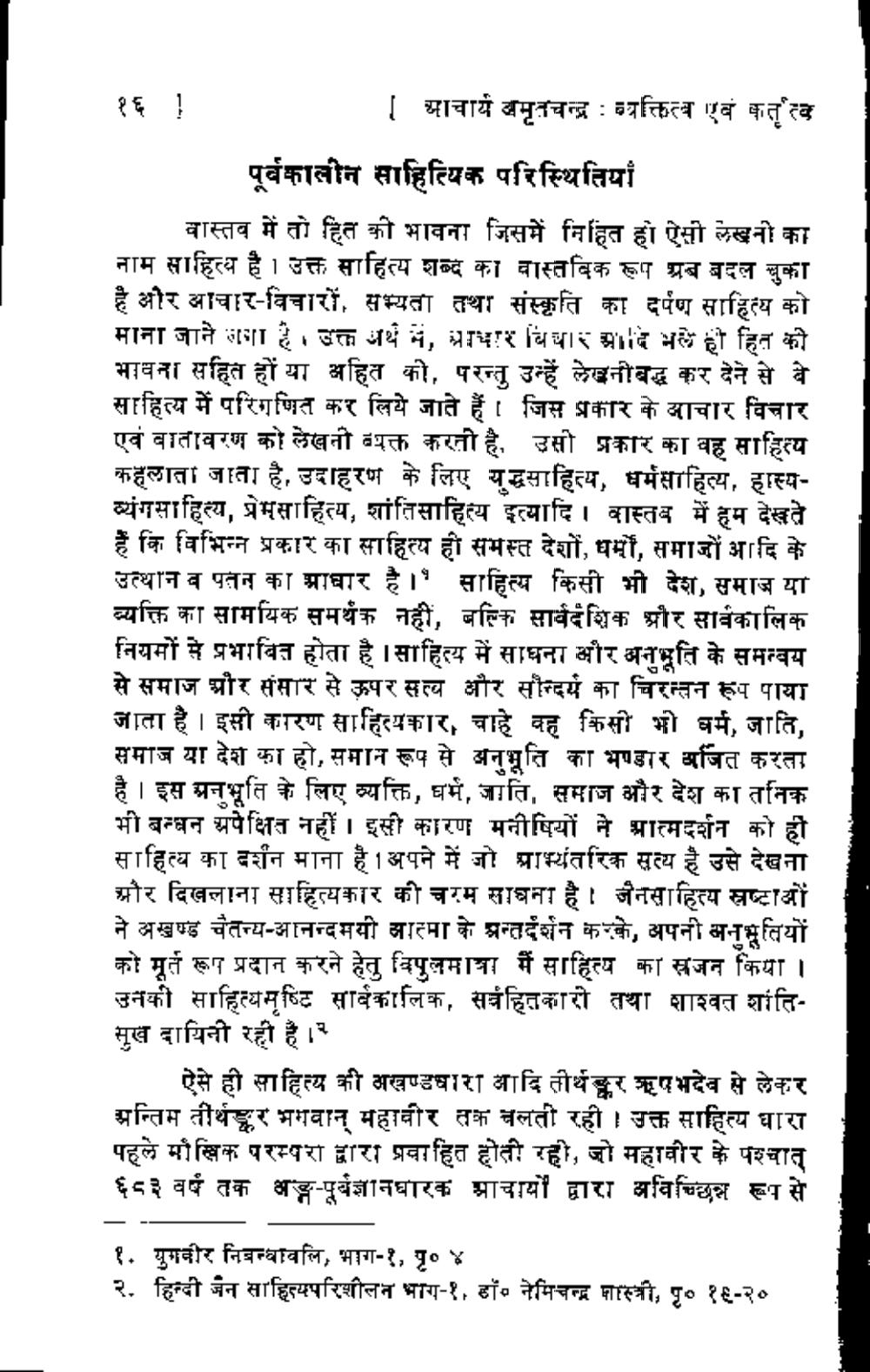________________
१६ !
। आचार्य अमृतचन्द्र : व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व
पूर्वकालीन साहित्यिक परिस्थितियाँ वास्तव में तो हित की भावना जिसमें निहित हो ऐसी लेखनी का नाम साहित्य है । उक्त साहित्य शब्द का वास्तविक रूप अब बदल चुका है और आचार-विचारों, सभ्यता तथा संस्कृति का दर्पण साहित्य को माना जाने लगा है। उक्त अर्थ में, प्राचार बिचार प्रादि भले ही हित को भावना सहित हों या अहित को, परन्तु उन्हें लेखनीबद्ध कर देने से वे साहित्य में परिगणित कर लिये जाते हैं। जिस प्रकार के आचार विचार एवं वातावरण को लेखती ब्यक्त करती है, उसी प्रकार का वह साहित्य कहलाता जाता है, उदाहरण के लिए युद्धसाहित्य, धर्मसाहित्य, हास्यव्यंगसाहित्य, प्रेमसाहित्य, शांतिसाहित्य इत्यादि । वास्तव में हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार का साहित्य ही समस्त देशों, धर्मों, समाजों आदि के उत्थान व पतन का प्राधार है।' साहित्य किसी भी देश, समाज या व्यक्ति का सामयिक समर्थक नहीं, बल्कि सार्वदेशिक और सार्वकालिक नियमों से प्रभावित होता है । साहित्य में साधना और अनुभूति के समन्वय से समाज और संसार से ऊपर सत्य और सौन्दर्य का चिरन्तन रूप पाया जाता है । इसी कारण साहित्यकार, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, समाज या देश का हो, समान रूप से अनुभूति का भण्डार जित करता है । इस अनभूति के लिए व्यक्ति, धर्म, जाति, समाज और देश का तनिक भी बन्धन अपेक्षित नहीं। इसी कारण मनीषियों ने प्रात्मदर्शन को ही साहित्य का दर्शन माना है । अपने में जो प्राभ्यंतरिक सत्य है उसे देखना और दिखलाना साहित्यकार की चरम साधना है। जैनसाहित्य स्रष्टाओं ने अखण्ड चैतन्य-आनन्दमयी आत्मा के अन्तर्दर्शन करके, अपनी अनभूतियों को मूर्त रूप प्रदान करने हेतु विपुलमात्रा में साहित्य का स्रजन किया । उनकी साहित्यमृष्टि सार्वकालिक, सर्वहितकारी तथा शाश्वत शांतिसुख दायिनी रही है ।
ऐसे ही साहित्य की अखण्डधारा आदि तीर्थकर ऋषभदेव से लेकर अन्तिम तीर्थङ्कर भगवान महावीर तक चलती रही। उक्त साहित्य धारा पहले मौखिक परम्परा द्वारा प्रवाहित होती रही, जो महावीर के पश्चात् ६८३ वर्ष तक अङ्ग-पूर्वज्ञानधारक प्राचार्यों द्वारा अविच्छिन्न रूप से
१. युगवीर निबन्धावलि, भाग-१, पृ०४ २. हिन्दी जन साहित्यपरिशीलन भाग-१, डॉ. नेमिचन्द्र शास्त्री, पृ० १६-२०