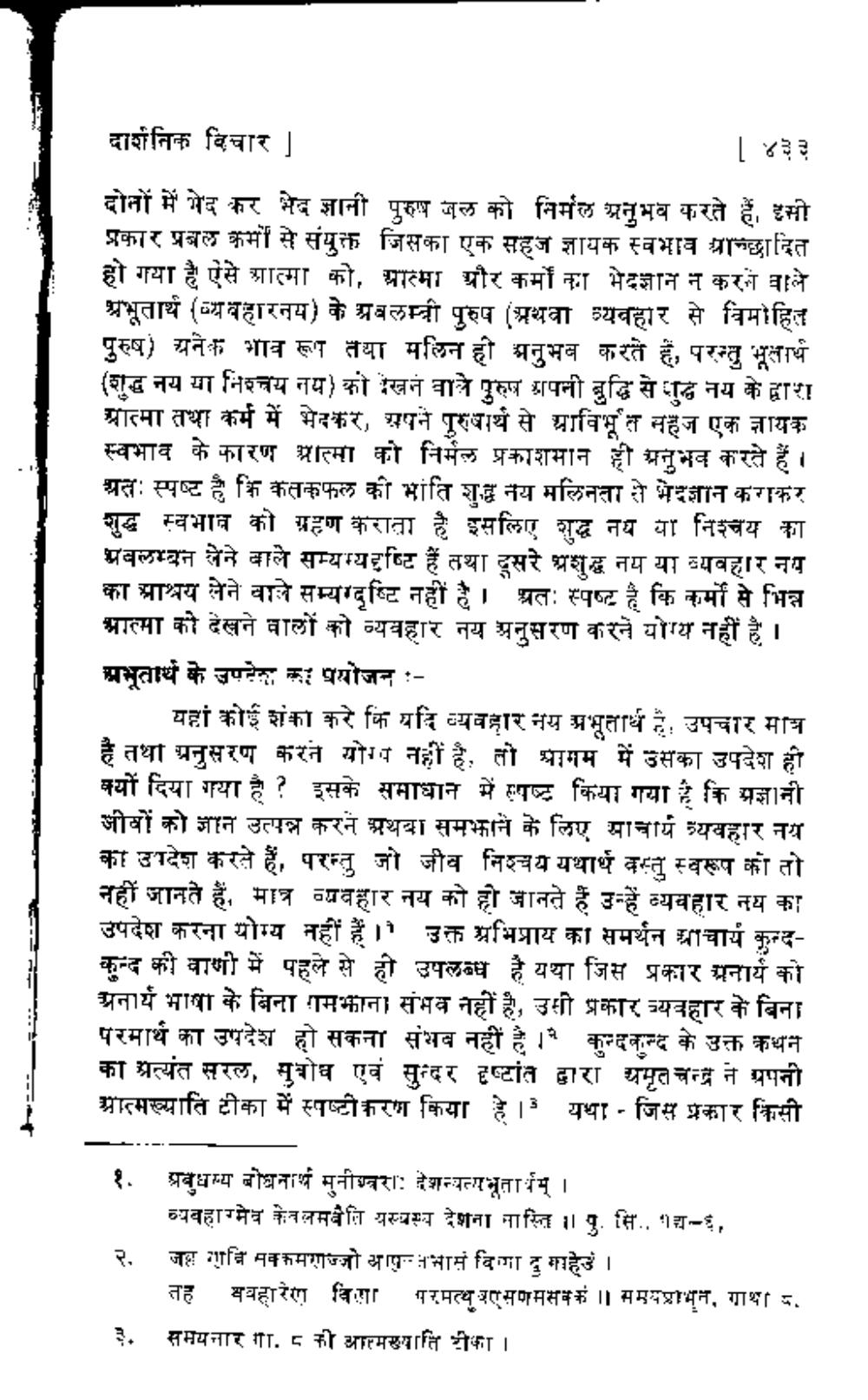________________
दार्शनिक विचार |
दोनों में भेद कर भेद ज्ञानी पुरुष जल को निर्मल अनुभव करते हैं, इमी प्रकार प्रबल कमों से संयुक्त जिसका एक सहज ज्ञायक स्वभाव प्रान्छादित हो गया है ऐसे अात्मा को, पात्मा और कर्मों का भेदज्ञान न करने वाले अभूतार्थ (व्यवहारनय) के अबलम्त्री पुरुष (अथवा व्यवहार से विमोहित पुरुष) अनेक भाव रूप तया मलिन ही अनुभव करते हैं, परन्तु भूतार्थ (शुद्ध नय या निश्चय नय) को देखने वाले पुरुष अपनी बुद्धि से शुद्ध नय के द्वारा प्रात्मा तथा कर्म में भेदकर, अपने पुरुषार्थ से पाविर्भूत महज एक ज्ञायक स्वभाव के कारण प्रात्मा को निर्मल प्रकाशमान ही अनुभव करते हैं। अतः स्पष्ट है कि कतकफल की भांति शुद्ध नय मलिनता से भेदज्ञान कराकर शुद्ध स्वभाव को ग्रहण कराता है इसलिए शुद्ध नय या निश्चय का अवलम्बन लेने वाले सम्यम्यदृष्टि हैं तथा दुसरे अशुद्ध नय या व्यवहार नय का प्राश्रय लेने वाले सम्यग्दृष्टि नहीं है। अतः स्पष्ट है कि कर्मों से भिन्न आत्मा को देखने वालों को व्यवहार नय अनुसरण करने योग्य नहीं है। प्रभूतार्थ के उपदेश का प्रयोजन :
यहां कोई शंका करे कि यदि व्यवहार नय अभूतार्थ है. उपचार मात्र है तथा अनुसरण करने योग्य नहीं है, तो प्रामम में उसका उपदेश ही क्यों दिया गया है ? इसके समाधान में स्पष्ट किया गया है कि प्रज्ञानी जीवों को जान उत्पन्न करने अथवा समझाने के लिए प्राचार्य व्यवहार नय का उपदेश करते हैं, परन्तु जो जीव निश्चय यथार्थ वस्तु स्वरूप को तो नहीं जानते हैं, मात्र व्यवहार नय को ही जानते हैं उन्हें व्यवहार नय का उपदेश करना योग्य नहीं है। उक्त अभिप्राय का समर्थन प्राचार्य कुन्दकन्द की वाणी में पहले से ही उपलब्ध है यथा जिस प्रकार अनार्य को अनार्य भाषा के बिना गमभाना संभव नहीं है, उसी प्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश हो सकना संभव नहीं है । कुन्दकुन्द के उक्त कथन का अत्यंत सरल, सुबोध एवं सुन्दर दृष्टांत द्वारा अमृत चन्द्र ने अपनी प्रात्मख्याति टीका में स्पष्टीकरण किया है। यथा- जिस प्रकार किसी
१. अबुधम्य बोधनार्थ मुनीश्वरा: देशन्यत्यभूतार्थम् ।।
व्यवहारमेव केवलमवैति यस्यस्य देशना नास्ति ।। यु. सि.. 'द्य-, २. जहानि मक्कमज्जो आपनमा विमा दमाहेउं ।
तह ववहारेण विणा परमत्थु एसण मसक्कं ।। ममयप्रामुन, गाथा ८. ३. समयनार गा. ८ की आत्मख्याति टीका ।