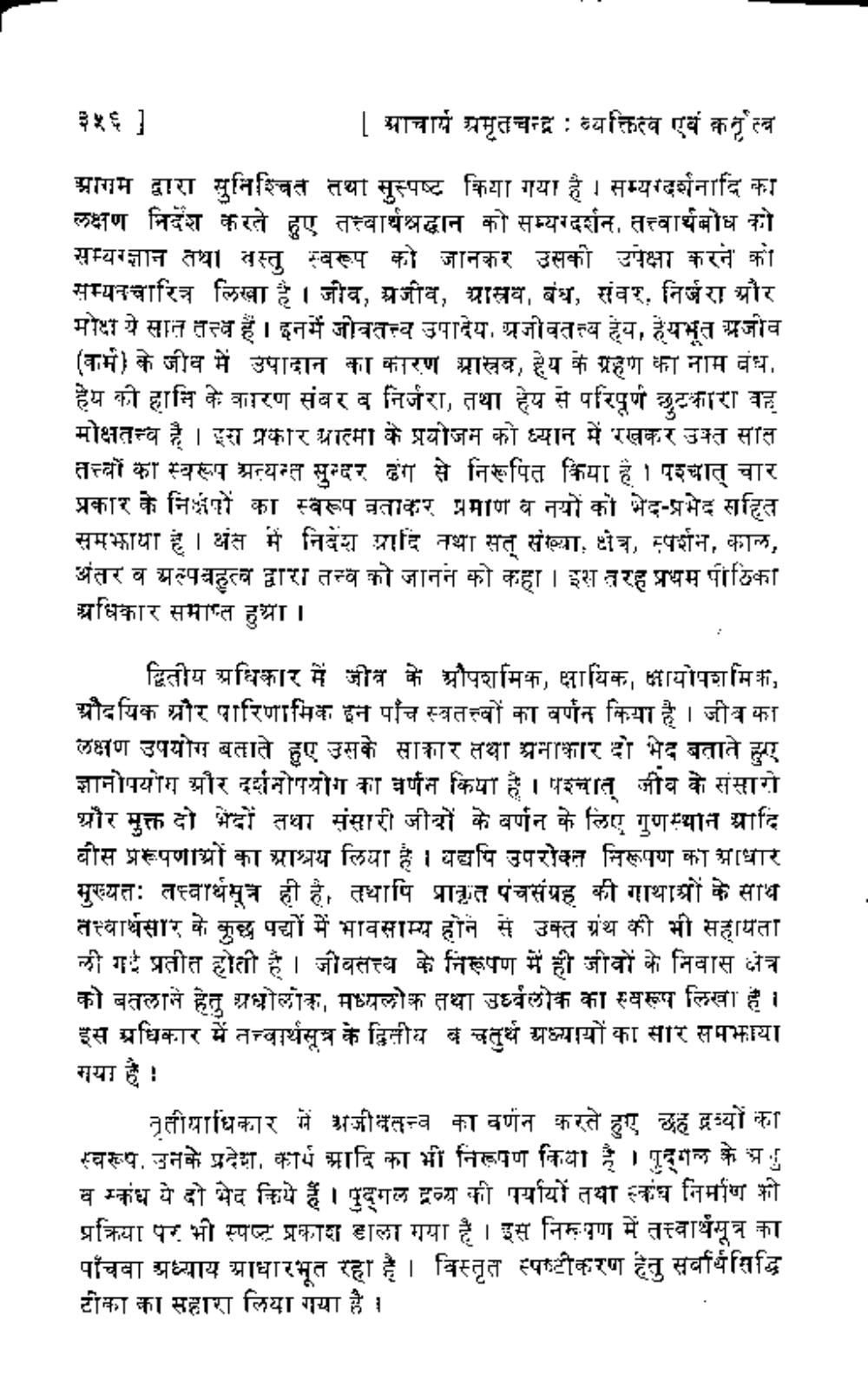________________
[ प्राचार्य अमृतचन्द्र : व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व
मागम द्वारा सुनिश्चित तथा सुस्पष्ट किया गया है । सम्यग्दर्शनादि का लक्षण निर्देश करते हुए तत्त्वार्थश्रद्धान को सम्यग्दर्शन, तत्त्वार्थबोध को सम्यग्ज्ञान तथा वस्तु स्वरूप को जानकर उसकी उपेक्षा करने को सम्यनचारित्र लिखा है । जीव, अजीव, ग्रासव, बंध, संवर. निर्जरा और मोदा ये सात तत्व हैं। इनमें जीवतत्व उपादेय, अजीवतत्व हेय, हेयभुत अजीव (कर्म) के जीव में उपादान का कारण प्रासब, हेय के ग्रहण का नाम बंध, हेय को हानि के कारण संबर व निर्जरा, तथा हेय से परिपूर्ण छुटकारा वह मोक्षतत्त्व है । इस प्रकार प्रात्मा के प्रयोजन को ध्यान में रखकर उक्त सात तत्त्वों का स्वरूप अत्यन्त सुन्दर ढंग से निरूपित किया है। पश्चात् चार प्रकार के निईगों का स्वरूप बताकर प्रमाण व नयों को भेद-प्रभेद सहित समझाया है । अंत में निवेश यादि नथा सत् संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर व अल्पबहुत्व द्वारा तत्त्व को जानने को कहा । इस तरह प्रथम पीठिका अधिकार समाप्त हुआ।
द्वितीय अधिकार में जीव के औपमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, ग्रौदयिक और पारिणामिका इन पाँच स्वतत्त्वों का वर्णन किया है । जीव का लक्षण उपयोग बताते हुए उसके साकार तथा अनाकार दो भेद बताते हुए ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग का वर्णन किया है। पश्चात् जीव के संसागे
और मुक्त दो भेदों तथा संसारी जीवों के वर्णन के लिए गुणस्थान आदि बीस प्ररूपणाओं का आश्रय लिया है। यद्यपि उपरोक्त निरूपण का आधार मुख्यतः तत्त्वार्थसूत्र ही है, तथापि प्राकृत पंचसंग्रह की गाथाओं के साथ तत्वाधंसार के कुछ पद्यों में भावसाम्य होने से उक्त ग्रंथ की भी सहायता ली गई प्रतीत होती है । जीवतत्त्व के निरूपण में ही जीवों के निवास क्षेत्र को बतलाने हेतु अधोलोक, मध्यलोक तथा उर्ध्वलोक का स्वरूप लिखा है। इस अधिकार में तत्त्वार्थसूत्र के द्वितीय व चतुर्थ अध्यायों का सार समझाया गया है।
नृतीयाधिकार में अजीवतन्व का वर्णन करते हुए छह द्रव्यों का स्वरूप. उनके प्रदेश, कार्य आदि का भी निरूपण किया है । गुदगल के अ: व स्कंध ये दो भेद किये हैं। पुद्गल द्रव्य की पर्यायों तथा स्कंध निर्माण की प्रक्रिया पर भी स्पष्ट प्रकाश डाला गया है । इस निम् पण में तत्त्वार्थसूत्र का पाँचवा अध्याय आधारभूत रहा है । विस्तृत स्पष्टीकरण हेतु सर्वार्थ सिद्धि टीका का सहारा लिया गया है ।