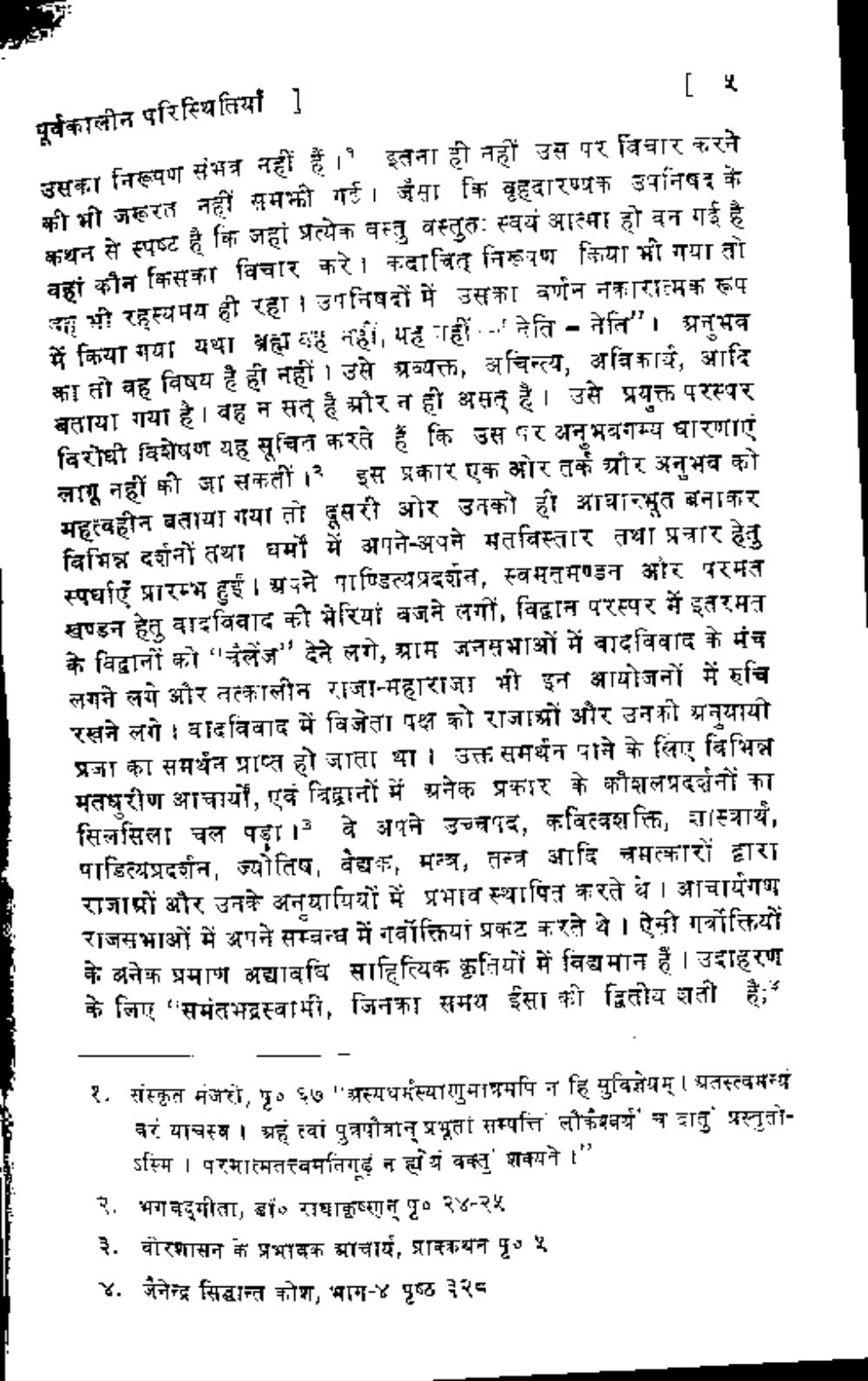________________
[ ५
पूर्वकालीन परिस्थितियां ।
निरूपण संभव नहीं हैं।' इतना ही नहीं उस पर विचार करने की जरूरत नहीं समझी गई। जमा कि वृहदारण्यक उपनिषद के
से स्पष्ट है कि जहां प्रत्येक वस्तु वस्तुतः स्वयं आत्मा हो बन गई है वो कौन किसका विचार करे। कदाचित् निरूपण किया भी गया तो डाकी रहस्यमय ही रहा । उपनिषदों में उसका वर्णन नकारात्मक रूप में किया गया यथा ब्रह्म यह नहीं यह नहीं ...' देति - नेति"। अनभव का तो वह विषय है ही नहीं। उसे अव्यक्त, अचिन्त्य, अविकार्य, आदि बताया गया है। वह न सत् है और न ही असत् है । उसे प्रयुक्त परस्पर विरोधी विशेषण यह सूचित करते हैं कि उस पर अनुभवगम्य धारणाएं लागू नहीं की जा सकती। इस प्रकार एक और तर्क पीर अनुभव को महत्वहीन बताया गया तो दूसरी ओर उनको ही आधारभूत बनाकर विभिन्न दर्शनों तथा धर्मों में अपने-अपने मतविस्तार तथा प्रचार हेतु स्पर्धाएं प्रारम्भ हई। अपने पाण्डित्यप्रदर्शन, स्वमतमण्डन और परमत खण्डन हेतु वादविवाद की भेरियां बजने लगों, विद्वान परस्पर में इतरमत के विद्वानों को 'चलेंज" देने लगे, ग्राम जनसभाओं में वादविवाद के मंच लगने लगे और तत्कालीन राजा-महाराजा भी इन आयोजनों में रुचि रखने लगे। बाद विवाद में विजेता पक्ष को राजाओं और उनको अनुयायो प्रजा का समर्थन प्राप्त हो जाता था। उक्त समर्थन पाने के लिए विभिन्न मतधुरीण आचार्यों, एवं विद्वानों में अनेक प्रकार के कौशलप्रदर्शनों का सिलसिला चल पड़ा। वे अपने उच्चपद, कवित्वशक्ति, शास्त्रार्थ, पाडित्यप्रदर्शन, ज्योतिष, बेद्यक, मन्त्र, तन्त्र आदि चमत्कारों द्वारा राजापों और उनके अनयायियों में प्रभाव स्थापित करते थे । आचार्यगण राजसभाओं में अपने सम्बन्ध में गर्वोक्तियां प्रकट करते थे। ऐनी गर्बोक्तियों के अनेक प्रमाण अद्यावधि साहित्यिक कृतियों में विद्यमान हैं । उदाहरण के लिाह "समंतभद्रस्वामी, जिनका समय ईसा की द्वितीय शती है;
१. संस्कृत मंजरों, पृ. ६७ ''अस्यधर्मस्याणुमानमपि न हि सुविज्ञेयम् । अतस्त्वमन्य
वरं याचस्व । अहं त्वां पुत्रपौत्रान् प्रभूतां सम्पत्ति लोकश्वर्य' च दातु प्रस्तुतो
ऽस्मि । परमात्मतत्त्वमतिगढ़ न ा यं वक्तु शक्यने ।" २. भगवद्गीता, डॉ० राधाकृष्णन् पृ. २४-२५ ३. वीरशासन के प्रभादक आचार्य, प्राक्कथन पृ ५ ४. जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश, भाग-४ पृष्ठ ३२८