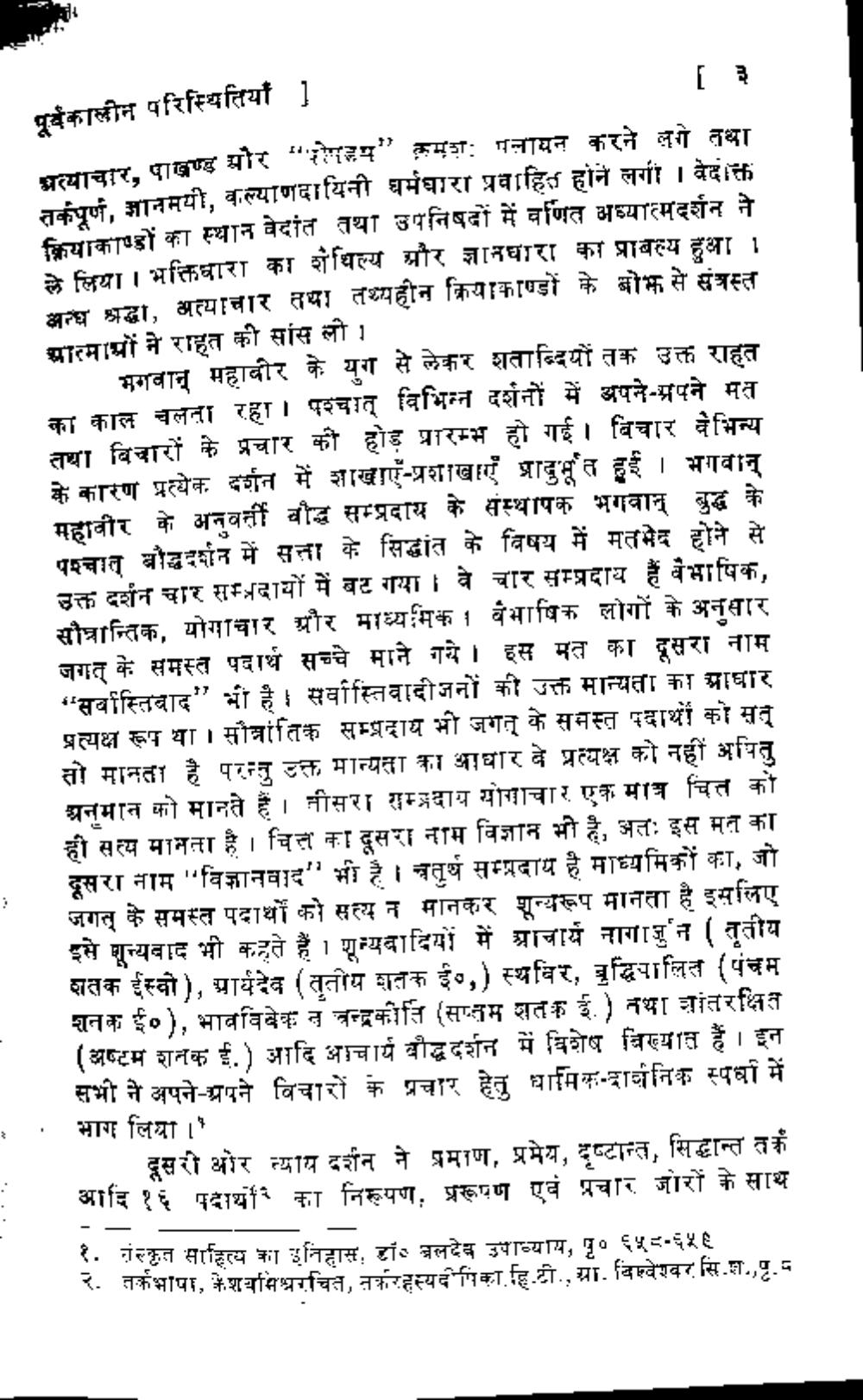________________
पूर्वकालीन परिस्थितियों ]
मार पाखण्ड और हिप" कृमश: पलायन करने लगे तथा का आनमयी, कल्याणदायिनी धर्मधारा प्रवाहित होने लगी । वेदोक्त
काण्डों का स्थान वेदांत तथा उपनिषदों में वर्णित अध्यात्मदर्शन ने ले लिया । भक्तिधारा का शैथिल्य और ज्ञानधारा का प्राबल्य हुआ ।
श्रद्धा, अत्याचार तथा तथ्यहीन क्रियाकाण्डों के बोझ से संत्रस्त आत्माओं ने राहत की सांस ली।
भगवान महावीर के युग से लेकर शताब्दियों तक उक्त राहत का काल चलता रहा। पश्चात् विभिन्न दर्शनों में अपने-अपने मत तथा विचारों के प्रचार की होड़ प्रारम्भ हो गई। बिचार भिन्य के कारण प्रत्येक दर्शन में शाखाएं-प्रशाखाएँ प्रादुर्भूत हुई । भगवान् महावीर के अनुवर्ती बौद्ध सम्प्रदाय के संस्थापक भगवान् बुद्ध के पश्चात् बौद्धदर्शन में सत्ता के सिद्धांत के विषय में मतभेद होने से उक्त दर्शन चार सम्प्रदायों में बट गया। वे चार सम्प्रदाय हैं वैभाषिक, सौत्रान्तिक, योगाचार और माध्यमिक । वैभाषिक लोगों के अनुसार जगत् के समस्त पदार्थ सच्चे माने गये। इस मत का दूसरा नाम "सर्वास्तिवाद" भी है। सर्वास्तिवादीजनों की उक्त मान्यता का आधार प्रत्यक्ष रूप था। सौत्रांतिक सम्प्रदाय भी जगत् के समस्त पदार्थों को मत तो मानता है परन्तु उक्त मान्यता का आधार वे प्रत्यक्ष को नहीं अपितु अनुमान को मानते हैं। तीसरा सम्प्रदाय योगाचार. एक मात्र चित्त को ही सत्य मानता है। चित्त का दूसरा नाम विज्ञान भी है, अतः इस मत का दूसरा नाम "विज्ञानवाद" भी है। चतुर्थ सम्प्रदाय है माध्यमिकों का, जो जगत् के समस्त पदार्थों को सत्य न मानकर शून्यरूप मानता है इसलिए इसे शून्यवाद भी कहते हैं । शून्यवादियों में प्राचार्य नागार्जुन ( तृतीय शतक ईस्वी), प्रार्यदेव (तृतीय शतक ई०,) स्थविर, बुद्धिघालित (पंचम शतक ई०), भावविवेक न चन्द्रकीति (सप्तम शतक ई.) तथा शांतरक्षित (अष्टम शतक ई.) आदि आचार्य बौद्ध दर्शन में विशेष विख्यात हैं। इन सभी ने अपने-अपने विचारों के प्रचार हेतु धामिक-दानिक स्पर्धा में भाग लिया।
. दूसरी ओर त्याय दर्शन ने प्रमाण, प्रमेय, दृष्टान्त, सिद्धान्त तक आदि १६ पदार्थों का निरूपण, प्ररूपण एवं प्रचार जोरों के साथ
१. संस्कृत साहित्य का इतिहास, डॉ बलदेव उपाध्याय, पृ० ६५८.६५६ २. तर्कभाषा, मैं शमिश्रचित, नरहस्यदपिका.हि.टी., ग्रा. विश्वेश्वर सिं.श.,पृ.८