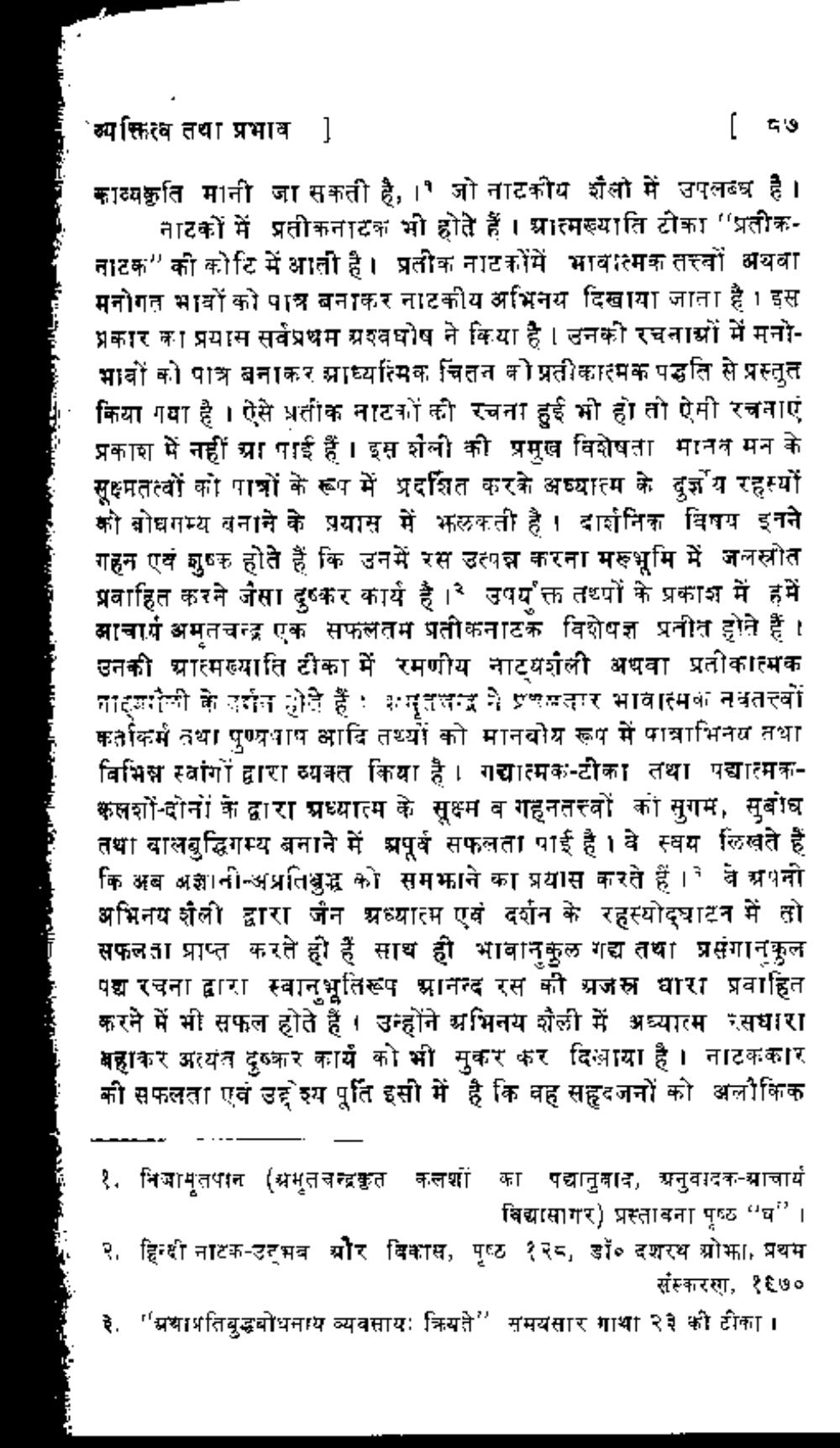________________
व्यक्तित्व तथा प्रभाव ]
[ ५७ काव्यकृति मानी जा सकती है, ।' जो नाटकीय शैलो में उपलब्ध है।
नाटकों में प्रतीकनाटक भी होते हैं। प्रात्मख्याति टोका "प्रतीकनाटक" की कोटि में आती है। प्रतीक नाटकों में भावात्मक तत्त्वों अथवा मनोगत भावों को पात्र बनाकर नाटकीय अभिनय दिखाया जाता है । इस प्रकार का प्रयास सर्वप्रथम अश्वघोष ने किया है। उनकी रचनाओं में मनोभावों को पात्र बनाकर प्राध्यत्मिक चितन प्रतीकात्मक पद्धति से प्रस्तुत किया गया है । ऐसे प्रतीक नाटकों की रचना हुई भी हो तो ऐसी रचनाएं प्रकाश में नहीं पापाई हैं। इस शैली की प्रमुख विशेषता मानव मन के सूक्ष्मतत्वों को पात्रों के रूप में प्रदर्शित करके अध्यात्म के दुय रहस्यों को बोधगम्य बनाने के प्रयास में झलकती है। दार्शनिक विषय इनने गहन एवं शुष्क होते हैं कि उनमें रस उत्पन्न करना मरूभूमि में जलस्रोत प्रवाहित करने जैसा दूष्कर कार्य हैं। उपर्य क्त तथ्यों के प्रकाश में हमें आचार्य अमृतचन्द्र एक सफलतम प्रतीकनाटक विशेषज्ञ प्रतीत होते हैं । उनकी प्रात्मख्याति टीका में रमणीय नाटयशली अथवा प्रतीकात्मक गादमागली के बनते हैं : ३. तपाद्र ने हार भावात्मवा नवतत्त्वों ककम तथा पुण्यपाप भादि तथ्यों को मानबोय रूप में पात्राभिनय तथा विभिन्न स्वांगों द्वारा व्यक्त किया है। गद्यात्मक-टीका तथा पद्यात्मकाकलशों-दोनों के द्वारा अध्यात्म के सूक्ष्म व गहनतत्वों को सुगम, सुबोध तथा बालबुद्धिगम्य बनाने में अपूर्व सफलता पाई है। वे स्वय लिखते हैं कि अब अज्ञानी अप्रतिवद्ध को समझाने का प्रयास करते हैं। वे अपनी अभिनय शैली द्वारा जैन अध्यात्म एवं दर्शन के रहस्योद्घाटन में तो सफलता प्राप्त करते ही हैं साथ ही भावानुकुल गद्य तथा प्रसंगानुकुल पञ्च रचना द्वारा स्वानुभूतिरूप प्रानन्द रस की अजस्र धारा प्रवाहित करने में भी सफल होते हैं। उन्होंने अभिनय शैली में अध्यात्म सधारा बहाकर अत्यंत दुष्कार कार्य को भी मुकर कर दिखाया है। नाटककार की सफलता एवं उद्देश्य पूर्ति इसी में है कि वह सहृदजनों को अलौकिक
१. निमामृतपान (अमृत चन्द्रकृत कलशों का पद्यानुवाद, अनुवादक-याचार्य
विद्यासागर) प्रस्तावना पृष्ठ “घ” | २. हिन्दी नाटक-उद्भव और विकास, पृष्ट १२८, डॉ० दशरथ प्रोझा, प्रथम
संस्करण, १९७० ३. 'प्रयापति बुद्धबोधनाय व्यवसायः क्रियते" समयसार गाथा २३ की टीका।