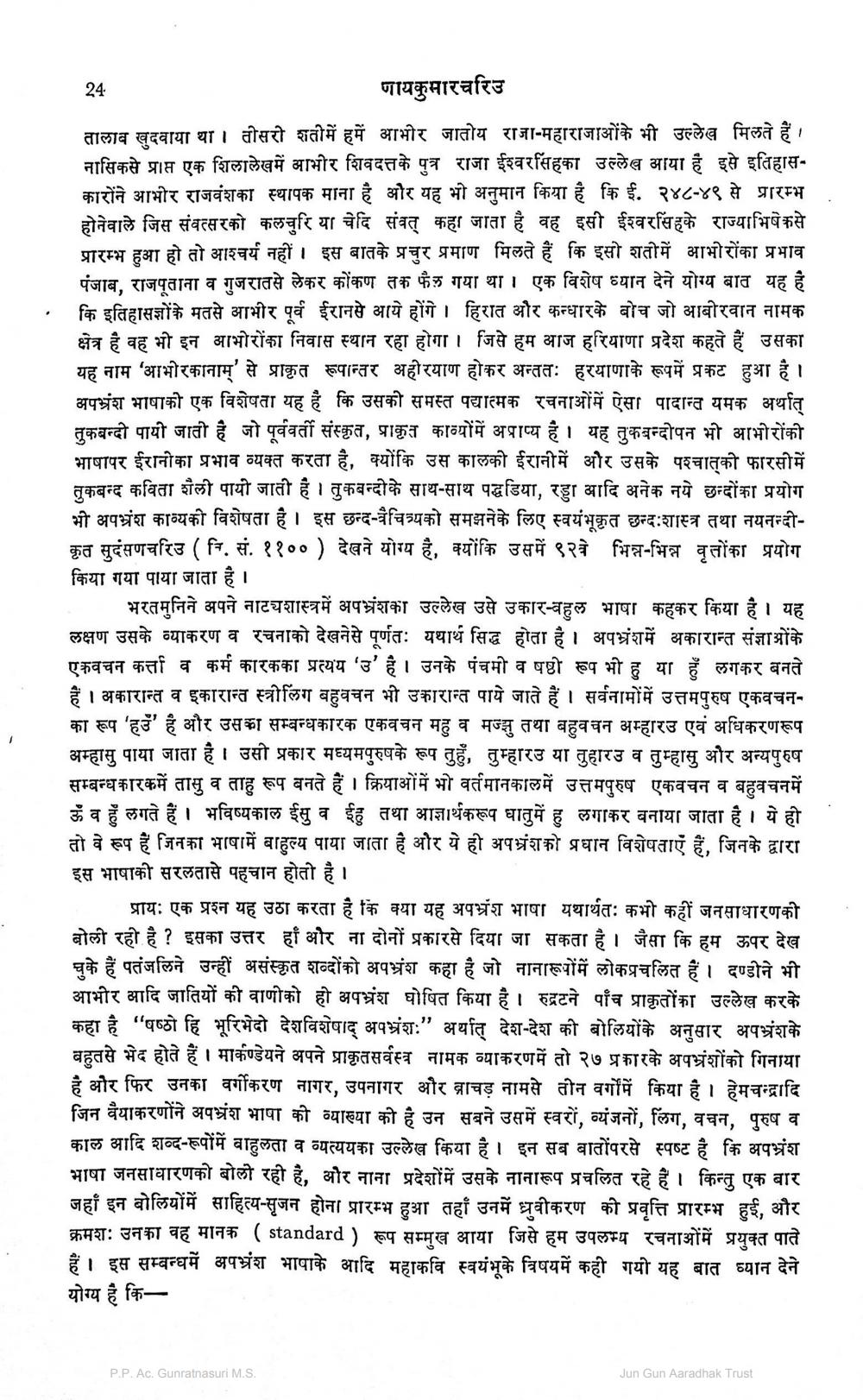________________ 24. णायकुमारचरिउ तालाब खुदवाया था। तीसरी शती में हमें आभीर जातीय राजा-महाराजाओंके भी उल्लेख मिलते हैं। नासिकसे प्राप्त एक शिलालेखमें आभीर शिवदत्तके पुत्र राजा ईश्वरसिंहका उल्लेख आया है इसे इतिहासकारोंने आभीर राजवंशका स्थापक माना है और यह भी अनुमान किया है कि ई. 248-49 से प्रारम्भ होनेवाले जिस संवत्सरको कलचुरि या चेदि संवत् कहा जाता है वह इसी ईश्वरसिंहके राज्याभिषेकसे प्रारम्भ हुआ हो तो आश्चर्य नहीं। इस बातके प्रचुर प्रमाण मिलते हैं कि इसो शती में आभीरोंका प्रभाव पंजाब, राजपूताना व गुजरातसे लेकर कोंकण तक फैल गया था। एक विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि इतिहासज्ञोंके मतसे आभीर पूर्व ईरानसे आये होंगे। हिरात और कन्धारके बोच जो आबीरवान नामक क्षेत्र है वह भी इन आभोरोंका निवास स्थान रहा होगा। जिसे हम आज हरियाणा प्रदेश कहते हैं उसका यह नाम 'आभीरकानाम्' से प्राकृत रूपान्तर अहीरयाण होकर अन्ततः हरयाणाके रूप में प्रकट हुआ है। अपभ्रंश भाषाको एक विशेषता यह है कि उसको समस्त पद्यात्मक रचनाओंमें ऐसा पादान्त यमक अर्थात् तुकबन्दी पायी जाती है जो पूर्ववर्ती संस्कृत, प्राकृत काव्योंमें अप्राप्य है। यह तुकबन्दीपन भी आभोरोंको भाषापर ईरानीका प्रभाव व्यक्त करता है, क्योंकि उस कालको ईरानीमें और उसके पश्चात्को फारसीमें तकबन्द कविता शैली पायी जाती है। तुकबन्दीके साथ-साथ पद्धडिया, रडा आदि अनेक नये छन्दोंका प्रयोग भी अपभ्रंश काव्यको विशेषता है। इस छन्द-वैचित्र्यको समझने के लिए स्वयंभूकृत छन्दःशास्त्र तथा नयनन्दीकृत सुदंसणचरिउ (नि. सं. 1100 ) देखने योग्य है, क्योंकि उसमें ९२वे भिन्न-भिन्न वृतोंका प्रयोग किया गया पाया जाता है। भरतमुनिने अपने नाट्यशास्त्रमें अपभ्रंशका उल्लेख उसे उकार-बहुल भाषा कहकर किया है। यह लक्षण उसके व्याकरण व रचनाको देखने से पूर्णतः यथार्थ सिद्ध होता है। अपभ्रंशमें अकारान्त संज्ञाओंके एकवचन कर्ता व कर्म कारकका प्रत्यय 'उ' है। उनके पंचमी व षष्ठी रूप भी हु या हुँ लगकर बनते हैं / अकारान्त व इकारान्त स्त्रीलिंग बहुवचन भी उकारान्त पाये जाते हैं / सर्वनामों में उत्तमपुरुष एकवचनका रूप 'हउँ' है और उसका सम्बन्धकारक एकवचन महु व मज्झु तथा बहुवचन अम्हारउ एवं अधिकरणरूप अम्हासु पाया जाता है। उसी प्रकार मध्यमपुरुषके रूप तुहुँ, तुम्हारउ या तुहारउ व तुम्हासु और अन्यपुरुष सम्बन्धकारकमें तासु व ताहु रूप बनते हैं / क्रियाओंमें भो वर्तमानकाल में उत्तमपुरुष एकवचन व बहुवचनमें तो वे रूप हैं जिनका भाषामें बाहुल्य पाया जाता है और ये ही अपभ्रंशको प्रधान विशेषताएं हैं, जिनके द्वारा इस भाषाकी सरलतासे पहचान होती है / प्रायः एक प्रश्न यह उठा करता है कि क्या यह अपभ्रंश भाषा यथार्थतः कभी कहीं जनसाधारणको बोली रही है ? इसका उत्तर हाँ और ना दोनों प्रकारसे दिया जा सकता है। जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं पतंजलिने उन्हीं असंस्कृत शब्दोंको अपभ्रंश कहा है जो नानारूपोंमें लोकप्रचलित हैं। दण्डीने भी आभीर आदि जातियों की वाणीको हो अपभ्रंश घोषित किया है। रुद्रटने पाँच प्राकृतोंका उल्लेख करके कहा है “षष्ठो हि भूरिभेदो देशविशेषाद् अपभ्रंशः" अर्थात् देश-देश की बोलियोंके अनुसार अपभ्रंशके बहुतसे भेद होते हैं / मार्कण्डेयने अपने प्राकृतसर्वस्त्र नामक व्याकरणमें तो 27 प्रकारके अपभ्रंशोंको गिनाया है और फिर उनका वर्गीकरण नागर, उपनागर और ब्राचड़ नामसे तीन वर्गों में किया है / हेमचन्द्रादि जिन वैयाकरणोंने अपभ्रंश भाषा की व्याख्या को है उन सबने उसमें स्वरों, व्यंजनों, लिंग, वचन, पुरुष व काल आदि शब्द-रूपोंमें बाहुलता व व्यत्ययका उल्लेख किया है। इन सब बातोंपरसे स्पष्ट है कि अपभ्रंश भाषा जनसाधारणको बोलो रही है, और नाना प्रदेशों में उसके नानारूप प्रचलित रहे हैं। किन्तु एक बार जहाँ इन बोलियोंमें साहित्य-सृजन होना प्रारम्भ हुआ तहाँ उनमें ध्रुवीकरण की प्रवृत्ति प्रारम्भ हुई, और क्रमशः उनका वह मानक ( standard ) रूप सम्मुख आया जिसे हम उपलभ्य रचनाओं में प्रयुक्त पाते हैं। इस सम्बन्धमें अपभ्रंश भाषाके आदि महाकवि स्वयंभूके विषयमें कही गयी यह बात ध्यान देने योग्य है कि P.P.AC.Gunratnasuri M.S. Jun Gun Aaradhak Trust