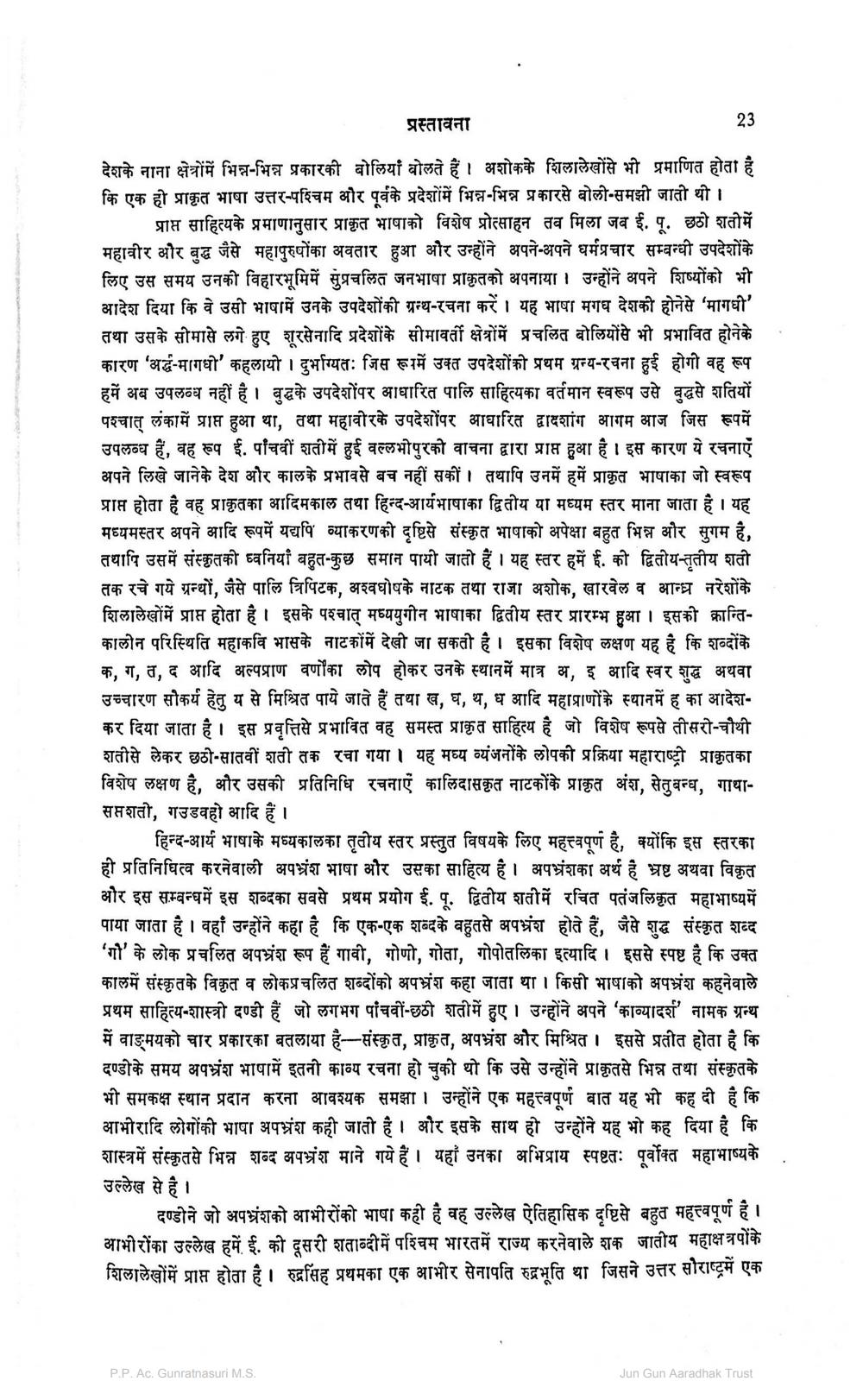________________ प्रस्तावना देशके नाना क्षेत्रोंमें भिन्न-भिन्न प्रकारकी बोलियां बोलते हैं। अशोकके शिलालेखोंसे भी प्रमाणित होता है कि एक ही प्राकृत भाषा उत्तर-पश्चिम और पूर्वके प्रदेशोंमें भिन्न-भिन्न प्रकारसे बोली-समझी जाती थी। प्राप्त साहित्यके प्रमाणानुसार प्राकृत भाषाको विशेष प्रोत्साहन तब मिला जब ई. पू. छठी शतीमें महावीर और बुद्ध जैसे महापुरुषोंका अवतार हुआ और उन्होंने अपने-अपने धर्मप्रचार सम्बन्धी उपदेशोंके लिए उस समय उनकी विहारभूमिमें सुप्रचलित जनभाषा प्राकृतको अपनाया। उन्होंने अपने शिष्योंको भी आदेश दिया कि वे उसी भाषामें उनके उपदेशोंकी ग्रन्थ-रचना करें। यह भाषा मगध देशकी होनेसे 'मागधी' तथा उसके सीमासे लगे हुए सेनादि प्रदेशोंके सीमावर्ती क्षेत्रोंमें प्रचलित बोलियोंसे भी प्रभावित होनेके कारण 'अर्द्ध-मागधो' कहलायो / दुर्भाग्यतः जिस रूपमें उक्त उपदेशोंको प्रथम ग्रन्य-रचना हुई होगी वह रूप हमें अब उपलब्ध नहीं है / बुद्धके उपदेशोंपर आधारित पालि साहित्यका वर्तमान स्वरूप उसे बुद्धसे शतियों पश्चात लंकामें प्राप्त हआ था, तथा महावीरके उपदेशोंपर आधारित द्वादशांग आगम आज जिस रूपमें उपलब्ध हैं, वह रूप ई. पांचवीं शतीमें हुई वल्लभीपुरको वाचना द्वारा प्राप्त हुआ है / इस कारण ये रचनाएं अपने लिखे जानेके देश और कालके प्रभावसे बच नहीं सकी। तथापि उनमें हमें प्राकृत भाषाका जो स्वरूप प्राप्त होता है वह प्राकृतका आदिमकाल तथा हिन्द-आर्यभाषाका द्वितीय या मध्यम स्तर माना जाता है / यह मध्यमस्तर अपने आदि रूपमें यद्यपि व्याकरणको दष्टिसे संस्कृत भाषाको अपेक्षा बहत भिन्न और सुगम है. तथापि उसमें संस्कृतको ध्वनियां बहुत-कुछ समान पायी जाती हैं / यह स्तर हमें ई. को द्वितीय-तृतीय शती तक रचे गये ग्रन्थों, जैसे पालि त्रिपिटक, अश्वघोषके नाटक तथा राजा अशोक, खारवेल व आन्ध्र नरेशोंके शिलालेखोंमें प्राप्त होता है। इसके पश्चात् मध्ययुगीन भाषाका द्वितीय स्तर प्रारम्भ हआ। इसकी क्रान्तिकालीन परिस्थिति महाकवि भासके नाटकोंमें देखी जा सकती है। इसका विशेष लक्षण यह है कि शब्दोंके क, ग, त, द आदि अल्पप्राण वोका लोप होकर उनके स्थान में मात्र अ, इ आदि स्वर शुद्ध अथवा उच्चारण सौकर्य हेतु य से मिश्रित पाये जाते हैं तथा ख, घ, थ, ध आदि महाप्राणों के स्थानमें ह का आदेशकर दिया जाता है। इस प्रवृत्तिसे प्रभावित वह समस्त प्राकृत साहित्य है जो विशेष रूपसे तीसरी-चौथी शतीसे लेकर छठी-सातवीं शती तक रचा गया। यह मध्य व्यंजनोंके लोपकी प्रक्रिया महाराष्ट्रो प्राकृतका विशेष लक्षण है, और उसको प्रतिनिधि रचनाएं कालिदासकृत नाटकोंके प्राकृत अंश, सेतुबन्ध, गाथासप्तशती, गउडवहो आदि हैं / हिन्द-आर्य भाषाके मध्यकालका तृतीय स्तर प्रस्तुत विषयके लिए महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इस स्तरका ही प्रतिनिधित्व करनेवाली अपभ्रंश भाषा और उसका साहित्य है। अपभ्रंशका अर्थ है भ्रष्ट अथवा विकृत और इस सम्बन्धमें इस शब्दका सबसे प्रथम प्रयोग ई. पू. द्वितीय शतीमें रचित पतंजलिकृत महाभाष्यमें पाया जाता है / वहां उन्होंने कहा है कि एक-एक शब्दके बहुतसे अपभ्रंश होते हैं, जैसे शुद्ध संस्कृत शब्द 'गो' के लोक प्रचलित अपभ्रंश रूप हैं गावी, गोणो, गोता, गोपोतलिका इत्यादि / इससे स्पष्ट है कि उक्त कालमें संस्कृत के विकृत व लोकप्रचलित शब्दोंको अपभ्रंश कहा जाता था। किसी भाषाको अपभ्रंश कहनेवाले प्रथम साहित्य-शास्त्री दण्डी हैं जो लगभग पांचवीं-छठी शतीमें हुए। उन्होंने अपने 'काव्यादर्श' नामक ग्रन्थ में वाङ्मयको चार प्रकारका बतलाया है-संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और मिश्रित / इससे प्रतीत होता है कि दण्डोके समय अपभ्रंश भाषामें इतनी काव्य रचना हो चुकी थी कि उसे उन्होंने प्राकृतसे भिन्न तथा संस्कृतके भी समकक्ष स्थान प्रदान करना आवश्यक समझ समझा। उन्होंने एक महत्त्वपूर्ण बात यह भी कह दी है कि आभीरादि लोगोंकी भाषा अपभ्रंश कही जाती है / और इसके साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया है कि शास्त्रमें संस्कृतसे भिन्न शब्द अपभ्रंश माने गये हैं। यहां उनका अभिप्राय स्पष्टतः पूर्वोक्त महाभाष्यके उल्लेख से है। ___ दण्डोने जो अपभ्रंशको आभीरोंको भाषा कही है वह उल्लेख ऐतिहासिक दृष्टिसे बहुत महत्त्वपूर्ण है। आभीरोंका उल्लेख हमें ई. की दूसरी शताब्दी में पश्चिम भारतमें राज्य करनेवाले शक जातीय महाक्षत्रपोंके शिलालेखोंमें प्राप्त होता है। रुद्रसिंह प्रथमका एक आभीर सेनापति रुद्रभूति था जिसने उत्तर सौराष्ट्रमें एक P.P. Ac. Gunratnasuri M.S. Jun Gun Aaradhak Trust