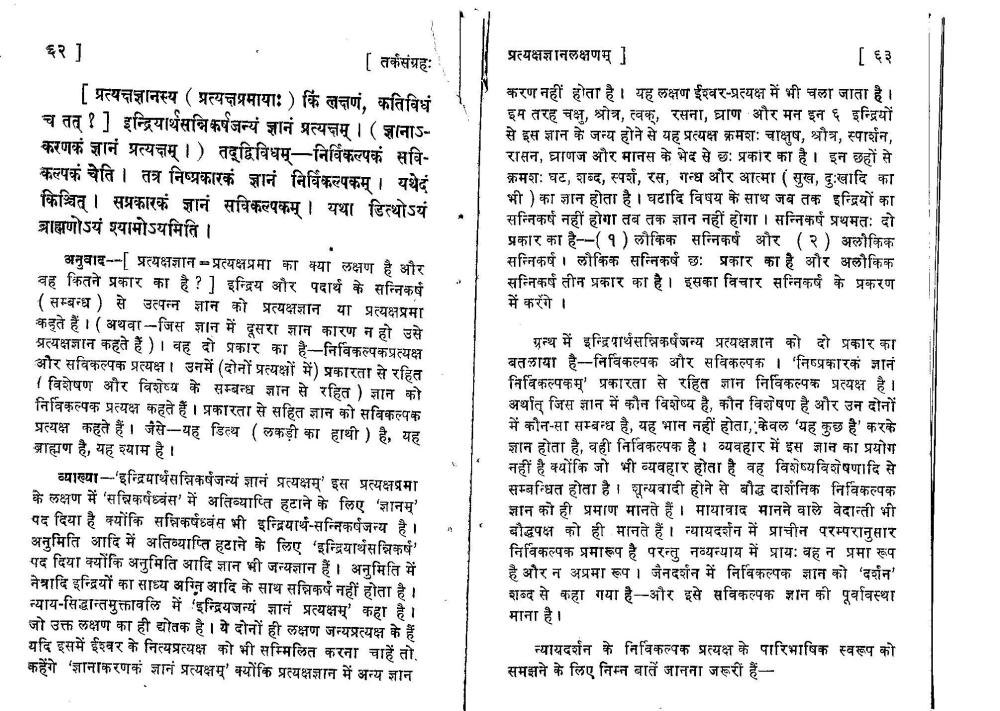________________ 62 ] [ तर्कसंग्रहः प्रत्यक्षज्ञानलक्षणम् ] [ 63 करण नहीं होता है। यह लक्षण ईश्वर-प्रत्यक्ष में भी चला जाता है। इम तरह चक्षु, श्रोत्र, त्वक्, रसना, घ्राण और मन इन 6 इन्द्रियों से इस ज्ञान के जन्य होने से यह प्रत्यक्ष क्रमशः चाक्षुष, श्रीत्र, स्पार्शन, रासन, घ्राणज और मानस के भेद से छः प्रकार का है। इन छहों से क्रमशः घट, शब्द, स्पर्श, रस, गन्ध और आत्मा ( सुख, दुःखादि का भी ) का ज्ञान होता है / घटादि विषय के साथ जब तक इन्द्रियों का सन्निकर्ष नहीं होगा तब तक ज्ञान नहीं होगा / सन्निकर्ष प्रथमतः दो प्रकार का है--(१) लौकिक सन्निकर्ष और (2) अलौकिक सन्निकर्ष / लौकिक सन्निकर्ष छ: प्रकार का है और अलौकिक सन्निकर्ष तीन प्रकार का है। इसका विचार सन्निकर्ष के प्रकरण में करेंगे। . सन्निकर्ष [प्रत्यक्षज्ञानस्य (प्रत्यक्षप्रमायाः) किं लक्षणं, कतिविधं च तत् ? ] इन्द्रियार्थसन्निकर्षजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम् / (ज्ञानाकरणकं ज्ञानं प्रत्यक्षम् / ) तद्विविधम्-निर्विकल्पकं सविकल्पकं चेति / तत्र निष्प्रकारकं ज्ञानं निर्विकल्पकम् / यथेदं किञ्चित् / सप्रकारकं ज्ञानं सविकल्पकम् / यथा डित्थोऽयं ब्राह्मणोऽयं श्यामोऽयमिति / अनुवाद--[ प्रत्यक्षज्ञान प्रत्यक्षप्रमा का क्या लक्षण है और वह कितने प्रकार का है? ] इन्द्रिय और पदार्थ के सन्निकर्ष (सम्बन्ध) से उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्षज्ञान या प्रत्यक्षप्रमा कहते हैं / ( अथवा-जिस ज्ञान में दूसरा ज्ञान कारण न हो उसे प्रत्यक्षज्ञान कहते हैं)। वह दो प्रकार का है-निर्विकल्पकप्रत्यक्ष और सविकल्पक प्रत्यक्ष। उनमें (दोनों प्रत्यक्षों में) प्रकारता से रहित (विशेषण और विशेष्य के सम्बन्ध ज्ञान से रहित) ज्ञान को निर्विकल्पक प्रत्यक्ष कहते हैं / प्रकारता से सहित ज्ञान को सविकल्पक प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे-यह डित्य (लकड़ी का हाथी) है, यह ब्राह्मण है, यह श्याम है। व्याख्या-'इन्द्रियार्थसन्निकर्षजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम्' इस प्रत्यक्षप्रमा के लक्षण में 'सन्निकर्षध्वंस' में अतिव्याप्ति हटाने के लिए 'ज्ञानम्' पद दिया है क्योंकि सन्निकर्षध्वंस भी इन्द्रियार्थ-सन्निकर्षजन्य है। अनुमिति आदि में अतिव्याप्ति हटाने के लिए 'इन्द्रियार्थसन्निकर्ष' पद दिया क्योंकि अनुमिति आदि ज्ञान भी जन्यज्ञान हैं। अनुमिति में नेत्रादि इन्द्रियों का साध्य अग्नि आदि के साथ सन्निकर्ष नहीं होता है। न्याय-सिद्धान्तमुक्तावलि में 'इन्द्रियजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम्' कहा है। जो उक्त लक्षण का ही द्योतक है। ये दोनों ही लक्षण जन्यप्रत्यक्ष के हैं यदि इसमें ईश्वर के नित्यप्रत्यक्ष को भी सम्मिलित करना चाहें तो, कहेंगे 'ज्ञानाकरणकं ज्ञानं प्रत्यक्षम्' क्योंकि प्रत्यक्षज्ञान में अन्य ज्ञान ग्रन्थ में इन्द्रिपार्थसन्निकर्षजन्य प्रत्यक्षज्ञान को दो प्रकार का बतलाया है-निर्विकल्पक और सविकल्पक / 'निष्प्रकारकं ज्ञानं निर्विकल्पकम्' प्रकारता से रहित ज्ञान निर्विकल्पक प्रत्यक्ष है। अर्थात् जिस ज्ञान में कौन विशेष्य है, कौन विशेषण है और उन दोनों में कौन-सा सम्बन्ध है, यह भान नहीं होता, केवल 'यह कूछ है' करके ज्ञान होता है, वही निर्विकल्पक है। व्यवहार में इस ज्ञान का प्रयोग नहीं है क्योंकि जो भी व्यवहार होता है वह विशेष्यविशेषणादि से सम्बन्धित होता है। शून्यवादी होने से बौद्ध दार्शनिक निर्विकल्पक ज्ञान को ही प्रमाण मानते हैं। मायावाद मानने वाले वेदान्ती भी बौद्धपक्ष को ही मानते हैं। न्यायदर्शन में प्राचीन परम्परानुसार निर्विकल्पक प्रमारूप है परन्तु नव्यन्याय में प्रायः वह न प्रमा रूप है और न अप्रमा रूप। जैनदर्शन में निर्विकल्पक ज्ञान को 'दर्शन' शब्द से कहा गया है और इसे सविकल्पक ज्ञान की पूर्वावस्था माना है। न्यायदर्शन के निर्विकल्पक प्रत्यक्ष के पारिभाषिक स्वरूप को समझने के लिए निम्न बातें जानना जरूरी हैं