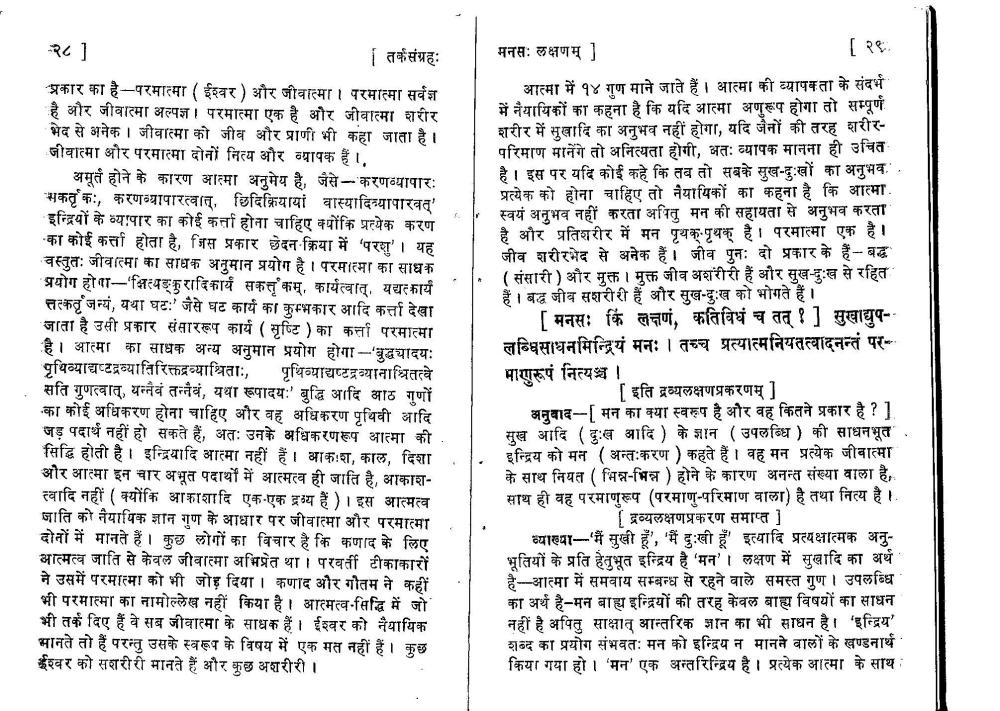________________ 28 ] / तर्कसंग्रहः प्रकार का है-परमात्मा ( ईश्वर ) और जीवात्मा। परमात्मा सर्वज्ञ है और जीवात्मा अल्पज्ञ। परमात्मा एक है और जीवात्मा शरीर भेद से अनेक / जीवात्मा को जीव और प्राणी भी कहा जाता है। जीवात्मा और परमात्मा दोनों नित्य और व्यापक हैं।, ___ अमूर्त होने के कारण आत्मा अनुमेय है, जैसे--करणब्यापारः मकर्तृकः, करणब्यापारत्वात्, छिदिक्रियायां वास्यादिव्यापारवत्' / इन्द्रियों के व्यापार का कोई कर्ता होना चाहिए क्योंकि प्रत्येक करण का कोई कर्ता होता है, जिस प्रकार छेदन क्रिया में 'परशु'। यह वस्तुत: जीवात्मा का साधक अनुमान प्रयोग है / परमात्मा का साधक प्रयोग होगा-'क्षित्यकुरादिकार्य सकत्तू कम्, कार्यत्वात्, यद्यत्कार्य तत्कर्तृ जन्यं, यथा घट:' जैसे घट कार्य का कुम्भकार आदि कर्ता देखा जाता है उसी प्रकार संसाररूप कार्य (सष्टि ) का कर्ता परमात्मा है। आत्मा का साधक अन्य अनुमान प्रयोग होगा-'बुद्धधादयः पृथिव्याद्यष्टद्रव्यातिरिक्तद्रव्याश्रिताः, पृथिव्याद्यष्टद्रव्यानाश्रितत्वे सति गुणत्वात्, यन्नैवं तन्नैवं, यथा रूपादयः' बुद्धि आदि आठ गुणों का कोई अधिकरण होना चाहिए और वह अधिकरण पृथिवी आदि जड़ पदार्थ नहीं हो सकते हैं, अतः उनके अधिकरणरूप आत्मा की सिद्धि होती है। इन्द्रियादि आत्मा नहीं हैं। आकाश, काल, दिशा और आत्मा इन चार अभूत पदार्थों में आत्मत्व ही जाति है, आकाशस्वादि नहीं ( क्योंकि आकाशादि एक-एक द्रव्य हैं)। इस आत्मत्व जाति को नैयायिक ज्ञान गण के आधार पर जीवात्मा और परमात्मा दोनों में मानते हैं। कुछ लोगों का विचार है कि कणाद के लिए आत्मत्व जाति से केवल जीवात्मा अभिप्रेत था। परवर्ती टीकाकारों ने उसमें परमात्मा को भी जोड़ दिया। कणाद और गौतम ने कहीं भी परमात्मा का नामोल्लेख नहीं किया है। आत्मत्व-सिद्धि में जो भी तर्क दिए हैं वे सब जीवात्मा के साधक हैं। ईश्वर को नैयायिक मानते तो हैं परन्तु उसके स्वरूप के विषय में एक मत नहीं हैं। कुछ ईश्वर को सशरीरी मानते हैं और कुछ अशरीरी। मनसः लक्षणम् ] [29 आत्मा में 14 गुण माने जाते हैं। आत्मा की व्यापकता के संदर्भ में नैयायिकों का कहना है कि यदि आत्मा अणुरूप होगा तो सम्पूर्ण शरीर में सुखादि का अनुभव नहीं होगा, यदि जैनों की तरह शरीरपरिमाण मानेंगे तो अनित्यता होगी, अतः व्यापक मानना ही उचित है। इस पर यदि कोई कहे कि तब तो सबके सुख-दुःखों का अनुभव' . प्रत्येक को होना चाहिए तो नैयायिकों का कहना है कि आत्मा स्वयं अनुभव नहीं करता अपितु मन की सहायता से अनुभव करता है और प्रतिशरीर में मन पृथक्-पृथक् है। परमात्मा एक है। जीव शरीरभेद से अनेक हैं। जीव पुनः दो प्रकार के हैं--बद्ध ( संसारी) और मुक्त / मुक्त जीव अशरीरी हैं और सुख-दुःख से रहित हैं / बद्ध जीव सशरीरी हैं और सुख-दुःख को भोगते हैं। [मनसः किं लक्षणं, कतिविधं च तत् ] सुखाद्युप-- लब्धिसाधनमिन्द्रियं मनः। तच्च प्रत्यात्मनियतत्वादनन्तं परभाणुरूपं नित्यश्च / [इति द्रव्यलक्षणप्रकरणम् ] अनुवाद-[ मन का क्या स्वरूप है और वह कितने प्रकार है ? 1 सुख आदि (दु:ख आदि) के ज्ञान (उपलब्धि ) की साधनभूत . इन्द्रिय को मन (अन्तःकरण) कहते हैं। वह मन प्रत्येक जीवात्मा के साथ नियत ( भिन्न-भिन्न ) होने के कारण अनन्त संख्या वाला है, साथ ही वह परमाणुरूप (परमाणु-परिमाण वाला) है तथा नित्य है। द्रव्यलक्षणप्रकरण समाप्त] व्याख्या-'मैं सुखी हूँ', 'मैं दु:खी हूँ' इत्यादि प्रत्यक्षात्मक अनुभूतियों के प्रति हेतुभूत इन्द्रिय है 'मन' / लक्षण में सुखादि का अर्थ है-आत्मा में समवाय सम्बन्ध से रहने वाले समस्त गुण / उपलब्धि का अर्थ है-मन बाह्य इन्द्रियों की तरह केवल बाह्य विषयों का साधन नहीं है अपितु साक्षात् आन्तरिक ज्ञान का भी साधन है। 'इन्द्रिय' शब्द का प्रयोग संभवतः मन को इन्द्रिय न मानने वालों के खण्डनार्थ किया गया हो / 'मन' एक अन्तरिन्द्रिय है। प्रत्येक आत्मा के साथ का.