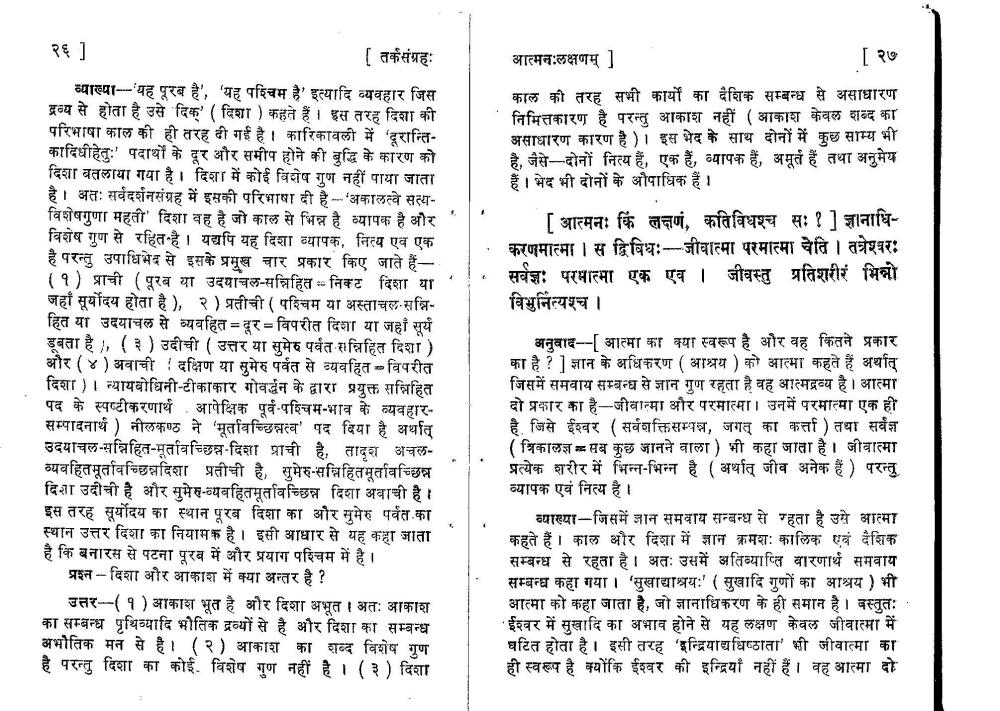________________ 26 ] [ तर्कसंग्रहः आत्मनःलक्षणम् ] [27 काल की तरह सभी कार्यों का दैशिक सम्बन्ध से असाधारण निमित्तकारण है परन्तु आकाश नहीं (आकाश केवल शब्द का असाधारण कारण है)। इस भेद के साथ दोनों में कुछ साम्य भी है, जैसे-दोनों नित्य हैं, एक हैं, व्यापक हैं, अमूर्त हैं तथा अनुमेय हैं। भेद भी दोनों के औपाधिक हैं। [आत्मनः किं लक्षणं, कतिविधश्च सः ? ] ज्ञानाधि- करणमात्मा / स द्विविधः-जीवात्मा परमात्मा चेति / तत्रेश्वरः सर्वज्ञः परमात्मा एक एव / जीवस्तु प्रतिशरीरं भिन्नो विभुनित्यश्च / व्याख्या-'यह पूरब है', 'यह पश्चिम है' इत्यादि व्यवहार जिस द्रव्य से होता है उसे दिक्' (दिशा) कहते हैं। इस तरह दिशा की परिभाषा काल की ही तरह दी गई है। कारिकावली में 'दूरान्तिकादिधीहेतु:' पदार्थों के दूर और समीप होने की बुद्धि के कारण को दिशा बतलाया गया है। दिशा में कोई विशेष गुण नहीं पाया जाता है। अतः सर्वदर्शनसंग्रह में इसकी परिभाषा दी है .... 'अकालस्वे सत्यविशेषगुणा महती' दिशा वह है जो काल से भिन्न है व्यापक है और " विशेष गुण से रहित है। यद्यपि यह दिशा व्यापक, नित्य एव एक है परन्तु उपाधिभेद से इसके प्रमुख चार प्रकार किए जाते हैं(१) प्राची (पूरब या उदयाचल-सन्निहित निक्ट दिशा या जहाँ सूर्योदय होता है), 2) प्रतीची ( पश्चिम या अस्ताचल-सन्निहित या उदयाचल से व्यवहित = दुर = विपरीत दिशा या जहाँ सूर्य डूबता है, (3) उदीची ( उत्तर या सुमेरु पर्वत सन्निहित दिशा) और (4) अवाची ! दक्षिण या सुमेरु पर्वत से व्यवहित विपरीत दिशा ) / न्यायबोधिनी-टीकाकार गोवर्द्धन के द्वारा प्रयुक्त सन्निहित पद के स्पष्टीकरणार्थ , आपेक्षिक पूर्व-पश्चिम-भाव के व्यवहारसम्पादनार्थ) नीलकण्ठ ने 'मूर्तावच्छिन्नत्व' पद दिया है अर्थात् उदयाचल-सन्निहित-मूर्तावच्छिन्न-दिशा प्राची है, तादृश अचलव्यवहितमूर्तावच्छिन्नदिशा प्रतीची है, सुमेरु-सन्निहितमूर्तावच्छिन्न दिशा उदीची है और सुमेस-व्यवहितमूर्तावच्छिन्न दिशा अवाली है। इस तरह सूर्योदय का स्थान पूरब दिशा का और सुमेरु पर्वत का . स्थान उत्तर दिशा का नियामक है। इसी आधार से यह कहा जाता है कि बनारस से पटना पूरब में और प्रयाग पश्चिम में है। प्रश्न-दिशा और आकाश में क्या अन्तर है ? उत्तर-(१) आकाश भूत है और दिशा अभूत / अतः आकाश का सम्बन्ध पृथिव्यादि भौतिक द्रव्यों से है और दिशा का सम्बन्ध अभौतिक मन से है। (2) आकाश का शब्द विशेष गुण है परन्तु दिशा का कोई. विशेष गुण नहीं है / (3) दिशा अनुवाद-[ आत्मा का क्या स्वरूप है और वह कितने प्रकार का है ? ] ज्ञान के अधिकरण (आश्रय ) को आत्मा कहते हैं अर्थात् जिसमें समवाय सम्बन्ध से ज्ञान गुण रहता है वह आत्मद्रव्य है। आत्मा दो प्रकार का है-जीवात्मा और परमात्मा। उनमें परमात्मा एक ही है. जिसे ईश्वर (सर्वशक्ति सम्पन्न, जगत् का कर्ता) तथा सर्वज्ञ (त्रिकालज्ञ सब कुछ जानने वाला) भी कहा जाता है। जीवात्मा प्रत्येक शरीर में भिन्न-भिन्न है ( अर्थात् जीव अनेक हैं) परन्तु व्यापक एवं नित्य है। व्याख्या-जिसमें ज्ञान समवाय सम्बन्ध से रहता है उसे आत्मा कहते हैं। काल और दिशा में ज्ञान क्रमशः कालिक एवं दैशिक सम्बन्ध से रहता है। अतः उसमें अतिव्याप्ति वारणार्थ समवाय सम्बन्ध कहा गया। 'सुखाद्याश्रयः' (सुखादि गुणों का आश्रय ) भी आत्मा को कहा जाता है, जो ज्ञानाधिकरण के ही समान है। वस्तुतः / ईश्वर में सुखादि का अभाव होने से यह लक्षण केवल जीवात्मा में घटित होता है। इसी तरह 'इन्द्रियाद्यधिष्ठाता' भी जीवात्मा का ही स्वरूप है क्योंकि ईश्वर की इन्द्रियाँ नहीं हैं। वह आत्मा दो /