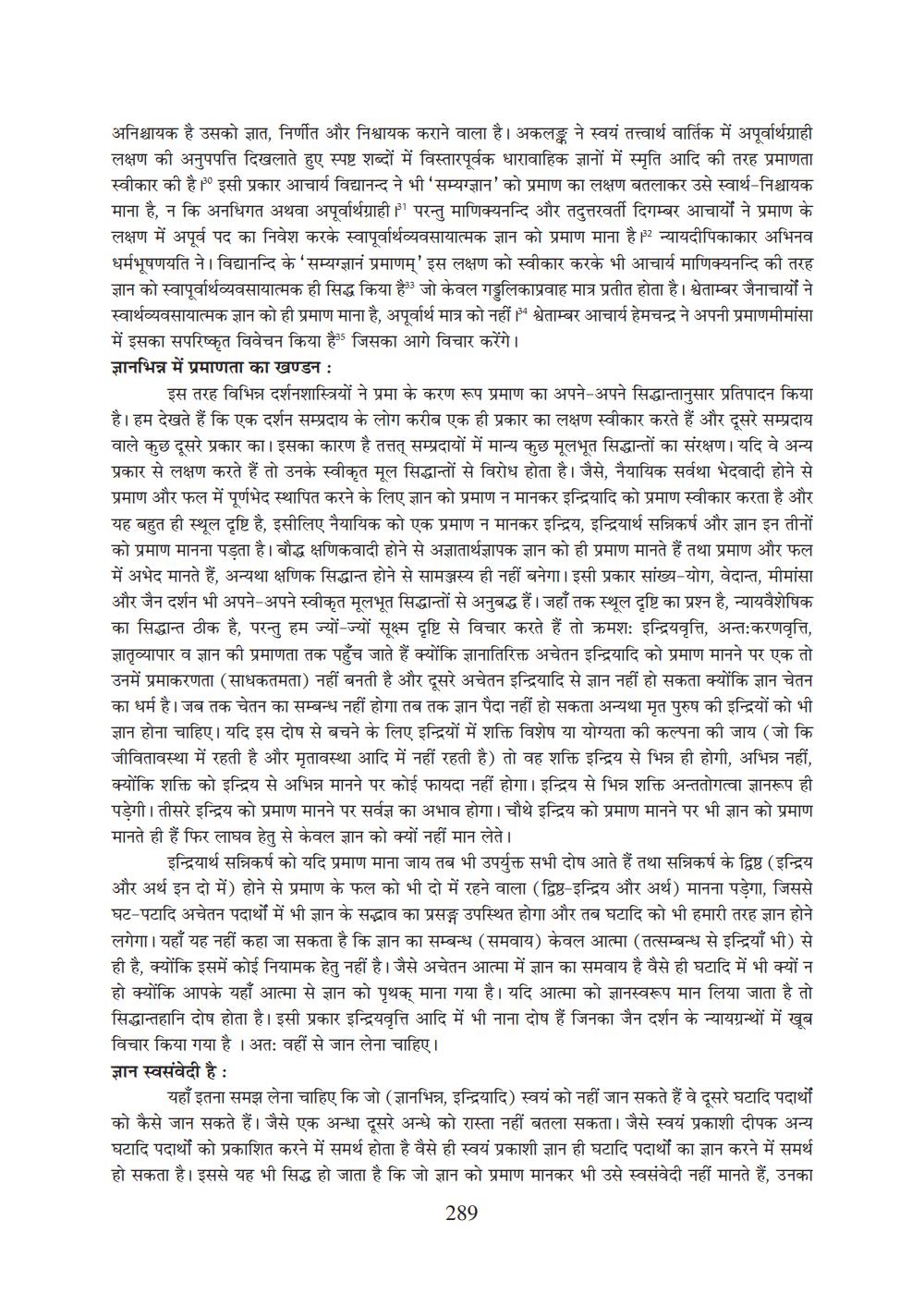________________ अनिश्चायक है उसको ज्ञात, निर्णीत और निश्वायक कराने वाला है। अकलङ्क ने स्वयं तत्त्वार्थ वार्तिक में अपूर्वार्थग्राही लक्षण की अनुपपत्ति दिखलाते हुए स्पष्ट शब्दों में विस्तारपूर्वक धारावाहिक ज्ञानों में स्मृति आदि की तरह प्रमाणता स्वीकार की है। इसी प्रकार आचार्य विद्यानन्द ने भी 'सम्यग्ज्ञान' को प्रमाण का लक्षण बतलाकर उसे स्वार्थ-निश्चायक माना है, न कि अनधिगत अथवा अपूर्वार्थग्राही। परन्तु माणिक्यनन्दि और तदुत्तरवर्ती दिगम्बर आचार्यों ने प्रमाण के लक्षण में अपूर्व पद का निवेश करके स्वापूर्वार्थव्यवसायात्मक ज्ञान को प्रमाण माना है। न्यायदीपिकाकार अभिनव धर्मभूषणयति ने। विद्यानन्दि के 'सम्यग्ज्ञानं प्रमाणम्' इस लक्षण को स्वीकार करके भी आचार्य माणिक्यनन्दि की तरह ज्ञान को स्वापूर्वार्थव्यवसायात्मक ही सिद्ध किया है जो केवल गडलिकाप्रवाह मात्र प्रतीत होता है। श्वेताम्बर जैनाचार्यों ने स्वार्थव्यवसायात्मक ज्ञान को ही प्रमाण माना है, अपूर्वार्थ मात्र को नहीं। श्वेताम्बर आचार्य हेमचन्द्र ने अपनी प्रमाणमीमांसा में इसका सपरिष्कृत विवेचन किया है जिसका आगे विचार करेंगे। ज्ञानभिन्न में प्रमाणता का खण्डन : __इस तरह विभिन्न दर्शनशास्त्रियों ने प्रमा के करण रूप प्रमाण का अपने-अपने सिद्धान्तानुसार प्रतिपादन किया है। हम देखते हैं कि एक दर्शन सम्प्रदाय के लोग करीब एक ही प्रकार का लक्षण स्वीकार करते हैं और दूसरे सम्प्रदाय वाले कुछ दूसरे प्रकार का। इसका कारण है तत्तत् सम्प्रदायों में मान्य कुछ मूलभूत सिद्धान्तों का संरक्षण। यदि वे अन्य प्रकार से लक्षण करते हैं तो उनके स्वीकृत मूल सिद्धान्तों से विरोध होता है। जैसे, नैयायिक सर्वथा भेदवादी होने से प्रमाण और फल में पूर्णभेद स्थापित करने के लिए ज्ञान को प्रमाण न मानकर इन्द्रियादि को प्रमाण स्वीकार करता है और यह बहुत ही स्थूल दृष्टि है, इसीलिए नैयायिक को एक प्रमाण न मानकर इन्द्रिय, इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष और ज्ञान इन तीनों को प्रमाण मानना पड़ता है। बौद्ध क्षणिकवादी होने से अज्ञातार्थज्ञापक ज्ञान को ही प्रमाण मानते हैं तथा प्रमाण और फल में अभेद मानते हैं, अन्यथा क्षणिक सिद्धान्त होने से सामञ्जस्य ही नहीं बनेगा। इसी प्रकार सांख्य-योग, वेदान्त, मीमांसा और जैन दर्शन भी अपने-अपने स्वीकृत मूलभूत सिद्धान्तों से अनुबद्ध हैं। जहाँ तक स्थूल दृष्टि का प्रश्न है, न्यायवैशेषिक का सिद्धान्त ठीक है, परन्तु हम ज्यों-ज्यों सूक्ष्म दृष्टि से विचार करते हैं तो क्रमश: इन्द्रियवृत्ति, अन्तःकरणवृत्ति, ज्ञातृव्यापार व ज्ञान की प्रमाणता तक पहुँच जाते हैं क्योंकि ज्ञानातिरिक्त अचेतन इन्द्रियादि को प्रमाण मानने पर एक तो उनमें प्रमाकरणता (साधकतमता) नहीं बनती है और दूसरे अचेतन इन्द्रियादि से ज्ञान नहीं हो सकता क्योंकि ज्ञान चेतन का धर्म है। जब तक चेतन का सम्बन्ध नहीं होगा तब तक ज्ञान पैदा नहीं हो सकता अन्यथा मृत पुरुष की इन्द्रियों को भी ज्ञान होना चाहिए। यदि इस दोष से बचने के लिए इन्द्रियों में शक्ति विशेष या योग्यता की कल्पना की जाय (जो कि जीवितावस्था में रहती है और मृतावस्था आदि में नहीं रहती है) तो वह शक्ति इन्द्रिय से भिन्न ही होगी, अभिन्न नहीं, क्योंकि शक्ति को इन्द्रिय से अभिन्न मानने पर कोई फायदा नहीं होगा। इन्द्रिय से भिन्न शक्ति अन्ततोगत्वा ज्ञानरूप ही पड़ेगी। तीसरे इन्द्रिय को प्रमाण मानने पर सर्वज्ञ का अभाव होगा। चौथे इन्द्रिय को प्रमाण मानने पर भी ज्ञान को प्रमाण मानते ही हैं फिर लाघव हेतु से केवल ज्ञान को क्यों नहीं मान लेते। इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष को यदि प्रमाण माना जाय तब भी उपर्युक्त सभी दोष आते हैं तथा सन्निकर्ष के द्विष्ठ (इन्द्रिय और अर्थ इन दो में) होने से प्रमाण के फल को भी दो में रहने वाला (द्विष्ठ-इन्द्रिय और अर्थ) मानना पड़ेगा, जिससे घट-पटादि अचेतन पदार्थों में भी ज्ञान के सद्भाव का प्रसङ्ग उपस्थित होगा और तब घटादि को भी हमारी तरह ज्ञान होने लगेगा। यहाँ यह नहीं कहा जा सकता है कि ज्ञान का सम्बन्ध (समवाय) केवल आत्मा (तत्सम्बन्ध से इन्द्रियाँ भी) से ही है, क्योंकि इसमें कोई नियामक हेतु नहीं है। जैसे अचेतन आत्मा में ज्ञान का समवाय है वैसे ही घटादि में भी क्यों न हो क्योंकि आपके यहाँ आत्मा से ज्ञान को पृथक् माना गया है। यदि आत्मा को ज्ञानस्वरूप मान लिया जाता है तो सिद्धान्तहानि दोष होता है। इसी प्रकार इन्द्रियवृत्ति आदि में भी नाना दोष हैं जिनका जैन दर्शन के न्यायग्रन्थों में खूब विचार किया गया है / अत: वहीं से जान लेना चाहिए। ज्ञान स्वसंवेदी है: यहाँ इतना समझ लेना चाहिए कि जो (ज्ञानभिन्न, इन्द्रियादि) स्वयं को नहीं जान सकते हैं वे दूसरे घटादि पदार्थों को कैसे जान सकते हैं। जैसे एक अन्धा दूसरे अन्धे को रास्ता नहीं बतला सकता। जैसे स्वयं प्रकाशी दीपक अन्य घटादि पदार्थों को प्रकाशित करने में समर्थ होता है वैसे ही स्वयं प्रकाशी ज्ञान ही घटादि पदार्थों का ज्ञान करने में समर्थ हो सकता है। इससे यह भी सिद्ध हो जाता है कि जो ज्ञान को प्रमाण मानकर भी उसे स्वसंवेदी नहीं मानते हैं, उनका 289