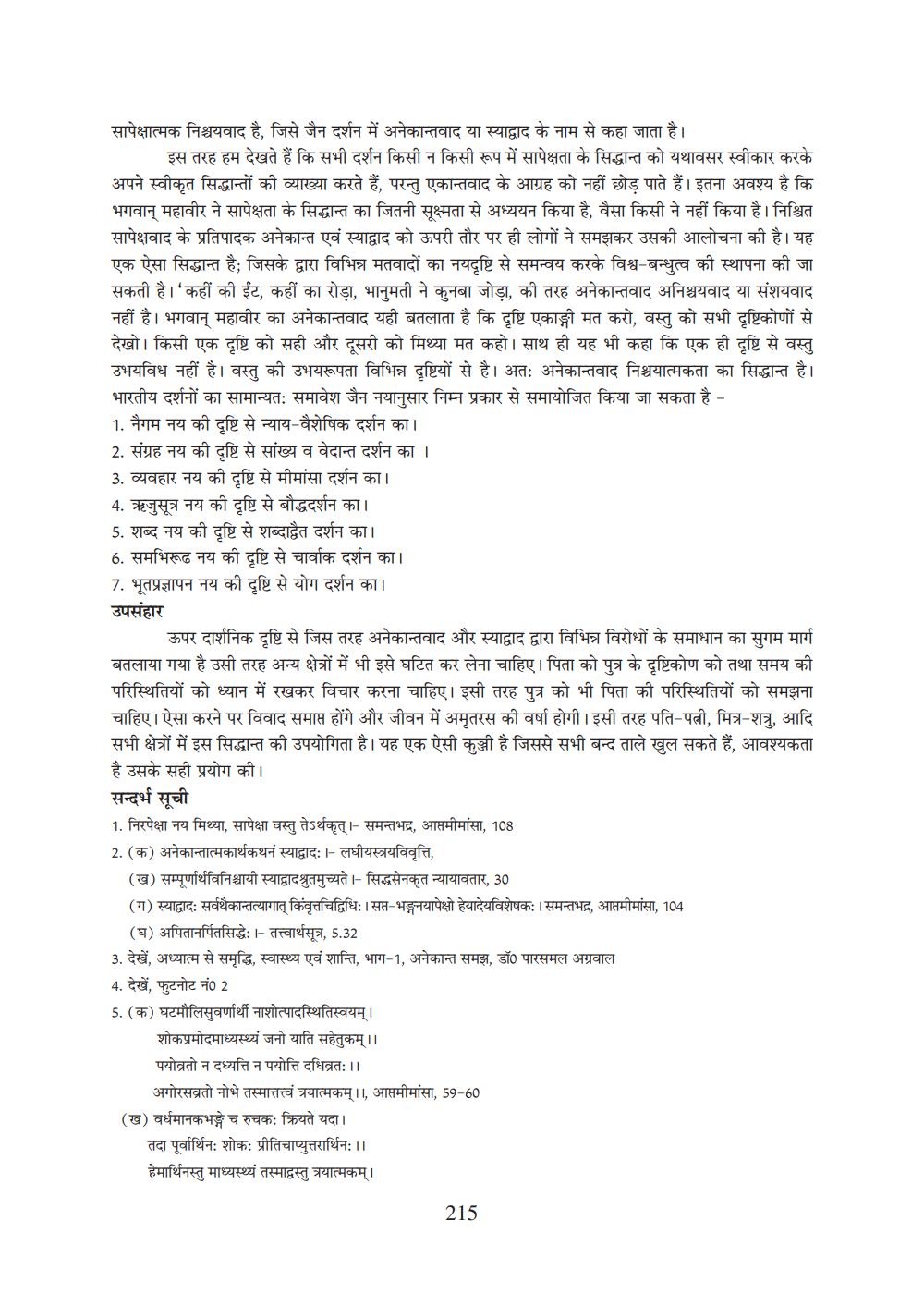________________ सापेक्षात्मक निश्चयवाद है, जिसे जैन दर्शन में अनेकान्तवाद या स्याद्वाद के नाम से कहा जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि सभी दर्शन किसी न किसी रूप में सापेक्षता के सिद्धान्त को यथावसर स्वीकार करके अपने स्वीकृत सिद्धान्तों की व्याख्या करते हैं, परन्तु एकान्तवाद के आग्रह को नहीं छोड़ पाते हैं। इतना अवश्य है कि भगवान् महावीर ने सापेक्षता के सिद्धान्त का जितनी सूक्ष्मता से अध्ययन किया है, वैसा किसी ने नहीं किया है। निश्चित सापेक्षवाद के प्रतिपादक अनेकान्त एवं स्याद्वाद को ऊपरी तौर पर ही लोगों ने समझकर उसकी आलोचना की है। यह एक ऐसा सिद्धान्त है; जिसके द्वारा विभिन्न मतवादों का नयदृष्टि से समन्वय करके विश्व-बन्धुत्व की स्थापना की जा सकती है। 'कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, की तरह अनेकान्तवाद अनिश्चयवाद या संशयवाद नहीं है। भगवान् महावीर का अनेकान्तवाद यही बतलाता है कि दृष्टि एकाङ्गी मत करो, वस्तु को सभी दृष्टिकोणों से देखो। किसी एक दृष्टि को सही और दूसरी को मिथ्या मत कहो। साथ ही यह भी कहा कि एक ही दृष्टि से वस्तु उभयविध नहीं है। वस्तु की उभयरूपता विभिन्न दृष्टियों से है। अतः अनेकान्तवाद निश्चयात्मकता का सिद्धान्त है। भारतीय दर्शनों का सामान्यतः समावेश जैन नयानुसार निम्न प्रकार से समायोजित किया जा सकता है - 1. नैगम नय की दृष्टि से न्याय-वैशेषिक दर्शन का। 2. संग्रह नय की दृष्टि से सांख्य व वेदान्त दर्शन का / 3. व्यवहार नय की दृष्टि से मीमांसा दर्शन का। 4. ऋजुसूत्र नय की दृष्टि से बौद्धदर्शन का। 5. शब्द नय की दृष्टि से शब्दाद्वैत दर्शन का। 6. समभिरूढ नय की दृष्टि से चार्वाक दर्शन का। 7. भूतप्रज्ञापन नय की दृष्टि से योग दर्शन का। उपसंहार ऊपर दार्शनिक दृष्टि से जिस तरह अनेकान्तवाद और स्याद्वाद द्वारा विभिन्न विरोधों के समाधान का सुगम मार्ग बतलाया गया है उसी तरह अन्य क्षेत्रों में भी इसे घटित कर लेना चाहिए। पिता को पुत्र के दृष्टिकोण को तथा समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर विचार करना चाहिए। इसी तरह पुत्र को भी पिता की परिस्थितियों को समझना चाहिए। ऐसा करने पर विवाद समाप्त होंगे और जीवन में अमृतरस की वर्षा होगी। इसी तरह पति-पत्नी, मित्र-शत्रु, आदि सभी क्षेत्रों में इस सिद्धान्त की उपयोगिता है। यह एक ऐसी कुञ्जी है जिससे सभी बन्द ताले खुल सकते हैं, आवश्यकता है उसके सही प्रयोग की। सन्दर्भ सूची 1. निरपेक्षा नय मिथ्या, सापेक्षा वस्तु तेऽर्थकृत्।- समन्तभद्र, आप्तमीमांसा, 108 2. (क) अनेकान्तात्मकार्थकथनं स्याद्वादः।- लघीयस्त्रयविवृत्ति, (ख) सम्पूर्णार्थविनिश्चायी स्याद्वादश्रुतमुच्यते।- सिद्धसेनकृत न्यायावतार, 30 (ग) स्याद्वाद: सर्वथैकान्तत्यागात् किंवृत्तचिद्विधिः / सप्त-भङ्गनयापेक्षो हेयादेयविशेषकः / समन्तभद्र, आप्तमीमांसा, 104 (घ) अपितानर्पितसिद्धेः।- तत्त्वार्थसूत्र, 5.32 3. देखें, अध्यात्म से समृद्धि, स्वास्थ्य एवं शान्ति, भाग-1, अनेकान्त समझ, डॉ० पारसमल अग्रवाल 4. देखें, फुटनोट नं02 5. (क) घटमौलिसुवर्णार्थी नाशोत्पादस्थितिस्वयम्। शोकप्रमोदमाध्यस्थ्यं जनो याति सहेतुकम्।। पयोव्रतो न दध्यत्ति न पयोत्ति दधिव्रतः।। अगोरसवतो नोभे तस्मात्तत्त्वं त्रयात्मकम् / / , आप्तमीमांसा, 59-60 (ख) वर्धमानकभङ्गे च रुचकः क्रियते यदा। तदा पूर्वार्थिनः शोकः प्रीतिचाप्युत्तरार्थिनः / / हेमार्थिनस्तु माध्यस्थ्यं तस्माद्वस्तु त्रयात्मकम्। 215