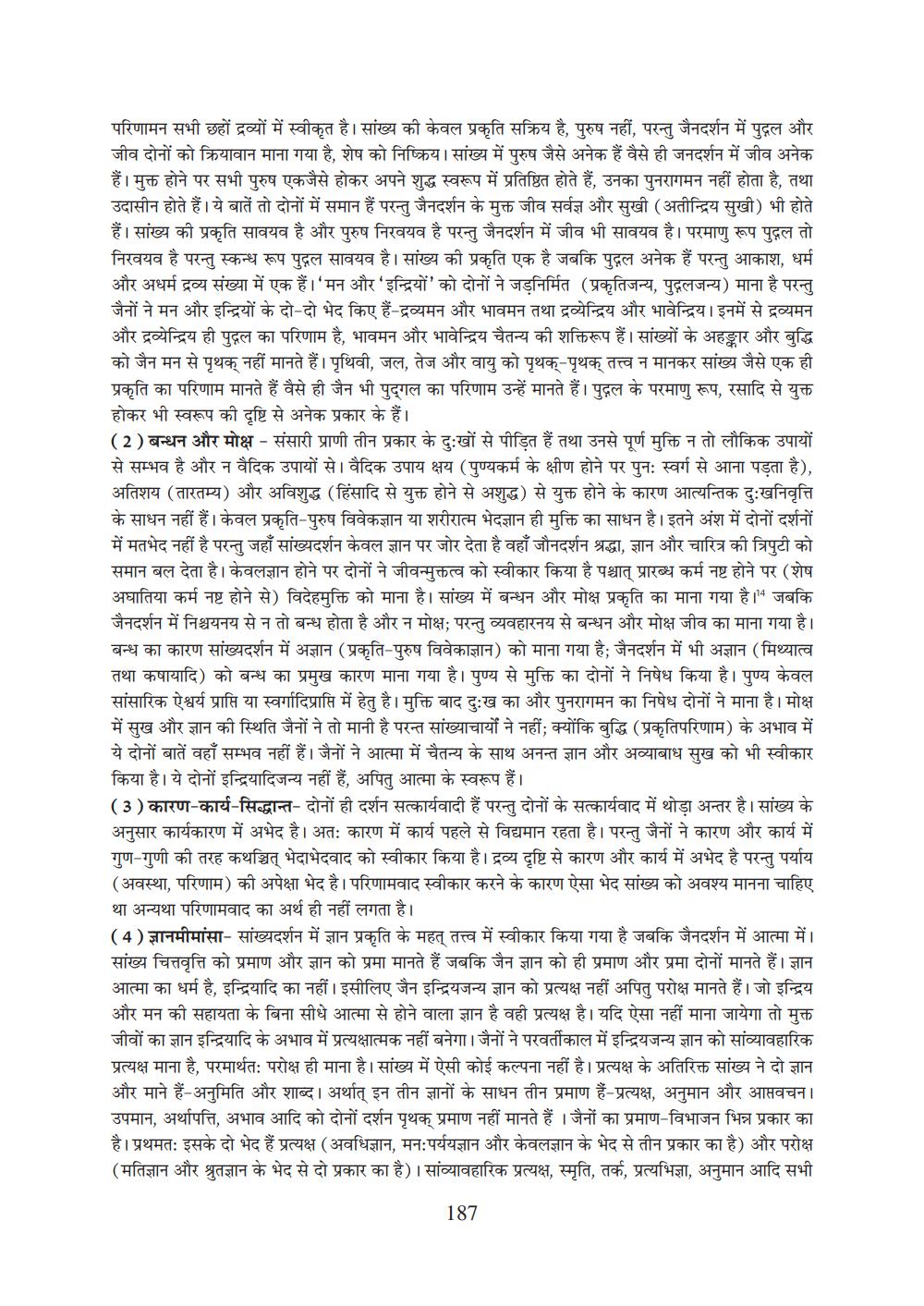________________ परिणामन सभी छहों द्रव्यों में स्वीकृत है। सांख्य की केवल प्रकृति सक्रिय है, पुरुष नहीं, परन्तु जैनदर्शन में पुद्गल और जीव दोनों को क्रियावान माना गया है, शेष को निष्क्रिय। सांख्य में पुरुष जैसे अनेक हैं वैसे ही जनदर्शन में जीव अनेक हैं। मुक्त होने पर सभी पुरुष एकजैसे होकर अपने शुद्ध स्वरूप में प्रतिष्ठित होते हैं, उनका पुनरागमन नहीं होता है, तथा उदासीन होते हैं। ये बातें तो दोनों में समान हैं परन्तु जैनदर्शन के मुक्त जीव सर्वज्ञ और सुखी (अतीन्द्रिय सुखी) भी होते हैं। सांख्य की प्रकृति सावयव है और पुरुष निरवयव है परन्तु जैनदर्शन में जीव भी सावयव है। परमाणु रूप पुद्गल तो निरवयव है परन्तु स्कन्ध रूप पुद्गल सावयव है। सांख्य की प्रकृति एक है जबकि पुद्गल अनेक हैं परन्तु आकाश, धर्म और अधर्म द्रव्य संख्या में एक हैं। 'मन और 'इन्द्रियों' को दोनों ने जड़निर्मित (प्रकृतिजन्य, पुद्गलजन्य) माना है परन्तु जैनों ने मन और इन्द्रियों के दो-दो भेद किए हैं-द्रव्यमन और भावमन तथा द्रव्येन्द्रिय और भावेन्द्रिय। इनमें से द्रव्यमन और द्रव्येन्द्रिय ही पुद्गल का परिणाम है, भावमन और भावेन्द्रिय चैतन्य की शक्तिरूप हैं। सांख्यों के अहङ्कार और बुद्धि को जैन मन से पृथक् नहीं मानते हैं। पृथिवी, जल, तेज और वायु को पृथक्-पृथक् तत्त्व न मानकर सांख्य जैसे एक ही प्रकृति का परिणाम मानते हैं वैसे ही जैन भी पुद्गल का परिणाम उन्हें मानते हैं। पुद्गल के परमाणु रूप, रसादि से युक्त होकर भी स्वरूप की दृष्टि से अनेक प्रकार के हैं। (2) बन्धन और मोक्ष- संसारी प्राणी तीन प्रकार के दुःखों से पीड़ित हैं तथा उनसे पूर्ण मुक्ति न तो लौकिक उपायों से सम्भव है और न वैदिक उपायों से। वैदिक उपाय क्षय (पुण्यकर्म के क्षीण होने पर पुनः स्वर्ग से आना पड़ता है), अतिशय (तारतम्य) और अविशुद्ध (हिंसादि से युक्त होने से अशुद्ध) से युक्त होने के कारण आत्यन्तिक दु:खनिवृत्ति के साधन नहीं हैं। केवल प्रकृति-पुरुष विवेकज्ञान या शरीरात्म भेदज्ञान ही मुक्ति का साधन है। इतने अंश में दोनों दर्शनों में मतभेद नहीं है परन्तु जहाँ सांख्यदर्शन केवल ज्ञान पर जोर देता है वहाँ जौनदर्शन श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र की त्रिपुटी को समान बल देता है। केवलज्ञान होने पर दोनों ने जीवन्मुक्तत्व को स्वीकार किया है पश्चात् प्रारब्ध कर्म नष्ट होने पर (शेष अघातिया कर्म नष्ट होने से) विदेहमुक्ति को माना है। सांख्य में बन्धन और मोक्ष प्रकृति का माना गया है। जबकि जैनदर्शन में निश्चयनय से न तो बन्ध होता है और न मोक्ष; परन्तु व्यवहारनय से बन्धन और मोक्ष जीव का माना गया है। बन्ध का कारण सांख्यदर्शन में अज्ञान (प्रकृति-पुरुष विवेकाज्ञान) को माना गया है; जैनदर्शन में भी अज्ञान (मिथ्यात्व तथा कषायादि) को बन्ध का प्रमुख कारण माना गया है। पुण्य से मुक्ति का दोनों ने निषेध किया है। पुण्य केवल सांसारिक ऐश्वर्य प्राप्ति या स्वर्गादिप्राप्ति में हेतु है। मुक्ति बाद दुःख का और पुनरागमन का निषेध दोनों ने माना है। मोक्ष में सुख और ज्ञान की स्थिति जैनों ने तो मानी है परन्त सांख्याचार्यों ने नहीं; क्योंकि बुद्धि (प्रकृतिपरिणाम) के अभाव में ये दोनों बातें वहाँ सम्भव नहीं हैं। जैनों ने आत्मा में चैतन्य के साथ अनन्त ज्ञान और अव्याबाध सुख को भी स्वीकार किया है। ये दोनों इन्द्रियादिजन्य नहीं हैं, अपितु आत्मा के स्वरूप हैं। (3) कारण-कार्य-सिद्धान्त- दोनों ही दर्शन सत्कार्यवादी हैं परन्तु दोनों के सत्कार्यवाद में थोड़ा अन्तर है। सांख्य के अनुसार कार्यकारण में अभेद है। अतः कारण में कार्य पहले से विद्यमान रहता है। परन्तु जैनों ने कारण और कार्य में गुण-गुणी की तरह कथञ्चित् भेदाभेदवाद को स्वीकार किया है। द्रव्य दृष्टि से कारण और कार्य में अभेद है परन्तु पर्याय (अवस्था, परिणाम) की अपेक्षा भेद है। परिणामवाद स्वीकार करने के कारण ऐसा भेद सांख्य को अवश्य मानना चाहिए था अन्यथा परिणामवाद का अर्थ ही नहीं लगता है। (4) ज्ञानमीमांसा-सांख्यदर्शन में ज्ञान प्रकृति के महत् तत्त्व में स्वीकार किया गया है जबकि जैनदर्शन में आत्मा में। सांख्य चित्तवृत्ति को प्रमाण और ज्ञान को प्रमा मानते हैं जबकि जैन ज्ञान को ही प्रमाण और प्रमा दोनों मानते हैं। ज्ञान आत्मा का धर्म है, इन्द्रियादि का नहीं। इसीलिए जैन इन्द्रियजन्य ज्ञान को प्रत्यक्ष नहीं अपितु परोक्ष मानते हैं। जो इन्द्रिय और मन की सहायता के बिना सीधे आत्मा से होने वाला ज्ञान है वही प्रत्यक्ष है। यदि ऐसा नहीं माना जायेगा तो मुक्त जीवों का ज्ञान इन्द्रियादि के अभाव में प्रत्यक्षात्मक नहीं बनेगा। जैनों ने परवर्तीकाल में इन्द्रियजन्य ज्ञान को सांव्यावहारिक प्रत्यक्ष माना है, परमार्थतः परोक्ष ही माना है। सांख्य में ऐसी कोई कल्पना नहीं है। प्रत्यक्ष के अतिरिक्त सांख्य ने दो ज्ञान और माने हैं-अनुमिति और शाब्द। अर्थात् इन तीन ज्ञानों के साधन तीन प्रमाण हैं-प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तवचन। उपमान, अर्थापत्ति, अभाव आदि को दोनों दर्शन पृथक् प्रमाण नहीं मानते हैं / जैनों का प्रमाण-विभाजन भिन्न प्रकार का है। प्रथमत: इसके दो भेद हैं प्रत्यक्ष (अवधिज्ञान, मन:पर्ययज्ञान और केवलज्ञान के भेद से तीन प्रकार का है) और परोक्ष (मतिज्ञान और श्रुतज्ञान के भेद से दो प्रकार का है)। सांव्यावहारिक प्रत्यक्ष, स्मृति, तर्क, प्रत्यभिज्ञा, अनुमान आदि सभी 187