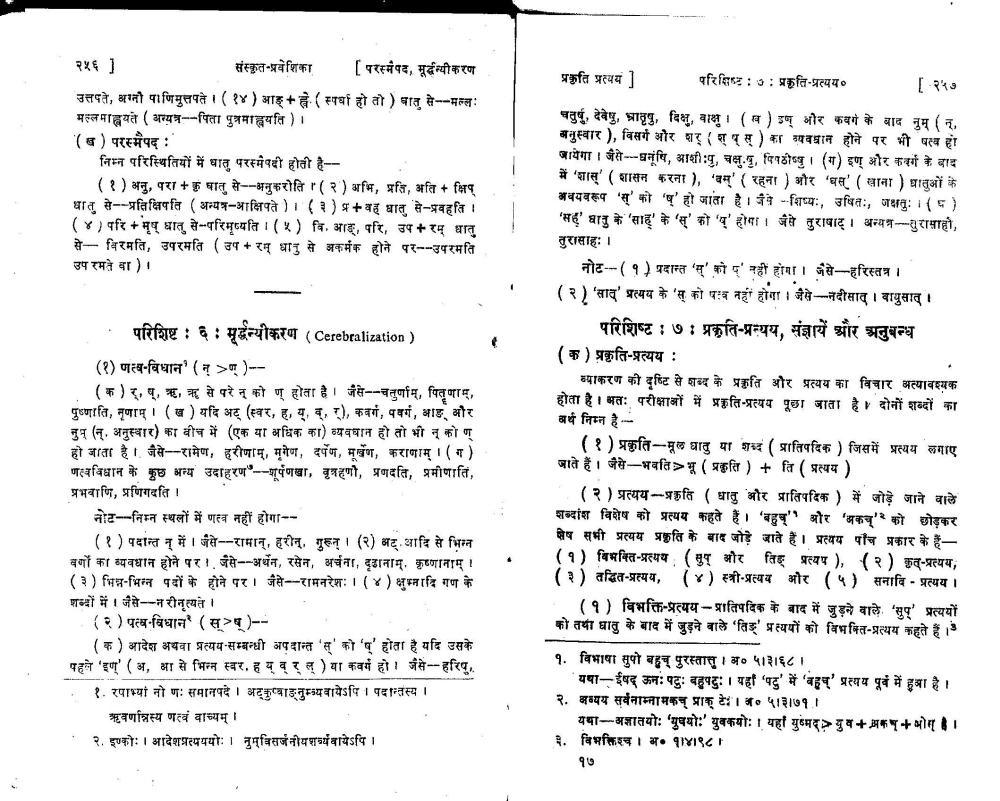________________ प्रकृति प्रत्यय ] परिशिष्ट :: प्रकृति-प्रत्यय० [ 257 256 ] संस्कृत-प्रवेशिका [परस्मैपद, मूर्द्धन्यीकरण उत्तपते, भग्नी पाणिमुत्तपते / (14) आङ् +हे (स्पर्धा हो तो) धातु से--मल्ल मल्ल माह्वयते ( अन्यत्र--पिता पुत्रमाह्वयति ) / (ख) परस्मैपद : निम्न परिस्थितियों में धातु परस्मैपदी होती है (1) अनु, परा + कृ धातु से--अनुकरोति / (2) अभि, प्रति, अति + क्षिप्.. धातु से--प्रतिक्षिपति (अन्यत्र-आक्षिपते)। (३)+वह धातु से-प्रवहति / (4) परि+मूष धातु से परिमृष्यति / (5) वि. आङ्, परि, उप + रम् धातु से-बिरमति, उपरमति ( उप + रम् धातु से अकर्मक होने पर---उपरमति उप रमते वा)। परिशिष्ट : 6: मृर्द्धन्यीकरण (Cerebralization ) (1) णत्व-विधान' (न >")-- (क) र , ऋ, ऋ से परे न् को ण होता है। जैसे--चतुर्णाम्, पितृणाम्, पुष्णाति, नृणाम् / (ख) यदि अट् (स्वर, ह, य, व, र), कवर्ग, पवर्ग, आङ, और नुम् (न, अनुस्वार) का बीच में (एक या अधिक का) व्यवधान हो तो भी न कोण हो जाता है। जैसे-रामेण, हरीणाम्, मृगेण, दर्पण, मूर्षण, कराणाम् / (ग) णत्यविधान के कुछ अन्य उदाहरण --शूर्पणखा, वणी, प्रणदति, प्रमीणाति, प्रभवाणि, प्रणिगदति / नोट-निम्न स्थलों में णत्व नहीं होगा-- (1) पदान्त न में / जैसे--रामान्, हरीन्, गुरुन् / (2) अट आदि से भिन्न वों का व्यवधान होने पर। जैसे--अर्थेन, रसेन, अर्चना, दृढानाम्, कृष्णानाम् / (3) भिन्न-भिन्न पदों के होने पर। जैसे-रामनरेशः / (4) क्षुम्नादि गण के शब्दों में / जैसे-नरीनत्यते।। (2) पत्व-विधान (स्>)--- (क) आदेश अथवा प्रत्यय-सम्बन्धी अपदान्त 'स' को 'ष' होता है यदि उसके पहले 'इण्' (अ, मा से भिन्न स्वर, ह य व र ल ) या कवर्ग हो। जैसे-हरिष, ...रपाभ्यां नो णः समानपदे / अकुप्वानुम्व्यवायेऽपि / पदान्तस्य / ऋवर्णान्नस्य णत्वं वाच्यम् / 2. इण्कोः / आदेशप्रत्यययोः / नुमुविसर्जनीयशर्यवायेऽपि / चतुर्षु, देवेषु, भ्रातृषु, दिक्षु, वाक्षु / (ख) इण् और कवगे के बाद नुम् (न्, अनुस्वार), विसर्ग और शर ( श् स् ) का व्यवधान होने पर भी षत्व हो जायेगा / जैसे---धनंषि, आशी:प, चक्षु., पिपठीषु / (ग) इण और कवर्ग के बाद में 'शास्' (शासन करना), 'वस्' (रहना ) और 'घस' (खाना) धातुओं के अवयवरूप 'स्' को '' हो जाता है। जैसे -शिष्यः, उषितः, जक्षतुः / (8) 'सह' धातु के 'साह' के 'स्' को 'ए' होगा। जैसे तुरापाट् / अन्यत्र---रासाही, तुरासाहः / नोट--(१) पदान्त 'स्' को म्' नहीं होगा। जैसे-हरिस्तत्र / (2) 'सात्' प्रत्यय के 'स् को पत्र नहीं होगा / जैसे-नदीसात् / वायुसात् / परिशिष्ट : 7: प्रकृति-प्रन्यय, संज्ञायें और अनुबन्ध (क) प्रकृति-प्रत्यय : व्याकरण की दृष्टि से शब्द के प्रकृति और प्रत्यय का विचार अत्यावश्यक होता है। अतः परीक्षाओं में प्रकृति-प्रत्यय पूछा जाता है। दोनों शब्दों का अर्थ निम्न है (1) प्रकृति-मूल धातु या शब्द (प्रातिपदिक ) जिसमें प्रत्यय लगाए जाते हैं। जैसे-भवति >भू (प्रकृति ) + ति (प्रत्यय) (2) प्रत्यय-प्रकृति (धातु और प्रातिपदिक ) में जोड़े जाने वाले शब्दांश विशेष को प्रत्यय कहते हैं। 'बहु' और 'अक'को छोड़कर शेष सभी प्रत्यय प्रकृति के बाद जोड़े जाते हैं। प्रत्यय पाँच प्रकार के हैं(१) विभक्ति-प्रत्यय (सुप् और तिङ् प्रत्यप), (2) कृत्-प्रत्यय, (3) तद्धित-प्रत्यय, (4) स्त्री-प्रत्यय और (5) सनावि-प्रत्यय / (1) विभक्ति-प्रत्यय-प्रातिपदिक के बाद में जुड़ने वाले 'सुप' प्रत्ययों को तथा धातु के बाद में जुड़ने वाले 'तिङ् प्रत्ययों को विभक्ति-प्रत्यय कहते हैं।' 1. विभाषा सुपो बहुच पुरस्तात्तु / अ० 5 / 3 / 68 / 'यषा-ईषद् ऊनः पटुः बहुपटुः / यहाँ 'पटु' में 'बहुप' प्रत्यय पूर्व में हुआ है। 2. अव्यय सर्वनाम्नामकच् प्राक् टे। ज०५।३।७१ / यथा--अज्ञातयोः 'युषयोः' युवकयोः / यहाँ युष्मद युव+क+ोग।। 3. विभक्तिश्च / अ. 1498 / 17