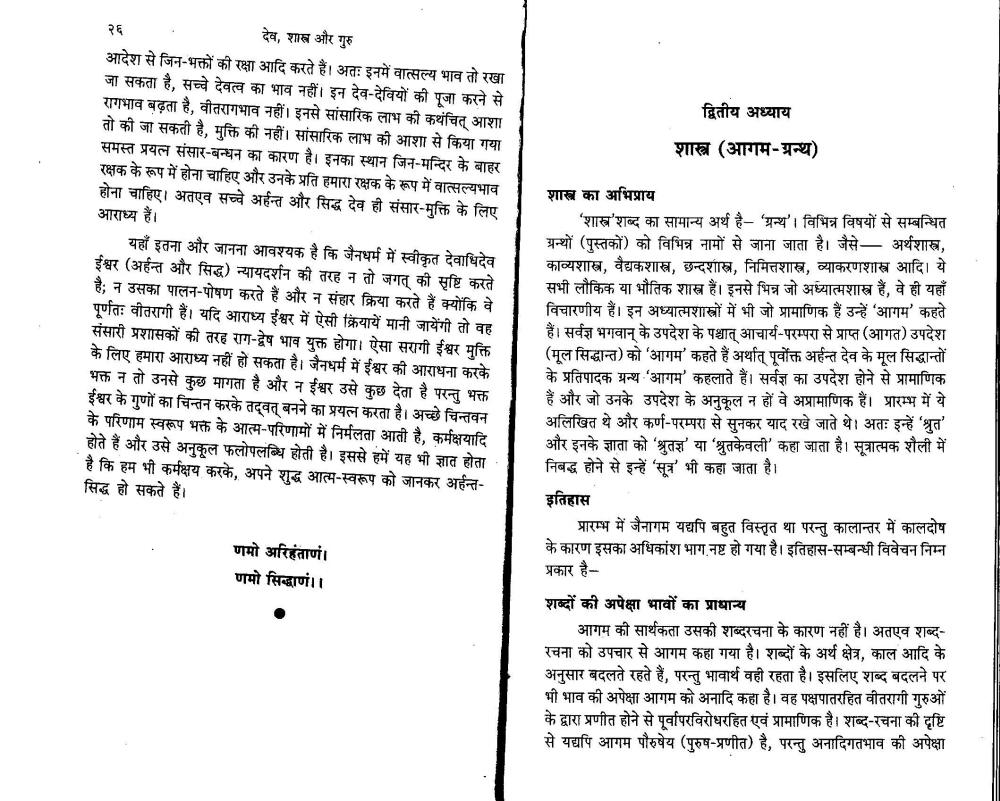________________ द्वितीय अध्याय शास्त्र (आगम-ग्रन्थ) देव, शास्त्र और गुरु आदेश से जिन-भक्तों की रक्षा आदि करते हैं। अतः इनमें वात्सल्य भाव तो रखा जा सकता है, सच्चे देवत्व का भाव नहीं। इन देव-देवियों की पूजा करने से रागभाव बढ़ता है, वीतरागभाव नहीं। इनसे सांसारिक लाभ की कथंचित् आशा तो की जा सकती है, मुक्ति की नहीं। सांसारिक लाभ की आशा से किया गया समस्त प्रयल संसार-बन्धन का कारण है। इनका स्थान जिन-मन्दिर के बाहर रक्षक के रूप में होना चाहिए और उनके प्रति हमारा रक्षक के रूप में वात्सल्यभाव होना चाहिए। अतएव सच्चे अर्हन्त और सिद्ध देव ही संसार-मुक्ति के लिए आराध्य हैं। यहाँ इतना और जानना आवश्यक है कि जैनधर्म में स्वीकृत देवाधिदेव ईश्वर (अर्हन्त और सिद्ध) न्यायदर्शन की तरह न तो जगत् की सृष्टि करते है; न उसका पालन-पोषण करते हैं और न संहार क्रिया करते हैं क्योंकि वे पूर्णतः वीतरागी हैं। यदि आराध्य ईश्वर में ऐसी क्रियायें मानी जायेंगी तो वह संसारी प्रशासकों की तरह राग-द्वेष भाव युक्त होगा। ऐसा सरागी ईश्वर मुक्ति के लिए हमारा आराध्य नहीं हो सकता है। जैनधर्म में ईश्वर की आराधना करके भक्त न तो उनसे कुछ मागता है और न ईश्वर उसे कुछ देता है परन्तु भक्त ईश्वर के गुणों का चिन्तन करके तद्वत् बनने का प्रयल करता है। अच्छे चिन्तवन के परिणाम स्वरूप भक्त के आत्म-परिणामों में निर्मलता आती है, कर्मक्षयादि होते हैं और उसे अनुकूल फलोपलब्धि होती है। इससे हमें यह भी ज्ञात होता है कि हम भी कर्मक्षय करके, अपने शुद्ध आत्म-स्वरूप को जानकर अर्हन्तसिद्ध हो सकते हैं। शास्त्र का अभिप्राय 'शास्त्र'शब्द का सामान्य अर्थ है- 'ग्रन्थ' / विभिन्न विषयों से सम्बन्धित ग्रन्थों (पुस्तकों) को विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे- अर्थशास्त्र, काव्यशास्त्र, वैद्यकशास्त्र, छन्दशास्त्र, निमित्तशास्त्र, व्याकरणशास्त्र आदि। ये सभी लौकिक या भौतिक शास्त्र हैं। इनसे भिन्न जो अध्यात्मशास्त्र हैं, वे ही यहाँ विचारणीय हैं। इन अध्यात्मशास्त्रों में भी जो प्रामाणिक हैं उन्हें 'आगम' कहते हैं। सर्वज्ञ भगवान् के उपदेश के पश्चात् आचार्य-परम्परा से प्राप्त (आगत) उपदेश (मूल सिद्धान्त) को 'आगम' कहते हैं अर्थात् पूर्वोक्त अर्हन्त देव के मूल सिद्धान्तों के प्रतिपादक ग्रन्थ 'आगम' कहलाते हैं। सर्वज्ञ का उपदेश होने से प्रामाणिक हैं और जो उनके उपदेश के अनुकूल न हों वे अप्रामाणिक हैं। प्रारम्भ में ये अलिखित थे और कर्ण-परम्परा से सुनकर याद रखे जाते थे। अतः इन्हें 'श्रुत' और इनके ज्ञाता को 'श्रुतज्ञ' या 'श्रुतकेवली' कहा जाता है। सूत्रात्मक शैली में निबद्ध होने से इन्हें 'सूत्र' भी कहा जाता है। इतिहास प्रारम्भ में जैनागम यद्यपि बहुत विस्तृत था परन्तु कालान्तर में कालदोष के कारण इसका अधिकांश भाग नष्ट हो गया है। इतिहास-सम्बन्धी विवेचन निम्न प्रकार हैशब्दों की अपेक्षा भावों का प्राधान्य आगम की सार्थकता उसकी शब्दरचना के कारण नहीं है। अतएव शब्दरचना को उपचार से आगम कहा गया है। शब्दों के अर्थ क्षेत्र, काल आदि के अनुसार बदलते रहते हैं, परन्तु भावार्थ वही रहता है। इसलिए शब्द बदलने पर भी भाव की अपेक्षा आगम को अनादि कहा है। वह पक्षपातरहित वीतरागी गुरुओं के द्वारा प्रणीत होने से पूर्वापरविरोधरहित एवं प्रामाणिक है। शब्द-रचना की दृष्टि से यद्यपि आगम पौरुषेय (पुरुष-प्रणीत) है, परन्तु अनादिगतभाव की अपेक्षा णमो अरिहंताणं। णमो सिद्धाणं।।