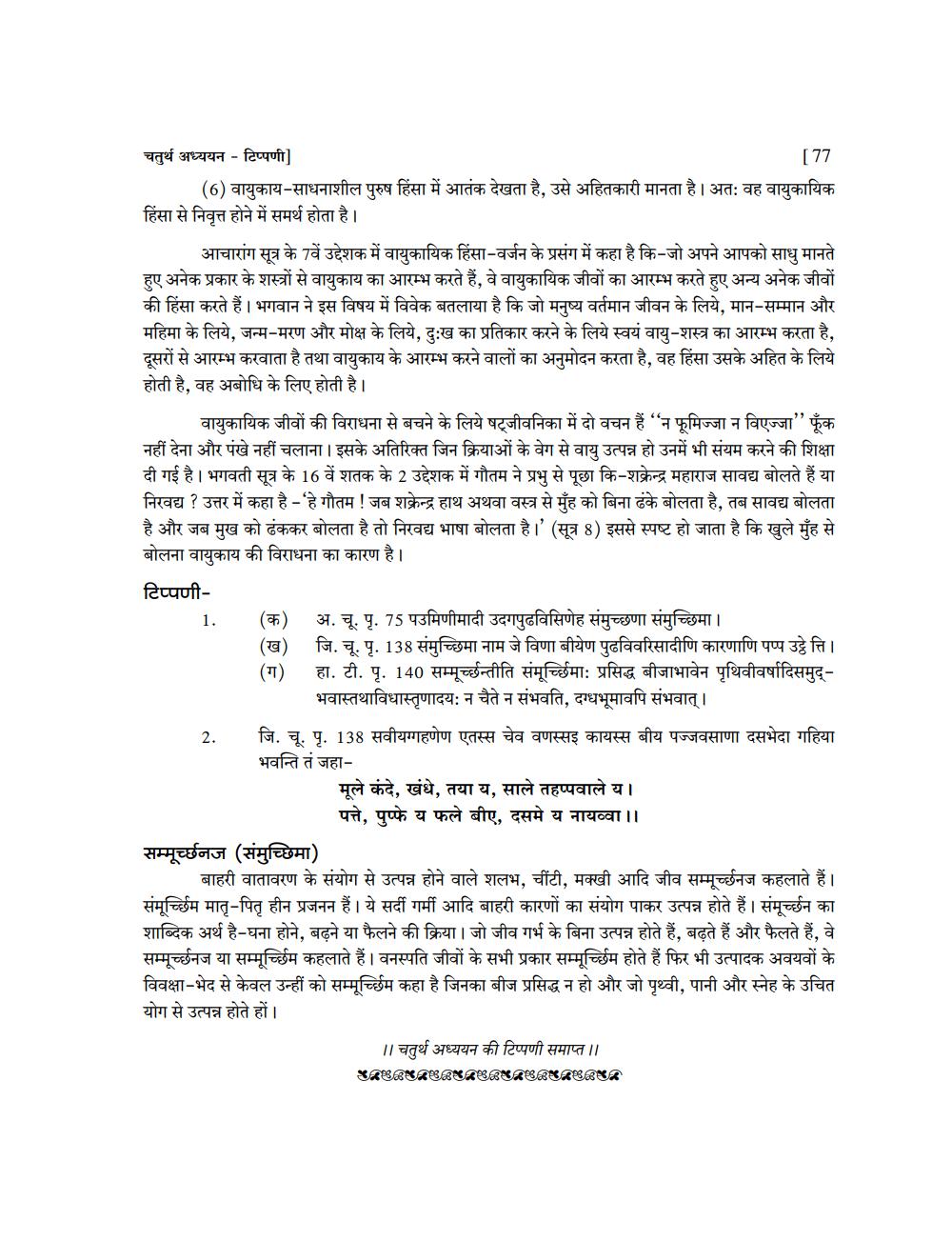________________
[77
चतुर्थ अध्ययन - टिप्पणी]
(6) वायुकाय-साधनाशील पुरुष हिंसा में आतंक देखता है, उसे अहितकारी मानता है। अत: वह वायुकायिक हिंसा से निवृत्त होने में समर्थ होता है।
आचारांग सूत्र के 7वें उद्देशक में वायुकायिक हिंसा-वर्जन के प्रसंग में कहा है कि-जो अपने आपको साधु मानते हुए अनेक प्रकार के शस्त्रों से वायुकाय का आरम्भ करते हैं, वे वायुकायिक जीवों का आरम्भ करते हुए अन्य अनेक जीवों की हिंसा करते हैं। भगवान ने इस विषय में विवेक बतलाया है कि जो मनुष्य वर्तमान जीवन के लिये, मान-सम्मान और महिमा के लिये, जन्म-मरण और मोक्ष के लिये, दुःख का प्रतिकार करने के लिये स्वयं वायु-शस्त्र का आरम्भ करता है, दूसरों से आरम्भ करवाता है तथा वायुकाय के आरम्भ करने वालों का अनुमोदन करता है, वह हिंसा उसके अहित के लिये होती है, वह अबोधि के लिए होती है।
वायुकायिक जीवों की विराधना से बचने के लिये षट्जीवनिका में दो वचन हैं “न फूमिज्जा न विएज्जा" फूंक नहीं देना और पंखे नहीं चलाना । इसके अतिरिक्त जिन क्रियाओं के वेग से वायु उत्पन्न हो उनमें भी संयम करने की शिक्षा दी गई है। भगवती सूत्र के 16 वें शतक के 2 उद्देशक में गौतम ने प्रभु से पूछा कि-शक्रेन्द्र महाराज सावध बोलते हैं या निरवद्य ? उत्तर में कहा है -'हे गौतम ! जब शक्रेन्द्र हाथ अथवा वस्त्र से मुँह को बिना ढंके बोलता है, तब सावध बोलता है और जब मुख को ढंककर बोलता है तो निरवद्य भाषा बोलता है।' (सूत्र 8) इससे स्पष्ट हो जाता है कि खुले मुँह से बोलना वायुकाय की विराधना का कारण है। टिप्पणी
अ. चू. पृ. 75 पउमिणीमादी उदगपुढविसिणेह संमुच्छणा समुच्छिमा। (ख) जि. चू. पृ. 138 समुच्छिमा नाम जे विणा बीयेण पुढविवरिसादीणि कारणाणि पप्प उट्टे त्ति । (ग) हा. टी. पृ. 140 सम्मूर्च्छन्तीति संमूर्छिमाः प्रसिद्ध बीजाभावेन पृथिवीवर्षादिसमुद्
भवास्तथाविधास्तृणादयः न चैते न संभवति, दग्धभूमावपि संभवात् । 2.
जि. चू. पृ. 138 सवीयग्गहणेण एतस्स चेव वणस्सइ कायस्स बीय पज्जवसाणा दसभेदा गहिया भवन्ति तं जहा
मूले कंदे, खंधे, तया य, साले तहप्पवाले य।
पत्ते, पुप्फे य फले बीए, दसमे य नायव्वा ।। सम्मूर्च्छनज (संमुच्छिमा)
___ बाहरी वातावरण के संयोग से उत्पन्न होने वाले शलभ, चींटी, मक्खी आदि जीव सम्मूर्छनज कहलाते हैं। संमूर्छिम मातृ-पितृ हीन प्रजनन हैं। ये सर्दी गर्मी आदि बाहरी कारणों का संयोग पाकर उत्पन्न होते हैं। संमूर्छन का शाब्दिक अर्थ है-घना होने, बढ़ने या फैलने की क्रिया । जो जीव गर्भ के बिना उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं और फैलते हैं, वे सम्मूर्च्छनज या सम्मूमि कहलाते हैं। वनस्पति जीवों के सभी प्रकार सम्मूर्छिम होते हैं फिर भी उत्पादक अवयवों के विवक्षा-भेद से केवल उन्हीं को सम्मूर्छिम कहा है जिनका बीज प्रसिद्ध न हो और जो पृथ्वी, पानी और स्नेह के उचित योग से उत्पन्न होते हों।
।। चतुर्थ अध्ययन की टिप्पणी समाप्त ।। URBURBURUBURBERROR
क)