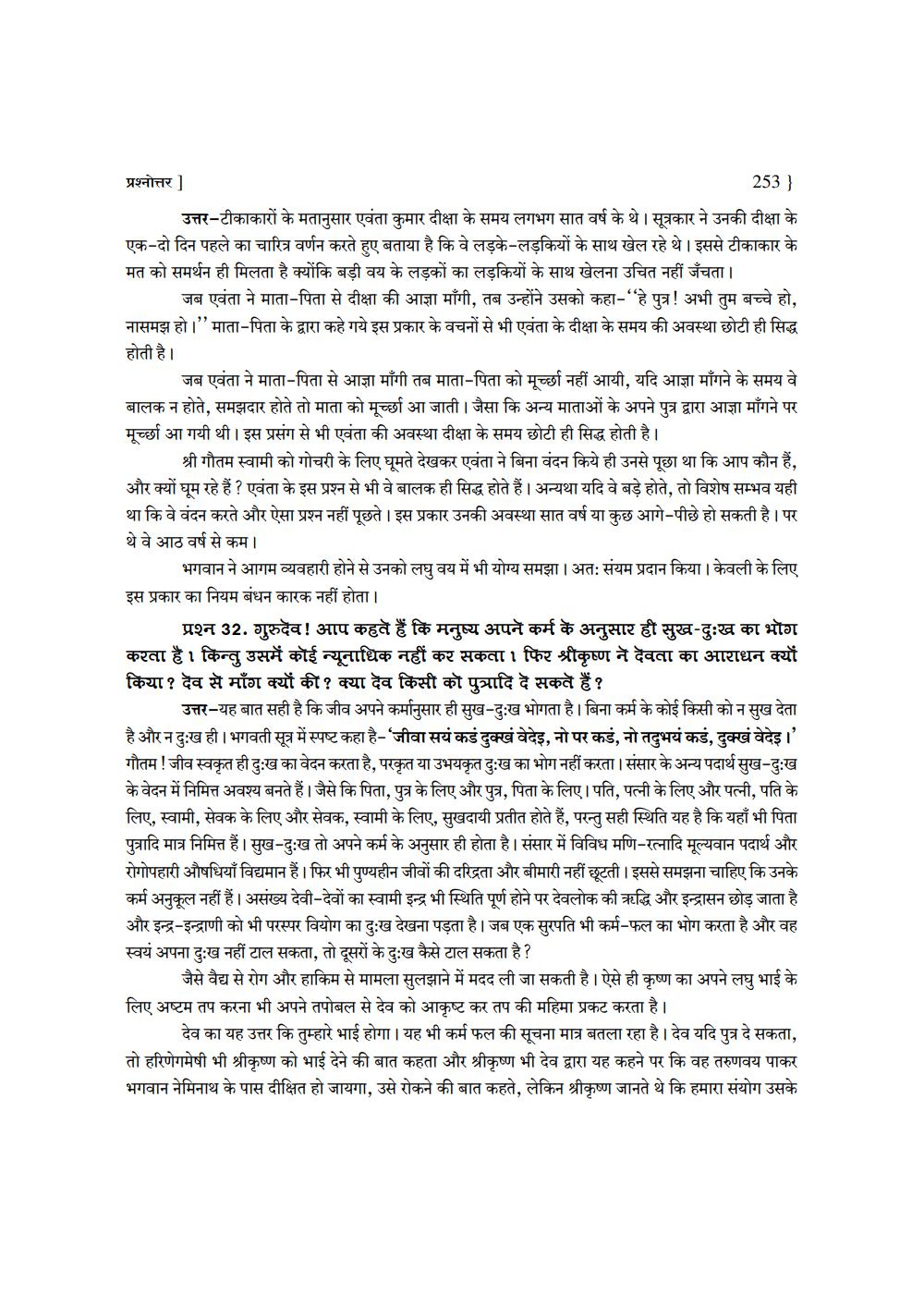________________
प्रश्नोत्तर]
253}
उत्तर-टीकाकारों के मतानुसार एवंता कुमार दीक्षा के समय लगभग सात वर्ष के थे। सूत्रकार ने उनकी दीक्षा के एक-दो दिन पहले का चारित्र वर्णन करते हुए बताया है कि वे लड़के-लड़कियों के साथ खेल रहे थे। इससे टीकाकार के मत को समर्थन ही मिलता है क्योंकि बड़ी वय के लड़कों का लड़कियों के साथ खेलना उचित नहीं ऊँचता।
जब एवंता ने माता-पिता से दीक्षा की आज्ञा माँगी, तब उन्होंने उसको कहा- “हे पुत्र! अभी तुम बच्चे हो, नासमझ हो।" माता-पिता के द्वारा कहे गये इस प्रकार के वचनों से भी एवंता के दीक्षा के समय की अवस्था छोटी ही सिद्ध होती है।
जब एवंता ने माता-पिता से आज्ञा माँगी तब माता-पिता को मूर्छा नहीं आयी, यदि आज्ञा माँगने के समय वे बालक न होते, समझदार होते तो माता को मूर्छा आ जाती । जैसा कि अन्य माताओं के अपने पुत्र द्वारा आज्ञा माँगने पर मूर्छा आ गयी थी। इस प्रसंग से भी एवंता की अवस्था दीक्षा के समय छोटी ही सिद्ध होती है।
श्री गौतम स्वामी को गोचरी के लिए घूमते देखकर एवंता ने बिना वंदन किये ही उनसे पूछा था कि आप कौन हैं, और क्यों घूम रहे हैं? एवंता के इस प्रश्न से भी वे बालक ही सिद्ध होते हैं। अन्यथा यदि वे बड़े होते, तो विशेष सम्भव यही था कि वे वंदन करते और ऐसा प्रश्न नहीं पूछते । इस प्रकार उनकी अवस्था सात वर्ष या कुछ आगे-पीछे हो सकती है। पर थे वे आठ वर्ष से कम।
भगवान ने आगम व्यवहारी होने से उनको लघु वय में भी योग्य समझा । अतः संयम प्रदान किया। केवली के लिए इस प्रकार का नियम बंधन कारक नहीं होता।
प्रश्न 32. गुरुदेव! आप कहते हैं कि मनुष्य अपने कर्म के अनुसार ही सुख-दुःख का भोग करता है। किन्तु उसमें कोई न्यूनाधिक नहीं कर सकता। फिर श्रीकृष्ण ने देवता का आराधन क्यों किया ? देव से माँग क्यों की? क्या देव किसी को पुत्रादि दे सकते हैं ?
उत्तर-यह बात सही है कि जीव अपने कर्मानुसार ही सुख-दु:ख भोगता है। बिना कर्म के कोई किसी को न सुख देता है और न दुःख ही। भगवती सूत्र में स्पष्ट कहा है-'जीवा सयं कडं दुक्खं वेदेइ, नो पर कडं, नो तदुभयं कडं, दुक्खं वेदेइ।' गौतम ! जीव स्वकृत ही दुःख का वेदन करता है, परकृत या उभयकृत दु:ख का भोग नहीं करता। संसार के अन्य पदार्थसुख-दुःख के वेदन में निमित्त अवश्य बनते हैं। जैसे कि पिता, पुत्र के लिए और पुत्र, पिता के लिए। पति, पत्नी के लिए और पत्नी, पति के लिए, स्वामी, सेवक के लिए और सेवक, स्वामी के लिए, सुखदायी प्रतीत होते हैं, परन्तु सही स्थिति यह है कि यहाँ भी पिता पुत्रादि मात्र निमित्त हैं। सुख-दुःख तो अपने कर्म के अनुसार ही होता है। संसार में विविध मणि-रत्नादि मूल्यवान पदार्थ और रोगोपहारी औषधियाँ विद्यमान हैं। फिर भी पुण्यहीन जीवों की दरिद्रता और बीमारी नहीं छूटती। इससे समझना चाहिए कि उनके कर्म अनुकूल नहीं हैं। असंख्य देवी-देवों का स्वामी इन्द्र भी स्थिति पूर्ण होने पर देवलोक की ऋद्धि और इन्द्रासन छोड़ जाता है
और इन्द्र-इन्द्राणी को भी परस्पर वियोग का दुःख देखना पड़ता है। जब एक सुरपति भी कर्म-फल का भोग करता है और वह स्वयं अपना दु:ख नहीं टाल सकता, तो दूसरों के दुःख कैसे टाल सकता है?
जैसे वैद्य से रोग और हाकिम से मामला सुलझाने में मदद ली जा सकती है। ऐसे ही कृष्ण का अपने लघु भाई के लिए अष्टम तप करना भी अपने तपोबल से देव को आकृष्ट कर तप की महिमा प्रकट करता है।
देव का यह उत्तर कि तुम्हारे भाई होगा। यह भी कर्म फल की सूचना मात्र बतला रहा है। देव यदि पुत्र दे सकता, तो हरिणेगमेषी भी श्रीकृष्ण को भाई देने की बात कहता और श्रीकृष्ण भी देव द्वारा यह कहने पर कि वह तरुणवय पाकर भगवान नेमिनाथ के पास दीक्षित हो जायगा, उसे रोकने की बात कहते, लेकिन श्रीकृष्ण जानते थे कि हमारा संयोग उसके