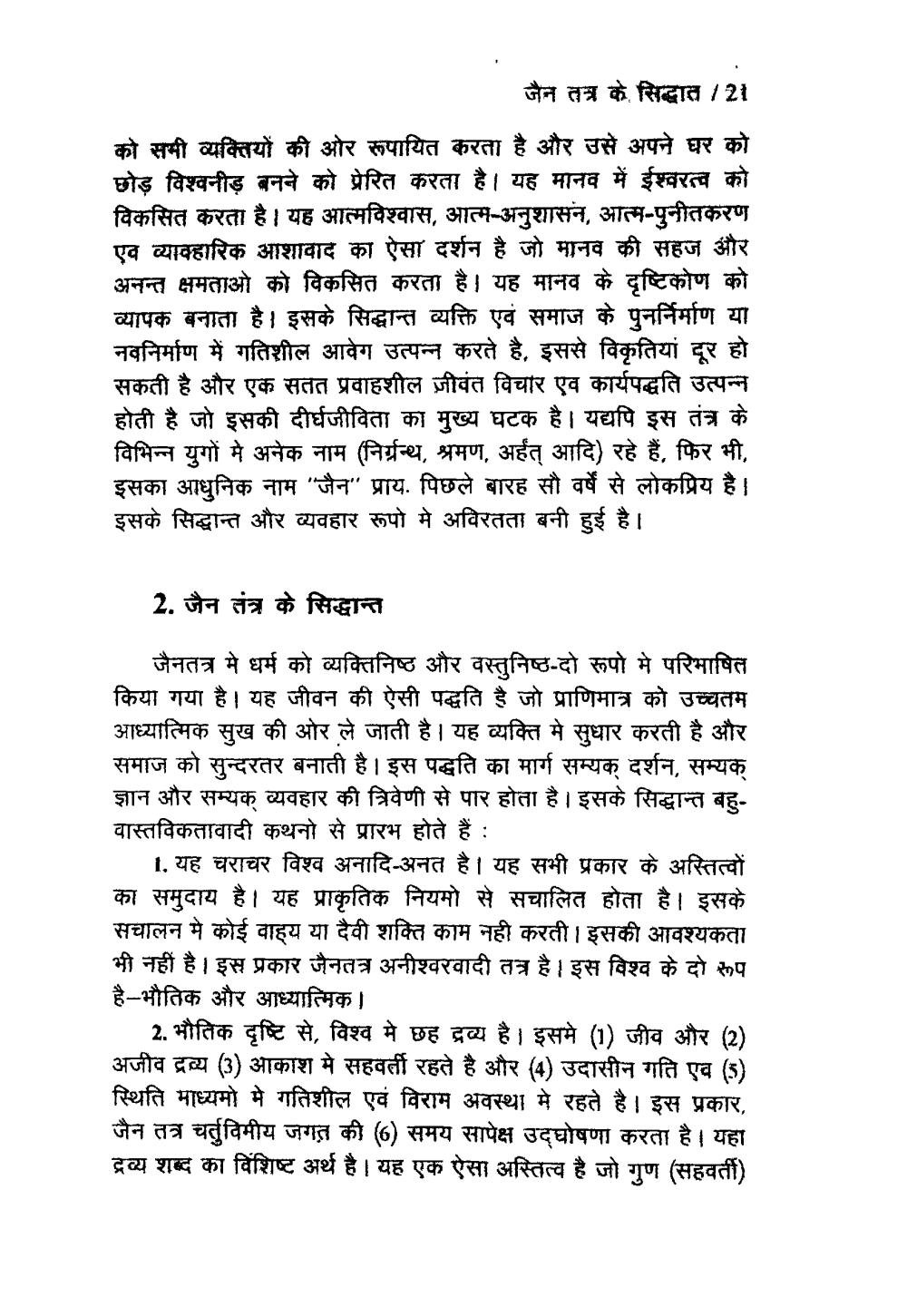________________
जैन तत्र के सिद्धात /21
को समी व्यक्तियों की ओर रूपायित करता है और उसे अपने घर को छोड़ विश्वनीड़ बनने को प्रेरित करता है। यह मानव में ईश्वरत्व को विकसित करता है। यह आत्मविश्वास, आत्म-अनुशासन, आत्म-पुनीतकरण एव व्यावहारिक आशावाद का ऐसा दर्शन है जो मानव की सहज और अनन्त क्षमताओ को विकसित करता है। यह मानव के दृष्टिकोण को व्यापक बनाता है। इसके सिद्धान्त व्यक्ति एवं समाज के पुनर्निर्माण या नवनिर्माण में गतिशील आवेग उत्पन्न करते है, इससे विकृतियां दूर हो सकती है और एक सतत प्रवाहशील जीवंत विचार एव कार्यपद्धति उत्पन्न होती है जो इसकी दीर्घजीविता का मुख्य घटक है। यद्यपि इस तंत्र के विभिन्न युगों में अनेक नाम (निर्ग्रन्थ, श्रमण, अहँत् आदि) रहे हैं, फिर भी, इसका आधुनिक नाम "जैन" प्राय. पिछले बारह सौ वर्षे से लोकप्रिय है। इसके सिद्धान्त और व्यवहार रूपो मे अविरतता बनी हुई है।
2. जैन तंत्र के सिद्धान्त
जैनतत्र मे धर्म को व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ-दो रूपो में परिभाषित किया गया है। यह जीवन की ऐसी पद्धति है जो प्राणिमात्र को उच्चतम आध्यात्मिक सुख की ओर ले जाती है। यह व्यक्ति में सुधार करती है और समाज को सुन्दरतर बनाती है। इस पद्धति का मार्ग सम्यक् दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक् व्यवहार की त्रिवेणी से पार होता है। इसके सिद्धान्त बहुवास्तविकतावादी कथनो से प्रारभ होते हैं :
1. यह चराचर विश्व अनादि-अनत है। यह सभी प्रकार के अस्तित्वों का समुदाय है। यह प्राकृतिक नियमो से सचालित होता है। इसके सचालन मे कोई वाह्य या दैवी शक्ति काम नहीं करती। इसकी आवश्यकता भी नहीं है। इस प्रकार जैनतत्र अनीश्वरवादी तत्र है। इस विश्व के दो रूप है-भौतिक और आध्यात्मिक।
2. भौतिक दृष्टि से, विश्व मे छह द्रव्य है। इसमे (1) जीव और (2) अजीव द्रव्य (3) आकाश मे सहवर्ती रहते है और (4) उदासीन गति एव (5) स्थिति माध्यमो मे गतिशील एवं विराम अवस्था मे रहते है। इस प्रकार, जैन तत्र चर्तुविमीय जगत की (6) समय सापेक्ष उद्घोषणा करता है। यहा द्रव्य शब्द का विशिष्ट अर्थ है। यह एक ऐसा अस्तित्व है जो गुण (सहवर्ती)