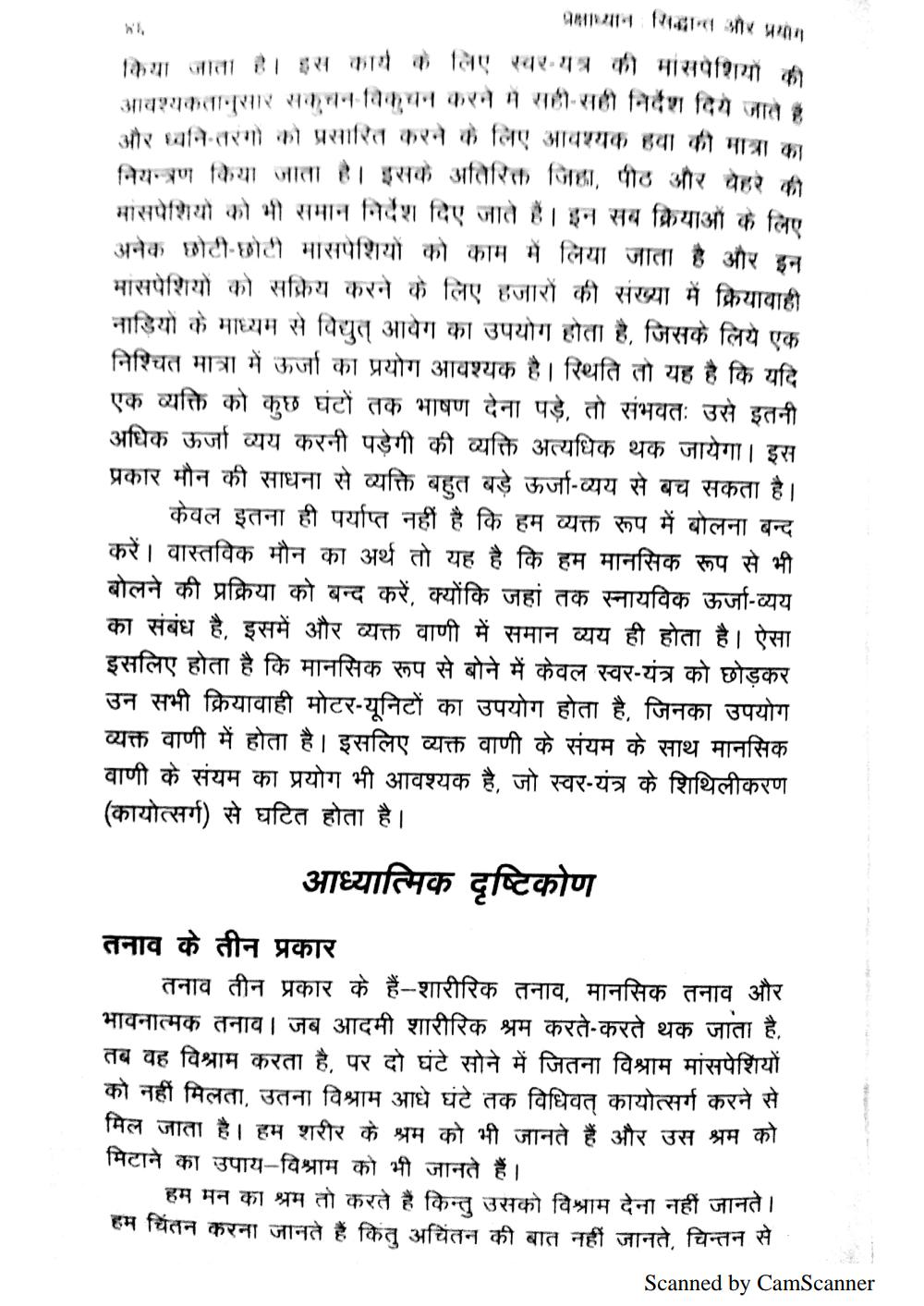________________
मान सिद्धान्त और प्रोग किया जाता है। इस कार्य के लिए रखर यत्र की मांसपेशियों की आवश्यकतानुसार सकुचन विकुचन करने में सही सही निर्देश दिये जाते और ध्वनि तरंगों को प्रसारित करने के लिए आवश्यक हवा की मात्रा का नियन्त्रण किया जाता है। इसके अतिरिक्त जिहा, पीठ और चेहरे की मासपेशियों को भी समान निर्देश दिए जाते है। इन सब क्रियाओं के लिए अनेक छोटी-छोटी मासपेशियों को काम में लिया जाता है और इन मासपेशियों को सक्रिय करने के लिए हजारों की संख्या में क्रियावाही नाडियों के माध्यम से विद्युत् आवेग का उपयोग होता है, जिसके लिये एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा का प्रयोग आवश्यक है। स्थिति तो यह है कि यदि एक व्यक्ति को कुछ घंटों तक भाषण देना पड़े, तो संभवतः उसे इतनी अधिक ऊर्जा व्यय करनी पड़ेगी की व्यक्ति अत्यधिक थक जायेगा। इस प्रकार मौन की साधना से व्यक्ति बहुत बड़े ऊर्जा-व्यय से बच सकता है।
केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है कि हम व्यक्त रूप में बोलना बन्द करें। वास्तविक मौन का अर्थ तो यह है कि हम मानसिक रूप से भी बोलने की प्रक्रिया को बन्द करें, क्योंकि जहां तक स्नायविक ऊर्जा-व्यय का संबंध है, इसमें और व्यक्त वाणी में समान व्यय ही होता है। ऐसा इसलिए होता है कि मानसिक रूप से बोने में केवल स्वर-यंत्र को छोड़कर उन सभी क्रियावाही मोटर-यूनिटों का उपयोग होता है, जिनका उपयोग व्यक्त वाणी में होता है। इसलिए व्यक्त वाणी के संयम के साथ मानसिक वाणी के संयम का प्रयोग भी आवश्यक है, जो स्वर-यंत्र के शिथिलीकरण (कायोत्सर्ग) से घटित होता है।
आध्यात्मिक दृष्टिकोण
तनाव के तीन प्रकार
तनाव तीन प्रकार के हैं-शारीरिक तनाव, मानसिक तनाव और भावनात्मक तनाव। जब आदमी शारीरिक श्रम करते-करते थक जाता है, तब वह विश्राम करता है, पर दो घंटे सोने में जितना विश्राम मांसपेशियों को नहीं मिलता, उतना विश्राम आधे घंटे तक विधिवत् कायोत्सर्ग करने से मिल जाता है। हम शरीर के श्रम को भी जानते हैं और उस श्रम को मिटाने का उपाय-विश्राम को भी जानते हैं।
हम मन का श्रम तो करते हैं किन्तु उसको विश्राम देना नहीं जानते। हम चिंतन करना जानते हैं किंतु अचिंतन की बात नहीं जानते, चिन्तन से
Scanned by CamScanner