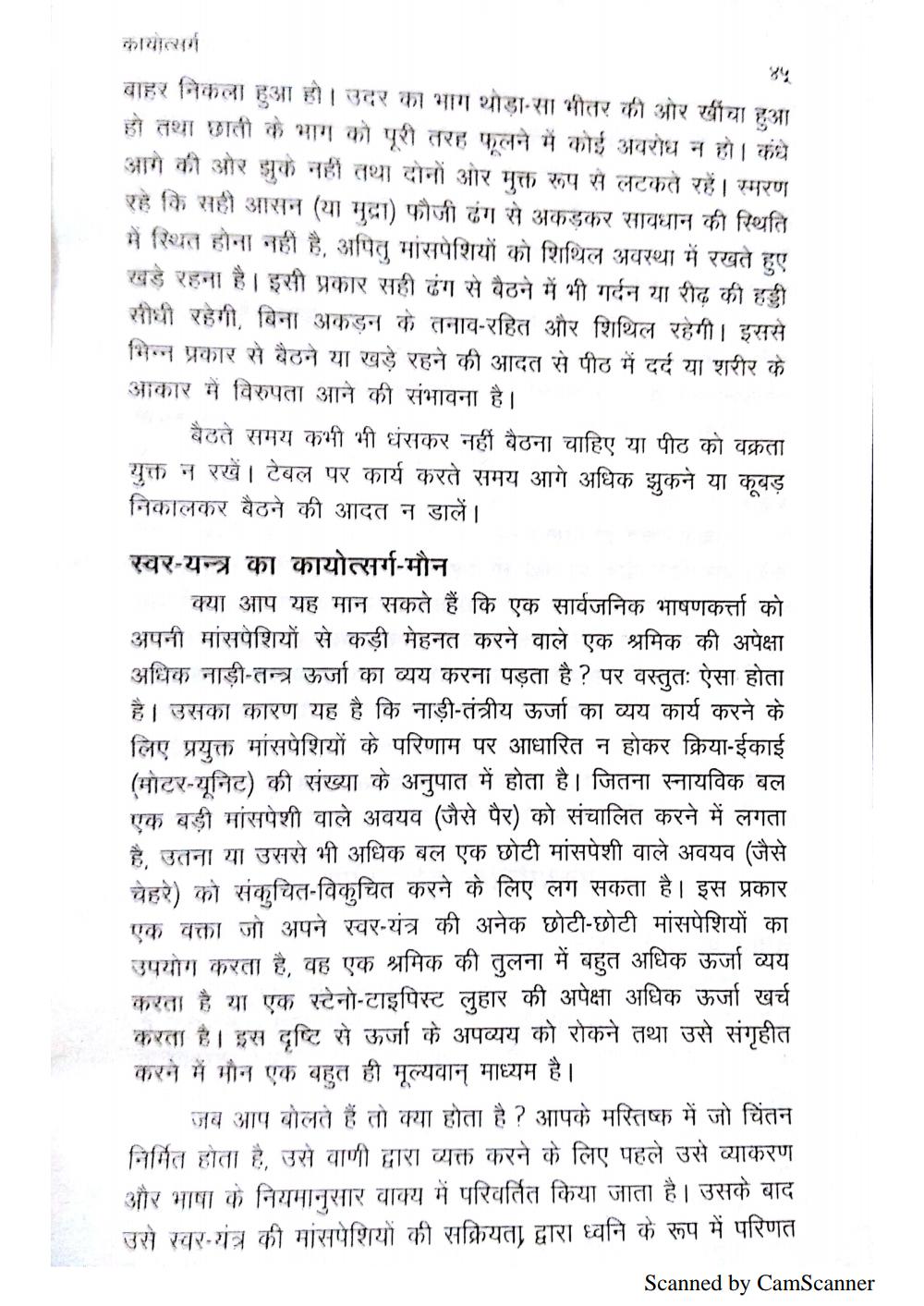________________
४५
कायोत्सर्ग
बाहर निकला हुआ हो। उदर का भाग थोड़ा-सा भीतर की ओर खींचा हुआ हो तथा छाती के भाग को पूरी तरह फूलने में कोई अवरोध न हो। कंधे आगे की ओर झुके नहीं तथा दोनों ओर मुक्त रूप से लटकते रहें। स्मरण रहे कि सही आसन (या मुद्रा) फौजी ढंग से अकड़कर सावधान की स्थिति में स्थित होना नहीं है, अपितु मांसपेशियों को शिथिल अवस्था में रखते हुए खड़े रहना है। इसी प्रकार सही ढंग से बैठने में भी गर्दन या रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, बिना अकड़न के तनाव रहित और शिथिल रहेगी। इससे भिन्न प्रकार से बैठने या खड़े रहने की आदत से पीठ में दर्द या शरीर के आकार में विरुपता आने की संभावना है।
बैठते समय कभी भी धंसकर नहीं बैठना चाहिए या पीठ को वक्रता युक्त न रखें। टेबल पर कार्य करते समय आगे अधिक झुकने या कूबड़ निकालकर बैठने की आदत न डालें ।
स्वर - यन्त्र का कायोत्सर्ग-मौन
क्या आप यह मान सकते हैं कि एक सार्वजनिक भाषणकर्त्ता को अपनी मांसपेशियों से कड़ी मेहनत करने वाले एक श्रमिक की अपेक्षा अधिक नाड़ी - तन्त्र ऊर्जा का व्यय करना पड़ता है ? पर वस्तुतः ऐसा होता है। उसका कारण यह है कि नाड़ी तंत्रीय ऊर्जा का व्यय कार्य करने के लिए प्रयुक्त मांसपेशियों के परिणाम पर आधारित न होकर क्रिया- ईकाई ( मोटर - यूनिट) की संख्या के अनुपात में होता है । जितना स्नायविक बल एक बड़ी मांसपेशी वाले अवयव (जैसे पैर) को संचालित करने में लगता है, उतना या उससे भी अधिक बल एक छोटी मांसपेशी वाले अवयव (जैसे चेहरे) को संकुचित - विकुचित करने के लिए लग सकता है। इस प्रकार एक वक्ता जो अपने स्वर-यंत्र की अनेक छोटी-छोटी मांसपेशियों का उपयोग करता है, वह एक श्रमिक की तुलना में बहुत अधिक ऊर्जा व्यय करता है या एक स्टेनो टाइपिस्ट लुहार की अपेक्षा अधिक ऊर्जा खर्च करता है। इस दृष्टि से ऊर्जा के अपव्यय को रोकने तथा उसे संगृहीत करने में मौन एक बहुत ही मूल्यवान् माध्यम है ।
जब आप बोलते हैं तो क्या होता है ? आपके मस्तिष्क में जो चिंतन निर्मित होता है, उसे वाणी द्वारा व्यक्त करने के लिए पहले उसे व्याकरण और भाषा के नियमानुसार वाक्य में परिवर्तित किया जाता है। उसके बाद उसे स्वर-यंत्र की मांसपेशियों की सक्रियता द्वारा ध्वनि के रूप में परिणत
Scanned by CamScanner