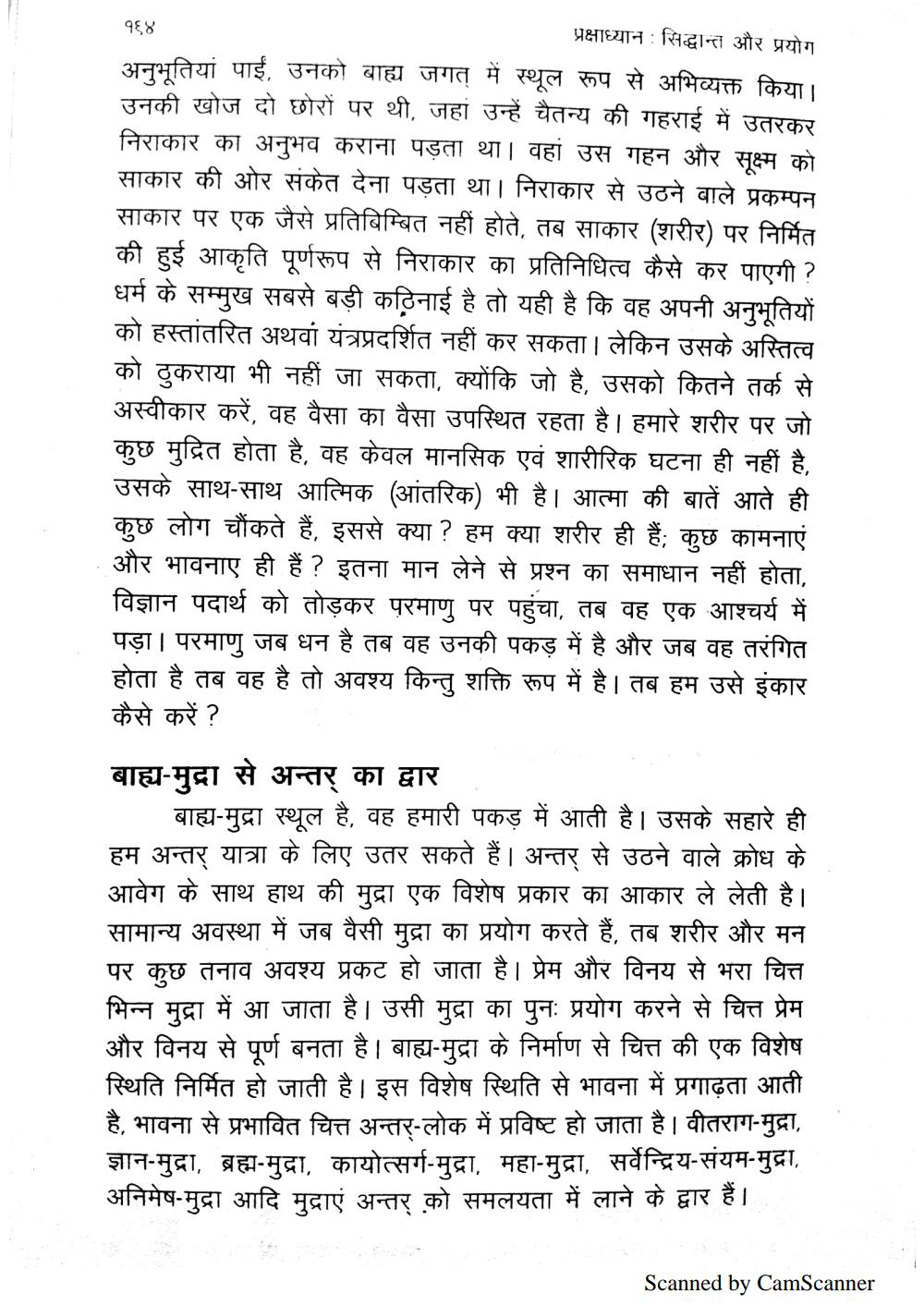________________
१६४
प्रक्षाध्यान : सिद्धान्त और प्रयोग अनुभूतियां पाईं, उनको बाह्य जगत् में स्थूल रूप से अभिव्यक्त किया। उनकी खोज दो छोरों पर थी, जहां उन्हें चैतन्य की गहराई में उतरकर निराकार का अनुभव कराना पड़ता था। वहां उस गहन और सूक्ष्म को साकार की ओर संकेत देना पड़ता था। निराकार से उठने वाले प्रकम्पन साकार पर एक जैसे प्रतिबिम्बित नहीं होते, तब साकार (शरीर) पर निर्मित की हुई आकृति पूर्णरूप से निराकार का प्रतिनिधित्व कैसे कर पाएगी? धर्म के सम्मुख सबसे बड़ी कठिनाई है तो यही है कि वह अपनी अनुभूतियों को हस्तांतरित अथवां यंत्रप्रदर्शित नहीं कर सकता। लेकिन उसके अस्तित्व को ठुकराया भी नहीं जा सकता, क्योंकि जो है, उसको कितने तर्क से अस्वीकार करें, वह वैसा का वैसा उपस्थित रहता है। हमारे शरीर पर जो कुछ मुद्रित होता है, वह केवल मानसिक एवं शारीरिक घटना ही नहीं है, उसके साथ-साथ आत्मिक (आंतरिक) भी है। आत्मा की बातें आते ही कुछ लोग चौंकते हैं, इससे क्या? हम क्या शरीर ही हैं; कुछ कामनाएं
और भावनाए ही हैं ? इतना मान लेने से प्रश्न का समाधान नहीं होता, विज्ञान पदार्थ को तोड़कर परमाणु पर पहुंचा, तब वह एक आश्चर्य में पड़ा। परमाणु जब धन है तब वह उनकी पकड़ में है और जब वह तरंगित होता है तब वह है तो अवश्य किन्तु शक्ति रूप में है। तब हम उसे इंकार कैसे करें?
बाह्य-मुद्रा से अन्तर् का द्वार
बाह्य-मुद्रा स्थूल है, वह हमारी पकड़ में आती है। उसके सहारे ही हम अन्तर् यात्रा के लिए उतर सकते हैं। अन्तर् से उठने वाले क्रोध के आवेग के साथ हाथ की मुद्रा एक विशेष प्रकार का आकार ले लेती है। सामान्य अवस्था में जब वैसी मुद्रा का प्रयोग करते हैं, तब शरीर और मन पर कुछ तनाव अवश्य प्रकट हो जाता है। प्रेम और विनय से भरा चित्त भिन्न मुद्रा में आ जाता है। उसी मुद्रा का पुनः प्रयोग करने से चित्त प्रेम
और विनय से पूर्ण बनता है। बाह्य-मुद्रा के निर्माण से चित्त की एक विशेष स्थिति निर्मित हो जाती है। इस विशेष स्थिति से भावना में प्रगाढ़ता आती है, भावना से प्रभावित चित्त अन्तर्-लोक में प्रविष्ट हो जाता है। वीतराग-मुद्रा, ज्ञान-मुद्रा, ब्रह्म-मुद्रा, कायोत्सर्ग-मुद्रा, महा-मुद्रा, सर्वेन्द्रिय-संयम-मुद्रा, अनिमेष-मुद्रा आदि मुद्राएं अन्तर् को समलयता में लाने के द्वार हैं।
Scanned by CamScanner