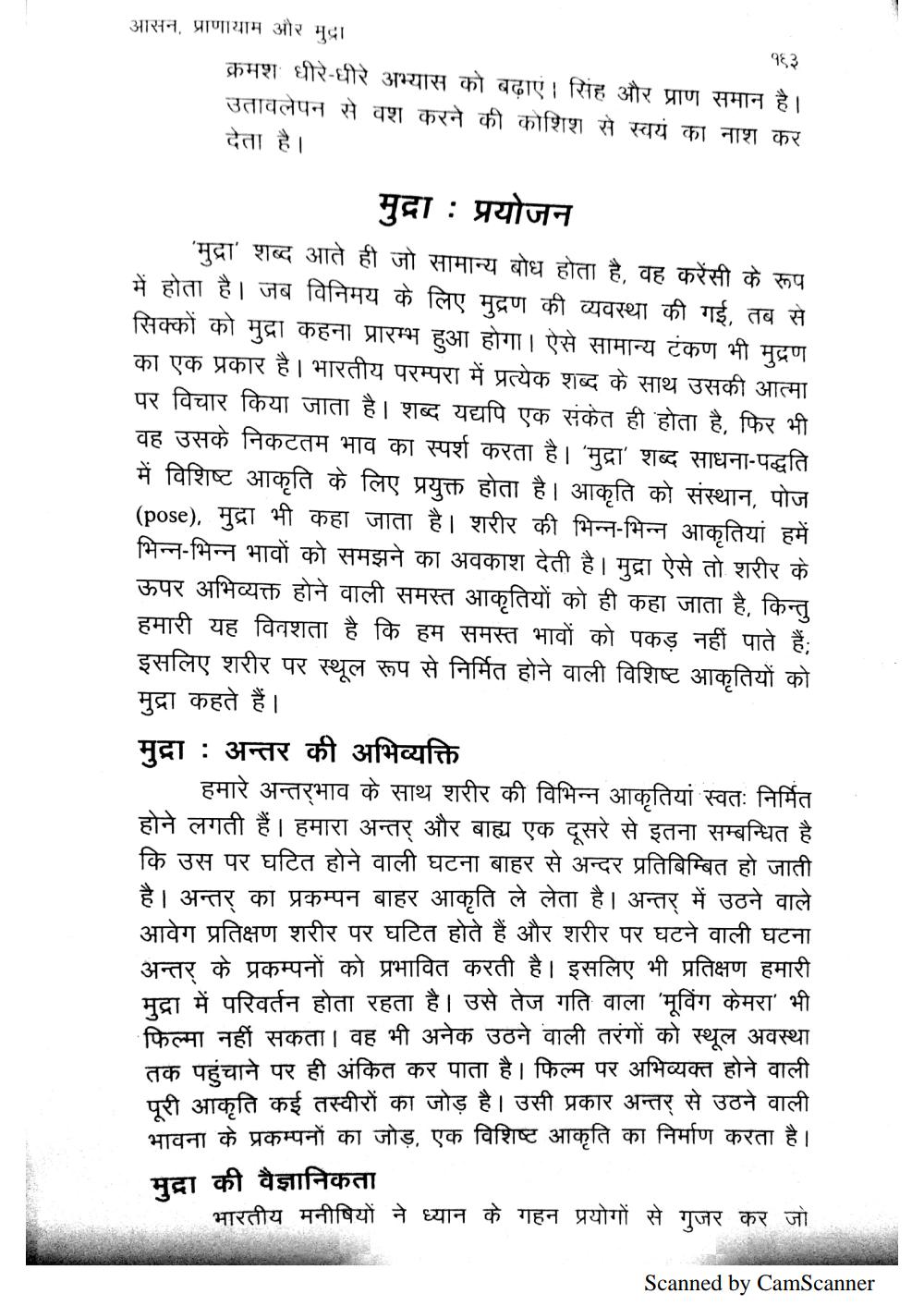________________
आसन, प्राणायाम और मुदा
१६३ क्रमश धीरे-धीरे अभ्यास को बढ़ाएं। सिंह और प्राण समान है। उतावलेपन से वश करने की कोशिश से स्वयं का नाश कर देता है।
मुद्रा : प्रयोजन 'मुद्रा' शब्द आते ही जो सामान्य बोध होता है, वह करेंसी के रूप में होता है। जब विनिमय के लिए मुद्रण की व्यवस्था की गई, तब से सिक्कों को मुद्रा कहना प्रारम्भ हुआ होगा। ऐसे सामान्य टंकण भी मुद्रण का एक प्रकार है। भारतीय परम्परा में प्रत्येक शब्द के साथ उसकी आत्मा पर विचार किया जाता है। शब्द यद्यपि एक संकेत ही होता है, फिर भी वह उसके निकटतम भाव का स्पर्श करता है। 'मुद्रा' शब्द साधना-पद्धति में विशिष्ट आकृति के लिए प्रयुक्त होता है। आकृति को संस्थान, पोज (pose), मुद्रा भी कहा जाता है। शरीर की भिन्न-भिन्न आकृतियां हमें भिन्न-भिन्न भावों को समझने का अवकाश देती है। मुद्रा ऐसे तो शरीर के ऊपर अभिव्यक्त होने वाली समस्त आकृतियों को ही कहा जाता है, किन्तु हमारी यह विवशता है कि हम समस्त भावों को पकड़ नहीं पाते हैं; इसलिए शरीर पर स्थूल रूप से निर्मित होने वाली विशिष्ट आकृतियों को मुद्रा कहते हैं। मुद्रा : अन्तर की अभिव्यक्ति
हमारे अन्तर्भाव के साथ शरीर की विभिन्न आकृतियां स्वतः निर्मित होने लगती हैं। हमारा अन्तर् और बाह्य एक दूसरे से इतना सम्बन्धित है कि उस पर घटित होने वाली घटना बाहर से अन्दर प्रतिबिम्बित हो जाती है। अन्तर् का प्रकम्पन बाहर आकृति ले लेता है। अन्तर् में उठने वाले आवेग प्रतिक्षण शरीर पर घटित होते हैं और शरीर पर घटने वाली घटना अन्तर् के प्रकम्पनों को प्रभावित करती है। इसलिए भी प्रतिक्षण हमारी मुद्रा में परिवर्तन होता रहता है। उसे तेज गति वाला 'मूविंग केमरा' भी फिल्मा नहीं सकता। वह भी अनेक उठने वाली तरंगों को स्थूल अवस्था तक पहुंचाने पर ही अंकित कर पाता है। फिल्म पर अभिव्यक्त होने वाली पूरी आकृति कई तस्वीरों का जोड़ है। उसी प्रकार अन्तर् से उठने वाली भावना के प्रकम्पनों का जोड़, एक विशिष्ट आकृति का निर्माण करता है। मुद्रा की वैज्ञानिकता
भारतीय मनीषियों ने ध्यान के गहन प्रयोगों से गुजर कर जो
Scanned by CamScanner