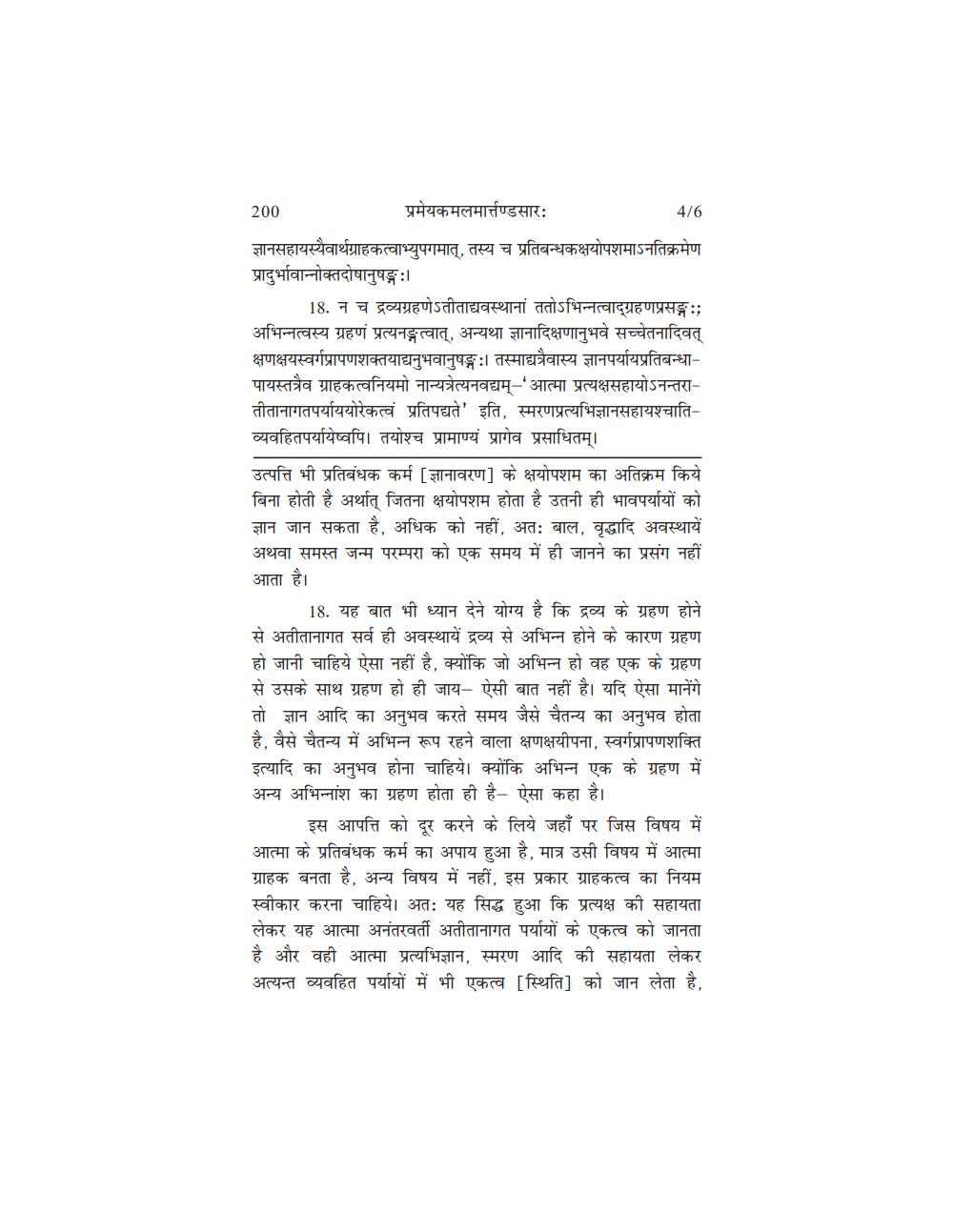________________
200
प्रमेयकमलमार्तण्डसारः
4/6
ज्ञानसहायस्यैवार्थग्राहकत्वाभ्युपगमात्, तस्य च प्रतिबन्धकक्षयोपशमाऽनतिक्रमेण प्रादुर्भावान्नोक्तदोषानुषङ्गः।
18. न च द्रव्यग्रहणेऽतीताद्यवस्थानां ततोऽभिन्नत्वाद्ग्रहणप्रसङ्गः; अभिन्नत्वस्य ग्रहणं प्रत्यनङ्गत्वात्, अन्यथा ज्ञानादिक्षणानुभवे सच्चेतनादिवत् क्षणक्षयस्वर्गप्रापणशक्तयाद्यनुभवानुषङ्गः। तस्माद्यत्रैवास्य ज्ञानपर्यायप्रतिबन्धापायस्तत्रैव ग्राहकत्वनियमो नान्यत्रेत्यनवद्यम्-'आत्मा प्रत्यक्षसहायोऽनन्तरातीतानागतपर्याययोरेकत्वं प्रतिपद्यते' इति, स्मरणप्रत्यभिज्ञानसहायश्चातिव्यवहितपर्यायेष्वपि। तयोश्च प्रामाण्यं प्रागेव प्रसाधितम्। उत्पत्ति भी प्रतिबंधक कर्म [ज्ञानावरण] के क्षयोपशम का अतिक्रम किये बिना होती है अर्थात् जितना क्षयोपशम होता है उतनी ही भावपर्यायों को ज्ञान जान सकता है, अधिक को नहीं, अतः बाल, वृद्धादि अवस्थायें अथवा समस्त जन्म परम्परा को एक समय में ही जानने का प्रसंग नहीं
आता है।
18. यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि द्रव्य के ग्रहण होने से अतीतानागत सर्व ही अवस्थायें द्रव्य से अभिन्न होने के कारण ग्रहण हो जानी चाहिये ऐसा नहीं है, क्योंकि जो अभिन्न हो वह एक के ग्रहण से उसके साथ ग्रहण हो ही जाय- ऐसी बात नहीं है। यदि ऐसा मानेंगे तो ज्ञान आदि का अनुभव करते समय जैसे चैतन्य का अनुभव होता है, वैसे चैतन्य में अभिन्न रूप रहने वाला क्षणक्षयीपना, स्वर्गप्रापणशक्ति इत्यादि का अनुभव होना चाहिये। क्योंकि अभिन्न एक के ग्रहण में अन्य अभिन्नांश का ग्रहण होता ही है- ऐसा कहा है।
इस आपत्ति को दूर करने के लिये जहाँ पर जिस विषय में आत्मा के प्रतिबंधक कर्म का अपाय हुआ है, मात्र उसी विषय में आत्मा ग्राहक बनता है, अन्य विषय में नहीं, इस प्रकार ग्राहकत्व का नियम स्वीकार करना चाहिये। अतः यह सिद्ध हुआ कि प्रत्यक्ष की सहायता लेकर यह आत्मा अनंतरवर्ती अतीतानागत पर्यायों के एकत्व को जानता है और वही आत्मा प्रत्यभिज्ञान, स्मरण आदि की सहायता लेकर अत्यन्त व्यवहित पर्यायों में भी एकत्व [स्थिति] को जान लेता है,