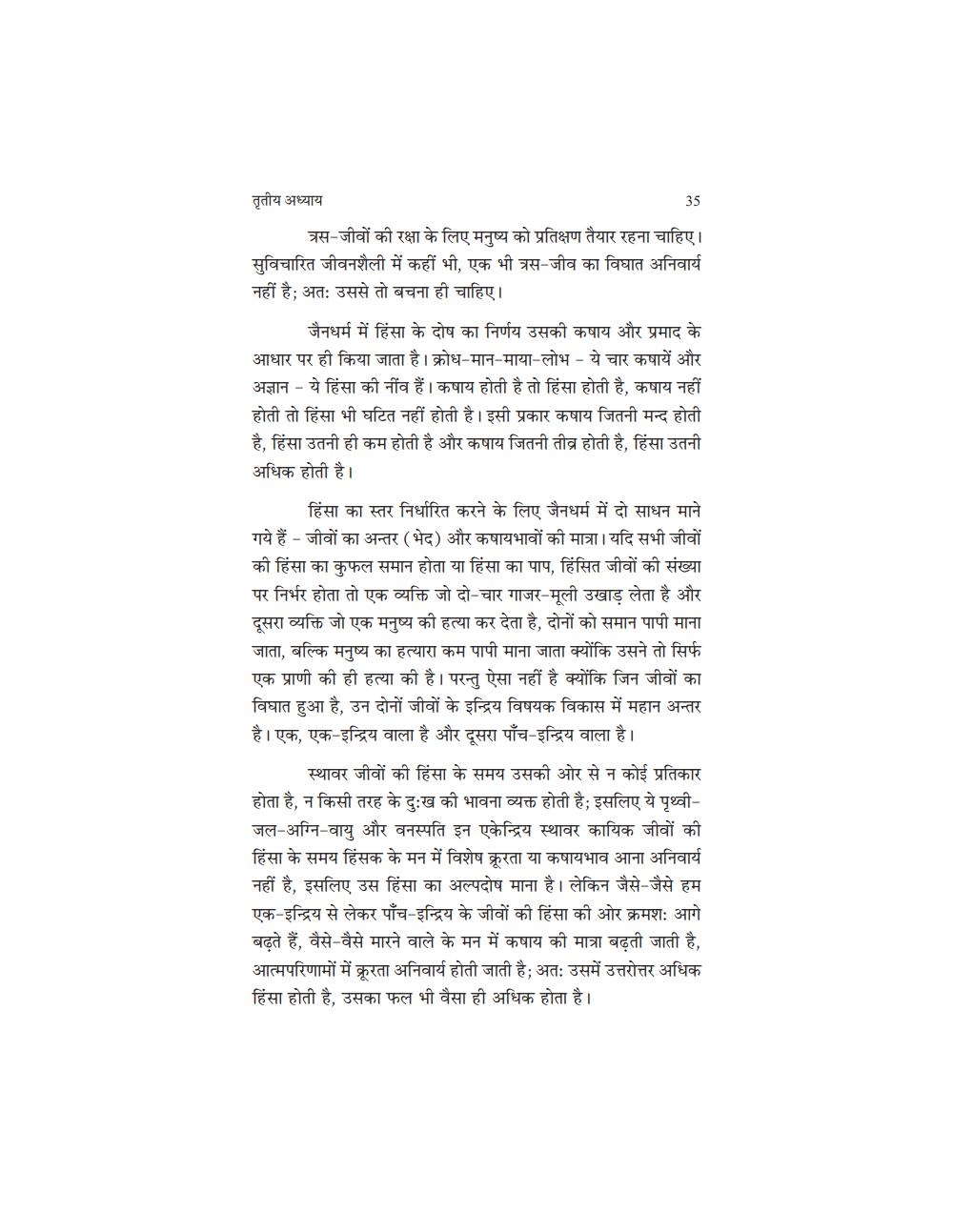________________
35
तृतीय अध्याय
त्रस-जीवों की रक्षा के लिए मनुष्य को प्रतिक्षण तैयार रहना चाहिए। सुविचारित जीवनशैली में कहीं भी, एक भी त्रस-जीव का विघात अनिवार्य नहीं है; अत: उससे तो बचना ही चाहिए।
जैनधर्म में हिंसा के दोष का निर्णय उसकी कषाय और प्रमाद के आधार पर ही किया जाता है। क्रोध-मान-माया-लोभ - ये चार कषायें और अज्ञान - ये हिंसा की नींव हैं। कषाय होती है तो हिंसा होती है, कषाय नहीं होती तो हिंसा भी घटित नहीं होती है। इसी प्रकार कषाय जितनी मन्द होती है, हिंसा उतनी ही कम होती है और कषाय जितनी तीव्र होती है, हिंसा उतनी अधिक होती है।
हिंसा का स्तर निर्धारित करने के लिए जैनधर्म में दो साधन माने गये हैं - जीवों का अन्तर (भेद) और कषायभावों की मात्रा। यदि सभी जीवों की हिंसा का कुफल समान होता या हिंसा का पाप, हिंसित जीवों की संख्या पर निर्भर होता तो एक व्यक्ति जो दो-चार गाजर-मूली उखाड़ लेता है और दूसरा व्यक्ति जो एक मनुष्य की हत्या कर देता है, दोनों को समान पापी माना जाता, बल्कि मनुष्य का हत्यारा कम पापी माना जाता क्योंकि उसने तो सिर्फ एक प्राणी की ही हत्या की है। परन्तु ऐसा नहीं है क्योंकि जिन जीवों का विघात हुआ है, उन दोनों जीवों के इन्द्रिय विषयक विकास में महान अन्तर है। एक, एक-इन्द्रिय वाला है और दूसरा पाँच-इन्द्रिय वाला है।
स्थावर जीवों की हिंसा के समय उसकी ओर से न कोई प्रतिकार होता है, न किसी तरह के दुःख की भावना व्यक्त होती है। इसलिए ये पृथ्वीजल-अग्नि-वायु और वनस्पति इन एकेन्द्रिय स्थावर कायिक जीवों की हिंसा के समय हिंसक के मन में विशेष क्रूरता या कषायभाव आना अनिवार्य नहीं है, इसलिए उस हिंसा का अल्पदोष माना है। लेकिन जैसे-जैसे हम एक-इन्द्रिय से लेकर पाँच-इन्द्रिय के जीवों की हिंसा की ओर क्रमशः आगे बढ़ते हैं, वैसे-वैसे मारने वाले के मन में कषाय की मात्रा बढ़ती जाती है, आत्मपरिणामों में क्रूरता अनिवार्य होती जाती है; अत: उसमें उत्तरोत्तर अधिक हिंसा होती है, उसका फल भी वैसा ही अधिक होता है।