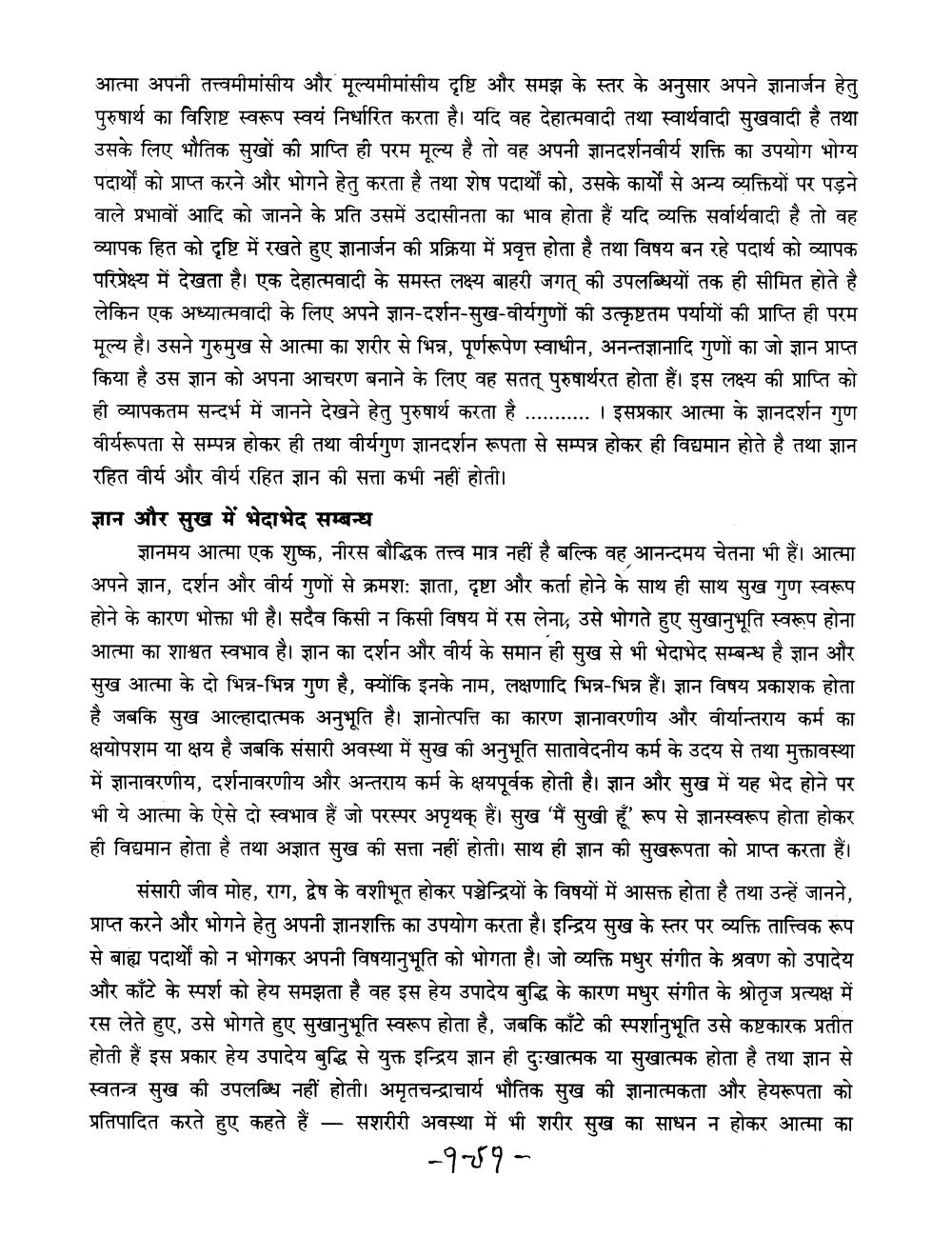________________ आत्मा अपनी तत्त्वमीमांसीय और मूल्यमीमांसीय दृष्टि और समझ के स्तर के अनुसार अपने ज्ञानार्जन हेतु पुरुषार्थ का विशिष्ट स्वरूप स्वयं निर्धारित करता है। यदि वह देहात्मवादी तथा स्वार्थवादी सुखवादी है तथा उसके लिए भौतिक सुखों की प्राप्ति ही परम मूल्य है तो वह अपनी ज्ञानदर्शनवीर्य शक्ति का उपयोग भोग्य पदार्थों को प्राप्त करने और भोगने हेतु करता है तथा शेष पदार्थों को, उसके कार्यों से अन्य व्यक्तियों पर पड़ने वाले प्रभावों आदि को जानने के प्रति उसमें उदासीनता का भाव होता हैं यदि व्यक्ति सर्वार्थवादी है तो वह व्यापक हित को दृष्टि में रखते हुए ज्ञानार्जन की प्रक्रिया में प्रवृत्त होता है तथा विषय बन रहे पदार्थ को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखता है। एक देहात्मवादी के समस्त लक्ष्य बाहरी जगत् की उपलब्धियों तक ही सीमित होते है लेकिन एक अध्यात्मवादी के लिए अपने ज्ञान-दर्शन-सुख-वीर्यगुणों की उत्कृष्टतम पर्यायों की प्राप्ति ही परम मूल्य है। उसने गुरुमुख से आत्मा का शरीर से भिन्न, पूर्णरूपेण स्वाधीन, अनन्तज्ञानादि गुणों का जो ज्ञान प्राप्त किया है उस ज्ञान को अपना आचरण बनाने के लिए वह सतत् पुरुषार्थरत होता हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति को ही व्यापकतम सन्दर्भ में जानने देखने हेतु पुरुषार्थ करता है ........... / इसप्रकार आत्मा के ज्ञानदर्शन गुण वीर्यरूपता से सम्पन्न होकर ही तथा वीर्यगुण ज्ञानदर्शन रूपता से सम्पन्न होकर ही विद्यमान होते है तथा ज्ञान रहित वीर्य और वीर्य रहित ज्ञान की सत्ता कभी नहीं होती। ज्ञान और सुख में भेदाभेद सम्बन्ध ज्ञानमय आत्मा एक शुष्क, नीरस बौद्धिक तत्त्व मात्र नहीं है बल्कि वह आनन्दमय चेतना भी हैं। आत्मा अपने ज्ञान, दर्शन और वीर्य गुणों से क्रमश: ज्ञाता, दृष्टा और कर्ता होने के साथ ही साथ सुख गुण स्वरूप होने के कारण भोक्ता भी है। सदैव किसी न किसी विषय में रस लेना, उसे भोगते हुए सुखानुभूति स्वरूप होना आत्मा का शाश्वत स्वभाव है। ज्ञान का दर्शन और वीर्य के समान ही सुख से भी भेदाभेद सम्बन्ध है ज्ञान और सुख आत्मा के दो भिन्न-भिन्न गुण है, क्योंकि इनके नाम, लक्षणादि भिन्न-भिन्न हैं। ज्ञान विषय प्रकाशक होता है जबकि सुख आल्हादात्मक अनुभूति है। ज्ञानोत्पत्ति का कारण ज्ञानावरणीय और वीर्यान्तराय कर्म का क्षयोपशम या क्षय है जबकि संसारी अवस्था में सुख की अनुभूति सातावेदनीय कर्म के उदय से तथा मुक्तावस्था में ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अन्तराय कर्म के क्षयपूर्वक होती है। ज्ञान और सुख में यह भेद होने पर भी ये आत्मा के ऐसे दो स्वभाव हैं जो परस्पर अपृथक् हैं। सुख 'मैं सुखी हूँ' रूप से ज्ञानस्वरूप होता होकर ही विद्यमान होता है तथा अज्ञात सुख की सत्ता नहीं होती। साथ ही ज्ञान की सुखरूपता को प्राप्त करता हैं। ____ संसारी जीव मोह, राग, द्वेष के वशीभूत होकर पञ्चेन्द्रियों के विषयों में आसक्त होता है तथा उन्हें जानने, प्राप्त करने और भोगने हेतु अपनी ज्ञानशक्ति का उपयोग करता है। इन्द्रिय सुख के स्तर पर व्यक्ति तात्त्विक रूप से बाह्य पदार्थों को न भोगकर अपनी विषयानुभूति को भोगता है। जो व्यक्ति मधुर संगीत के श्रवण को उपादेय और काँटे के स्पर्श को हेय समझता है वह इस हेय उपादेय बुद्धि के कारण मधुर संगीत के श्रोतृज प्रत्यक्ष में रस लेते हुए, उसे भोगते हुए सुखानुभूति स्वरूप होता है, जबकि काँटे की स्पर्शानुभूति उसे कष्टकारक प्रतीत होती हैं इस प्रकार हेय उपादेय बुद्धि से युक्त इन्द्रिय ज्ञान ही दुःखात्मक या सुखात्मक होता है तथा ज्ञान से स्वतन्त्र सुख की उपलब्धि नहीं होती। अमृतचन्द्राचार्य भौतिक सुख की ज्ञानात्मकता और हेयरूपता को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं - सशरीरी अवस्था में भी शरीर सुख का साधन न होकर आत्मा का -1-59